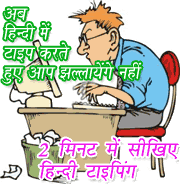सावन आया बरसने को आँगन नहीं रहा
सावन आया बरसने को आँगन नहीं रहाघटाओं में बरसने का पागलपन नहीं रहा
आती है बारिश, लोगों के दिल भीगते नहीं
नीम और पीपल के पेड़ों पे झूला नहीं रहा.
यही अब सच है...शायद. किसी ने डूबे-डूबे मन से बताया कि भारत में सावन के समय अब उतना मजा नहीं आता जितना पहले आता था...वो बरसाती मौसम..पानी बरसने के पहले वो मस्त बहकी हवायें..जो बारिश आने के पहले आँधी की तरह आकर हर चीज़ अस्त-व्यस्त कर जाती थीं..कहाँ हैं ? होंगी कहीं...पागल हो जाते थे हम सब उनके लिये...अब भी उनके आने का सब इंतज़ार करते हैं....उनका सब लोग मजा लेना चाहते हैं...और वो बादल कहाँ हैं जो सावन में बरसने के लिये पागल रहते थे...सुना है कि अब उनके बहुत नखरे हो गये हैं..बहुत सोच समझकर आते हैं बरसने के लिये...साथ में बदलते हुये समय के रहन-सहन के साथ सावन मनाने की समस्या भी सोचनीय हो गयी है...उन हवाओं की मस्ती का आनंद लेने को अब हर जगह खुली छतें नहीं...खुले आँगन नहीं..कहीं-कहीं तो बरामदे भी नहीं..घरों के पिछवाड़े नहीं जहाँ कोई नीम या पीपल जैसे पेड़ हों जिनपर झूला डाला जा सके. जहाँ बड़ी-बड़ी इमारतें हैं वहाँ शहरों में बच्चे पार्क में खेलते हैं तो वहाँ खुले में स्टील के फ्रेम पर झूले होते हैं जिन पर प्लास्टिक की सीटें होती हैं...आजकल कई जगह टायर आदि को भी सीट की जगह बाँध देते हैं...सबकी अपनी-अपनी किस्मत...आज के बच्चे पहले मनाये जाने वाले सावन का हाल सुनकर आश्चर्य प्रकट करते हैं...और उन बातों को एक दिलचस्प कहानी की तरह सुनते हैं.
लो अब बचपन की बातें करते हुये अपना बचपन भी सजीव हो गया जिसमें..आँगन, जीना, छत, झूला, आम के बौर, और पेड़ों पर पत्तों के बीच छिपी कुहुकती हुई कोयलिया, नीम और पपीते के पेड़ ..जंगल जलेबियों के सफ़ेद गुलाबी गुच्छे..दीवारों या पेड़ों पर चढ़ती हुई गुलपेंचे की बेल जो अब भी मेरी यादों की दीवार पर लिपटी हुई है...हरसिंगार के पेड़ से झरते हुये उसके नारंगी-सफ़ेद महकते कोमल फूल...सबह-सुबह की मदहोश हवा में उनींदी आँखों को मलते हुये सूरज के निकलने से पहले जम्हाई लेकर उठना और अपने दादा जी के साथ बागों की तरफ घूमने जाना...पड़ोस के कुछ और बच्चे को भी साथ बटोर लेते थे...और उन कच्ची धूल भरी सड़कों पर कभी-कभी चप्पलों को हाथ में पकड़ कर दौड़ते हुये चलना..आहा !! उस मिट्टी की शीतलता को याद करके मन रोमांचित हो उठता है...आँखों को ताज़ा कर देने वाली सुबह के समय की हरियाली व उन दृश्यों की बात ही निराली थी. जगह-जगह आम के पेड़ थे कभी जमीन पर गिरे हुये आम बटोरना और कभी आमों पर ढेला मारकर उन्हें गिराना...उसका आनंद ही अवर्णनीय है. अपने इस बचपन की कहानी में एक खुला आँगन भी था..बड़ी सी छत थी जहाँ बरसाती हवायें चलते ही उनका आनंद लेने को बच्चे एकत्र हो जाते थे. और बारिश होते ही उसमें भीगकर पानी में छपाछप करते हुए हाथों को फैलाकर घूमते हुए नाचते थे...एक दूसरे पर पानी उछालते थे...और उछलते-कूदते गाना गाते थे...बिजली चमकती थी या बादलों की गड़गड़ाहट होती थी तो भयभीत होकर अन्दर भागते थे और फिर कुछ देर में वापस बाहर भाग कर आ जाते थे...फिर भीगते थे कांपते हुये और पूरी तृप्ति होने पर ही या किसी से डांट खाने पर अपने को सुखाकर कपड़े बदलते थे...छाता लगाकर बड़े से आँगन में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना...हवा की ठंडक से बदन का सिहर जाना....और मक्खियाँ भी बरसात की वजह से वरामदे व कमरों में ठिकाना ढूँढती फिरती थीं...अरे हाँ, भूल ही गयी बताना कि ऐसे मौसम में फिर गरम-गरम पकौड़ों का बनना जरूरी होता था...ये रिवाज़ भारत में हर जगह क्यों है...हा हा...क्या मजा आता था.
अब बच्चे उतना आनंद नहीं ले पाते..उनके तरीके बदल गये हैं, जगहें बदल गयी हैं ना घरों में वो बात रही और ना ही बच्चों में. ये भी सुना है कि सावन का तीज त्योहार भी उतने उत्साह से नहीं मनाया जाता जितना पहले होता था...लेकिन हम लोगों के पास मन लगाने को यही सिम्पल साधन थे मनोरंजन के..क्या आनंद था ! तीजों पर झूला पड़ता था तो उल्लास का ठिकाना नहीं रहता था...पेड़ की शीतल हवा में जमीन पर पड़ी कुचली निमकौरिओं की उड़ती गंध..वो पेड़ की फुनगी पर बैठ कर काँव-काँव करते कौये...और पास में कुआँ और पपीते का पेड़ जिस पर लगे हुये कच्चे-पक्के पपीते...काश मुझे वो सावन फिर से मिल जाये...नीम के पेड़ पर झूला झूलते हुये..ठंडी सर्र-सर्र चलती हवा में उँची-उँची पैंगे लेना..अपनी बारी का इंतजार करना..दूसरे को धक्का देना...गिर पड़ने पर झाड़-पूँछ कर फिर तैयार हो जाना झूलने को...आज भी सब लोग आनंद लेना चाहते इन सब बातों का पर अब वो बात कहाँ ..लोग बदले बातें बदलीं..रीति-रिवाजें बदलीं..बस बातों में ही सावन रह गया है.
शन्नो अग्रवाल
(तस्वीर बैठक के पुराने साथी अबयज़ खान ने भेजी है)



 सन्देश आने लगे कि यह धारावाहिक साहित्यिक उपन्यास जैसा लगता है, इसे ज़रूर देखो, और मैंने इसे बड़े चाव से देखना शुरू किया, शुरू में इसे बेहद पसंद भी किया. राजस्थान में आखा तीज के दिन सामूहिक बाल विवाह होते हैं, जिस की तरफ समाज सुधारकों का ध्यान नहीं गया. सरकारें कुछ हद तक कोशिशें करती रही पर जब तक मानसिक रूप से कोई समाज नहीं बदलेगा तब तक कितने भी कड़े क़ानून बन जाएँ, समाज नहीं सुधर सकता, चाहे वे खाप पंचायतों के निर्दयी आदेश हों, चाहे Honour killings के अभिशाप. ये सब समाज में बने रहेंगे, जब तक कोई महापुरुष इन समाजों का हृदय ही परिवर्तित न कर के रख दे. राजस्थान में कहते हैं कि यदि हम बच्चों की शादियाँ न करें तो देवता नाराज़ हो जाएंगे और देवताओं के कोप के रूप में न जाने कौन सा अनर्थ हम पर आन पड़ेगा. राजा राम मोहन रॉय ने जब सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया तो ब्रिटिश से केवल क़ानून ही नहीं बदलवाया, वरन दिन रात एक कर के गांव गांव जा कर लोगों की सुषुप्त चेतनाओं को झकझोरा, उन का मन बदला था. यहाँ तो यह हालत है कि राजस्थान में ‘सती महिमा’ पर भी लोग उच्च न्यायालय गए थे कि सरकार होती कौन है, हमें सती महिमा पर उत्सव करने से रोकने वाली. बहरहाल, बात तो ‘बालिका वधु’ धारावाहिक की चल्र रही थी. इस धारावाहिक में एक अबोध बालिका आनंदी का बचपन में ही ब्याह तय हो जाता है. ब्याह होता क्या है, यह उस बच्ची को पता ही नहीं. वह माँ से यह खबर सुनते ही आस पड़ोस में दौड़ी दौड़ी चली जाती है. जो जहाँ बैठा या खड़ा है, सब को खुशी से बताती जाती है – ‘मेरा ब्याह तय हो गया... मेरा ब्याह तय हो गया...’. पर जिस घड़ी सासरे जाना होता है, तब सचमुच रोने लगती है. उस की कोई टीचर पुलिस लाती है, पर आनंदी इस सारे घटनाचक्र की विभीषिका से डर कर केवल इतना ही समझ पाती है कि यदि पुलिस को पता चल गया कि उस का ब्याह हो रहा है तो पुलिस उस के बापू को पकड़ लेगी, और वह टीचर की इस चेतावनी के बावजूद कि झूठ बोलने वालों की नाक फूल जाती है, पुलिस से झूठ बोलती है. उधर टीचर को गांव छोडना पड़ता है क्यों कि गाँव के लोग उस के घर में ही तोड़-फोड़ कर के उस के घर को तहस-नहस कर डालते हैं. ये सब बहुत वास्तविक और प्रभावशाली लगा. कुछ वर्ष पहले ‘स्टार न्यूज़’ पर जब मैंने एक खबर सुनी कि बाल विवाह रुकवाने की कोशिश करने वाली एक महिला के हाथ ही काट दिए गए, तब रूह सचमुच, अविश्वसनीयता के मारे काँप गई थी. इसलिए इस धारावाहिक की साहित्यिक सामाजिक गहराई को मैं पहचान गया था. गांव के पिछड़ेपन की सूरत चंपा नाम की एक लड़की की व्यथा कथा से पता चलती है. बचपन में ही चंपा की शादी तय हो गई थी, पर चंपा अपने मंगेतर के ही एक हमनाम लड़के के साथ भाग गई और वापस आई तो बर्बाद सी हालत में थी क्यों कि वह माँ बनने वाली थी और उस का प्रेमी भाग चुका था. किशोरावस्था की अबोधता में की हुई भूल के कारण जिस स्थिति में चंपा पहुँच चुकी थी, उस में उस का सहारा बनना तो दूर, पूरा गांव अपने सरपंच की शरण में आ खडा हुआ कि अब क्या किया जाए. सरपंच उस समय दरिंदगी की एक प्रतिमा सा लगता है और घोषित करता है कि चंपा को मार डालने में गांव का एक एक व्यक्ति अब उस का साथ देगा. पूरा गांव दौड़ पड़ता है, उस अभागी लड़की की खोज में जो एक मंदिर में भयभीत, कांपती सी छुपी है और आनंदी जैसी कुछ सहेलियों की मदद से ही गांव से भाग जाती है. सासरे में आनंदी के पति की ज़ालिम दादी सा कल्याणी है, जो पिछड़े हुए गांवों के ज़ालिम समाज की गली सड़ी प्रथाओं की ही प्रतीक है. जो समाज अपनी ही बालिकाओं पर न जाने कैसे कैसे ज़ुल्म ढाता है, कोई परम्पराओं के नाम पर तो कोई देवताओं के नाम पर. आनंदी अपने पति जगदीसा के साथ एक ही मेज़ पर खाना नहीं खा सकती. पहले उस का बीं (पति) खाना खाएगा, फिर उस की जूठी प्लेट में बींदड़ी (पत्नी) खाएगी. ये सब तो आनंदी को सहना ही पड़ा. पर गांव की किसी बाल विधवा को चूडियां पहनाने के जुर्म में आनंदी को दादी सा रात भर कोठरी में बंद कर देती है. उस के सास-ससुर या पति या ताई उसे निकाल न सकें, या पानी तक न पहुंचाएं, इसलिए बंद कोठरी के बाहर कुर्सी डाल कर बैठ जाती है दादी सा. पिछले 500 एपिसोड में आनंदी पर हो रहे अत्याचारों का एक लंबा सिलसिला है, जिस में कोई बड़ी उम्र की बहूरानी भी शायद जीते जी मर जाए. आनंदी को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता, जब कि पढ़ने में वह बहुत प्रखर है, पूरे स्कूल के सभी विद्यार्थियों में. कभी किसी भूल पर उसे घर से निकाल कर मायके भेज दिया जाता है, वह भी दूसरे गांव में जाने के लिए अकेले ही बस में चढ़ा दिया जाता है. जब उस की टीचर कुछ साल बाद अचानक गांव आती है और उस के घर किसी उत्सव में शामिल होती है तो वह सब के सामने इस बात का भांडा भी फोड़ती है कि कल्याणी देवी (दादी सा) ने उस की किताबें खुद आनंदी से ही जलवा दी हैं. यही नहीं, पिता की मार खा कर आनंदी का किशोर पति गांव से भाग कर मुंबई चला जाता है और वहां किसी अपराधी गिरोह में फंस जाता है जो बच्चों के शरीर के अंग काट कर उन्हें भिखारी बना देता है. वहां भी आनंदी ही पहुँचती है ससुर के साथ और पति को अपराधियों की गोली से बचा कर खुद अपने सिर पर गोली झेलती है. पर दादी सा को इतनी बड़ी घटना के बावजूद बींदड़ी पराई और ज़ुल्मों की हक़दार ही अधिक नज़र आती है. आनंदी के बीमार हो चुके होने का बहाना बना कर वह चुपके चुपके जगदीसा का दूसरा विवाह भी करवा देती है जहाँ से महापंचायत के ज़रिये ही जगदीसा को दूसरी पत्नी से छुटकारा मिलता है. आनंदी की तरह और भी बहू-बेटियां हैं जो एक नारकीय जीवन जीती हैं. जैसे दादी सा की अपनी ही पोती सुगना जिस का पति गौने वाले दिन ही डाकुओं की गोली का शिकार हो कर मर जाता है. सुगना क्यों कि विधवा हो चुकी है, इसलिए उसे कोठरी में एक ज़लील सी जिंदगी जीनी पड़ती है, जहाँ वह फर्श पर सोए और अपना खाना खुद बनाए. दादी सा के बड़े सुपुत्र की पहली पत्नी कुल का चिराग जनने की प्रक्रिया में उस चिराग के बचने की उम्मीद में शहीद हो जाती है तो दादी सा उस बड़े पुत्र का ब्याह उस से भी बीस वर्ष छोटी लड़की से करा कर आती है. ये सब के सब एक अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य हैं. पर सवाल ये है कि इतने अत्याचार सहने के बावजूद आनंदी का पिता खज़ान सिंह आनंदी को अपने सासरे से वापस मायके ला का उस संबंध को तोड़ क्यों नहीं सका. आनंदी तो दिन-ब-दिन सासरे से जुड़ती चली जाती है. वह जब आई तो अबोध थी पर पांच साल बीतते न बीतते वह मूर्खता की सीमा तक अबोध बन जाती है और खुद ही घोषित करती है कि क्यों कि दादी सा को मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इस लिए मैं आगे ना पढूंगी. जगदीसा से इस कदर अटूट तरीके से जुड गई सी दिखती है आनंदी कि अब उस से बिछोह के समय उसे स्वयं पर कोई बहुत बड़ा अत्यचार सा होता लगता है. क्या आनंदी का इस कदर सासरे से अति प्यार करना और पति से बुरी तरह भावनात्मक स्तर तक जुड़ जाना बाल विवाह करवाने वालों की हिम्मत नहीं बढ़ाएगा? आनंदी हर मुसीबत सह कर भी अपने सासरे में खुश बल्कि बेहद खुश सी नज़र आती है. यदि पहली बार जब उसे किसी गलती के कारण मायके भेज दिया गया तभी वह न लौटती और अपने पिता के पास रह कर पढ़ लिख कर बड़ी होती तब उसे अपने फैसले स्वयं लेने की पूरी आज़ादी होती और उसे बचपन में हुआ वह विवाह महज़ एक मूर्खता ही लगता. पति जगदीसा भी बड़ा हो चुका होता और यदि ये दोनों बचपन के पति-पत्नी युवा हो कर पिछला सब भूल कर अपने अपने समाज में कहीं अन्यत्र प्यार कर बैठते तो? तब क्या समाज की आँखें न खुलती कि इन के प्यार करने की, अपना पति स्वयं चुनने की उम्र तो अब आई है, और वह बचपन वाली शादी सचमुच व्यर्थ सी है जिस में अत्याचारों से लड़ने की कोई चेतना तक बचपन में असंभव है. युवा आनंदी जिस से प्यार करती, बराबरी के स्तर पर करती और अपने ससुराल में वह पति के साथ एक ही मेज़ पर खाना खाती. सास-ससुर की इज्ज़त करती पर अपनी शर्तों पर जीती. दादी सा जैसी ज़ालिम औरत को दो टूक जवाब देती या उस के विरुद्ध विद्रोह करती. कोई कह सकता है कि धारावाहिक में इतनी सारी बालिका-वधुओं की जिंदगी दिखा दी गई तो धारावाहिक विफल कैसे हुआ. पर यह पूरा धारावाहिक आनंदी पर इतना अधिक फोकस करता कि बाकी सब बातें अनायास ही बेहद गौण हो जाती हैं. पिछले 10-15 एपिसोड में तो पति के प्रति आनंदी का जूनून सीमा पार कर गया है. जगदीसा और आनंदी का प्रेम वयस्क जोड़ों को भी मात कर देता है. पांच वर्ष के लिए मायके भेज दिए जाने पर आनंदी की पति के लिए असह्य तड़प और पति का स्कूल से ही बिना किसी को बताए अपने गांव जैतसर से आनंदी के गांव बेलारिया आ जाना. और रेगिस्तान में दूर से करीब आते हुए आनंदी और जगदीसा को जिस तरीके से स्लो कैमरा में फिल्मांकित किया गया है, वह सचमुच किसी वयस्क जोड़े की प्रेम कहानी सा लगता है. आनंदी का frustration तो कहीं भी नज़र नहीं आता. बाल विवाह के कारण आनंदी की कोई क्षति भी हुई होगी, यह कहीं द्रष्टव्य ही नहीं है. बल्कि मायके में एक मंदिर की तरह उस ने सब की तस्वीरें सजा रखी हैं और खाना खाते समय पहले पति को भोग भी लगाती है. वह बावलियों की तरह एक एक तस्वीर को देख पहाडा सा रटती है – ये सासू माँ ... ये बापू सा ...और ये? रेगिस्तान में 5 वर्ष प्रतिदिन दूर तक इंतज़ार में देखते देखते उस की पथराई आँखें और एक छोटी सी सहेली के पूछने पर कि किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या, उस का कहना कि 5 साल से इंतज़ार ही तो कर रही हूँ. यह सब देख कर लगता है कि नायक- नायिका की केवल उम्र छोटी है, बाकी सब तो किसी जनम जनम के साथ की प्रेम कहानी जैसा लगता है. धारावाहिक में बीच में लम्बाई प्राप्त करने के लिए स्टंट प्रसंग भी आए जैसे कि दादी सा के देवर महावीर सिंह को पता चलना कि दादी सा का बड़ा बेटा वसंत दरअसल उस का बेटा है आदि. कुल मिला कर यह सारा धारावाहिक आनंदी पर इतना ज़्यादा केंद्रित हो गया है कि किसी भी प्रकार से यह लगता ही नहीं कि यह बाल विवाह के विरुद्ध प्रचार करता है. इसे देख देख कर तो माँ बाप अपने बच्चों को आनंदी जैसी बहादुर लड़की बनने की प्रेरणा देंगे जिसने मुसीबतों पर मुसीबतें देखी पर अपनी जगह अडिग रही और अपना पूरा जनम ऐसी मुसीबतों वाली ससुराल को दे दिया. ऐसी शिक्षा दे कर कोई आश्चर्य नहीं कि समाज में बाल-विवाह बढ़ने शुरू हो जाएँ.
सन्देश आने लगे कि यह धारावाहिक साहित्यिक उपन्यास जैसा लगता है, इसे ज़रूर देखो, और मैंने इसे बड़े चाव से देखना शुरू किया, शुरू में इसे बेहद पसंद भी किया. राजस्थान में आखा तीज के दिन सामूहिक बाल विवाह होते हैं, जिस की तरफ समाज सुधारकों का ध्यान नहीं गया. सरकारें कुछ हद तक कोशिशें करती रही पर जब तक मानसिक रूप से कोई समाज नहीं बदलेगा तब तक कितने भी कड़े क़ानून बन जाएँ, समाज नहीं सुधर सकता, चाहे वे खाप पंचायतों के निर्दयी आदेश हों, चाहे Honour killings के अभिशाप. ये सब समाज में बने रहेंगे, जब तक कोई महापुरुष इन समाजों का हृदय ही परिवर्तित न कर के रख दे. राजस्थान में कहते हैं कि यदि हम बच्चों की शादियाँ न करें तो देवता नाराज़ हो जाएंगे और देवताओं के कोप के रूप में न जाने कौन सा अनर्थ हम पर आन पड़ेगा. राजा राम मोहन रॉय ने जब सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया तो ब्रिटिश से केवल क़ानून ही नहीं बदलवाया, वरन दिन रात एक कर के गांव गांव जा कर लोगों की सुषुप्त चेतनाओं को झकझोरा, उन का मन बदला था. यहाँ तो यह हालत है कि राजस्थान में ‘सती महिमा’ पर भी लोग उच्च न्यायालय गए थे कि सरकार होती कौन है, हमें सती महिमा पर उत्सव करने से रोकने वाली. बहरहाल, बात तो ‘बालिका वधु’ धारावाहिक की चल्र रही थी. इस धारावाहिक में एक अबोध बालिका आनंदी का बचपन में ही ब्याह तय हो जाता है. ब्याह होता क्या है, यह उस बच्ची को पता ही नहीं. वह माँ से यह खबर सुनते ही आस पड़ोस में दौड़ी दौड़ी चली जाती है. जो जहाँ बैठा या खड़ा है, सब को खुशी से बताती जाती है – ‘मेरा ब्याह तय हो गया... मेरा ब्याह तय हो गया...’. पर जिस घड़ी सासरे जाना होता है, तब सचमुच रोने लगती है. उस की कोई टीचर पुलिस लाती है, पर आनंदी इस सारे घटनाचक्र की विभीषिका से डर कर केवल इतना ही समझ पाती है कि यदि पुलिस को पता चल गया कि उस का ब्याह हो रहा है तो पुलिस उस के बापू को पकड़ लेगी, और वह टीचर की इस चेतावनी के बावजूद कि झूठ बोलने वालों की नाक फूल जाती है, पुलिस से झूठ बोलती है. उधर टीचर को गांव छोडना पड़ता है क्यों कि गाँव के लोग उस के घर में ही तोड़-फोड़ कर के उस के घर को तहस-नहस कर डालते हैं. ये सब बहुत वास्तविक और प्रभावशाली लगा. कुछ वर्ष पहले ‘स्टार न्यूज़’ पर जब मैंने एक खबर सुनी कि बाल विवाह रुकवाने की कोशिश करने वाली एक महिला के हाथ ही काट दिए गए, तब रूह सचमुच, अविश्वसनीयता के मारे काँप गई थी. इसलिए इस धारावाहिक की साहित्यिक सामाजिक गहराई को मैं पहचान गया था. गांव के पिछड़ेपन की सूरत चंपा नाम की एक लड़की की व्यथा कथा से पता चलती है. बचपन में ही चंपा की शादी तय हो गई थी, पर चंपा अपने मंगेतर के ही एक हमनाम लड़के के साथ भाग गई और वापस आई तो बर्बाद सी हालत में थी क्यों कि वह माँ बनने वाली थी और उस का प्रेमी भाग चुका था. किशोरावस्था की अबोधता में की हुई भूल के कारण जिस स्थिति में चंपा पहुँच चुकी थी, उस में उस का सहारा बनना तो दूर, पूरा गांव अपने सरपंच की शरण में आ खडा हुआ कि अब क्या किया जाए. सरपंच उस समय दरिंदगी की एक प्रतिमा सा लगता है और घोषित करता है कि चंपा को मार डालने में गांव का एक एक व्यक्ति अब उस का साथ देगा. पूरा गांव दौड़ पड़ता है, उस अभागी लड़की की खोज में जो एक मंदिर में भयभीत, कांपती सी छुपी है और आनंदी जैसी कुछ सहेलियों की मदद से ही गांव से भाग जाती है. सासरे में आनंदी के पति की ज़ालिम दादी सा कल्याणी है, जो पिछड़े हुए गांवों के ज़ालिम समाज की गली सड़ी प्रथाओं की ही प्रतीक है. जो समाज अपनी ही बालिकाओं पर न जाने कैसे कैसे ज़ुल्म ढाता है, कोई परम्पराओं के नाम पर तो कोई देवताओं के नाम पर. आनंदी अपने पति जगदीसा के साथ एक ही मेज़ पर खाना नहीं खा सकती. पहले उस का बीं (पति) खाना खाएगा, फिर उस की जूठी प्लेट में बींदड़ी (पत्नी) खाएगी. ये सब तो आनंदी को सहना ही पड़ा. पर गांव की किसी बाल विधवा को चूडियां पहनाने के जुर्म में आनंदी को दादी सा रात भर कोठरी में बंद कर देती है. उस के सास-ससुर या पति या ताई उसे निकाल न सकें, या पानी तक न पहुंचाएं, इसलिए बंद कोठरी के बाहर कुर्सी डाल कर बैठ जाती है दादी सा. पिछले 500 एपिसोड में आनंदी पर हो रहे अत्याचारों का एक लंबा सिलसिला है, जिस में कोई बड़ी उम्र की बहूरानी भी शायद जीते जी मर जाए. आनंदी को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता, जब कि पढ़ने में वह बहुत प्रखर है, पूरे स्कूल के सभी विद्यार्थियों में. कभी किसी भूल पर उसे घर से निकाल कर मायके भेज दिया जाता है, वह भी दूसरे गांव में जाने के लिए अकेले ही बस में चढ़ा दिया जाता है. जब उस की टीचर कुछ साल बाद अचानक गांव आती है और उस के घर किसी उत्सव में शामिल होती है तो वह सब के सामने इस बात का भांडा भी फोड़ती है कि कल्याणी देवी (दादी सा) ने उस की किताबें खुद आनंदी से ही जलवा दी हैं. यही नहीं, पिता की मार खा कर आनंदी का किशोर पति गांव से भाग कर मुंबई चला जाता है और वहां किसी अपराधी गिरोह में फंस जाता है जो बच्चों के शरीर के अंग काट कर उन्हें भिखारी बना देता है. वहां भी आनंदी ही पहुँचती है ससुर के साथ और पति को अपराधियों की गोली से बचा कर खुद अपने सिर पर गोली झेलती है. पर दादी सा को इतनी बड़ी घटना के बावजूद बींदड़ी पराई और ज़ुल्मों की हक़दार ही अधिक नज़र आती है. आनंदी के बीमार हो चुके होने का बहाना बना कर वह चुपके चुपके जगदीसा का दूसरा विवाह भी करवा देती है जहाँ से महापंचायत के ज़रिये ही जगदीसा को दूसरी पत्नी से छुटकारा मिलता है. आनंदी की तरह और भी बहू-बेटियां हैं जो एक नारकीय जीवन जीती हैं. जैसे दादी सा की अपनी ही पोती सुगना जिस का पति गौने वाले दिन ही डाकुओं की गोली का शिकार हो कर मर जाता है. सुगना क्यों कि विधवा हो चुकी है, इसलिए उसे कोठरी में एक ज़लील सी जिंदगी जीनी पड़ती है, जहाँ वह फर्श पर सोए और अपना खाना खुद बनाए. दादी सा के बड़े सुपुत्र की पहली पत्नी कुल का चिराग जनने की प्रक्रिया में उस चिराग के बचने की उम्मीद में शहीद हो जाती है तो दादी सा उस बड़े पुत्र का ब्याह उस से भी बीस वर्ष छोटी लड़की से करा कर आती है. ये सब के सब एक अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य हैं. पर सवाल ये है कि इतने अत्याचार सहने के बावजूद आनंदी का पिता खज़ान सिंह आनंदी को अपने सासरे से वापस मायके ला का उस संबंध को तोड़ क्यों नहीं सका. आनंदी तो दिन-ब-दिन सासरे से जुड़ती चली जाती है. वह जब आई तो अबोध थी पर पांच साल बीतते न बीतते वह मूर्खता की सीमा तक अबोध बन जाती है और खुद ही घोषित करती है कि क्यों कि दादी सा को मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इस लिए मैं आगे ना पढूंगी. जगदीसा से इस कदर अटूट तरीके से जुड गई सी दिखती है आनंदी कि अब उस से बिछोह के समय उसे स्वयं पर कोई बहुत बड़ा अत्यचार सा होता लगता है. क्या आनंदी का इस कदर सासरे से अति प्यार करना और पति से बुरी तरह भावनात्मक स्तर तक जुड़ जाना बाल विवाह करवाने वालों की हिम्मत नहीं बढ़ाएगा? आनंदी हर मुसीबत सह कर भी अपने सासरे में खुश बल्कि बेहद खुश सी नज़र आती है. यदि पहली बार जब उसे किसी गलती के कारण मायके भेज दिया गया तभी वह न लौटती और अपने पिता के पास रह कर पढ़ लिख कर बड़ी होती तब उसे अपने फैसले स्वयं लेने की पूरी आज़ादी होती और उसे बचपन में हुआ वह विवाह महज़ एक मूर्खता ही लगता. पति जगदीसा भी बड़ा हो चुका होता और यदि ये दोनों बचपन के पति-पत्नी युवा हो कर पिछला सब भूल कर अपने अपने समाज में कहीं अन्यत्र प्यार कर बैठते तो? तब क्या समाज की आँखें न खुलती कि इन के प्यार करने की, अपना पति स्वयं चुनने की उम्र तो अब आई है, और वह बचपन वाली शादी सचमुच व्यर्थ सी है जिस में अत्याचारों से लड़ने की कोई चेतना तक बचपन में असंभव है. युवा आनंदी जिस से प्यार करती, बराबरी के स्तर पर करती और अपने ससुराल में वह पति के साथ एक ही मेज़ पर खाना खाती. सास-ससुर की इज्ज़त करती पर अपनी शर्तों पर जीती. दादी सा जैसी ज़ालिम औरत को दो टूक जवाब देती या उस के विरुद्ध विद्रोह करती. कोई कह सकता है कि धारावाहिक में इतनी सारी बालिका-वधुओं की जिंदगी दिखा दी गई तो धारावाहिक विफल कैसे हुआ. पर यह पूरा धारावाहिक आनंदी पर इतना अधिक फोकस करता कि बाकी सब बातें अनायास ही बेहद गौण हो जाती हैं. पिछले 10-15 एपिसोड में तो पति के प्रति आनंदी का जूनून सीमा पार कर गया है. जगदीसा और आनंदी का प्रेम वयस्क जोड़ों को भी मात कर देता है. पांच वर्ष के लिए मायके भेज दिए जाने पर आनंदी की पति के लिए असह्य तड़प और पति का स्कूल से ही बिना किसी को बताए अपने गांव जैतसर से आनंदी के गांव बेलारिया आ जाना. और रेगिस्तान में दूर से करीब आते हुए आनंदी और जगदीसा को जिस तरीके से स्लो कैमरा में फिल्मांकित किया गया है, वह सचमुच किसी वयस्क जोड़े की प्रेम कहानी सा लगता है. आनंदी का frustration तो कहीं भी नज़र नहीं आता. बाल विवाह के कारण आनंदी की कोई क्षति भी हुई होगी, यह कहीं द्रष्टव्य ही नहीं है. बल्कि मायके में एक मंदिर की तरह उस ने सब की तस्वीरें सजा रखी हैं और खाना खाते समय पहले पति को भोग भी लगाती है. वह बावलियों की तरह एक एक तस्वीर को देख पहाडा सा रटती है – ये सासू माँ ... ये बापू सा ...और ये? रेगिस्तान में 5 वर्ष प्रतिदिन दूर तक इंतज़ार में देखते देखते उस की पथराई आँखें और एक छोटी सी सहेली के पूछने पर कि किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या, उस का कहना कि 5 साल से इंतज़ार ही तो कर रही हूँ. यह सब देख कर लगता है कि नायक- नायिका की केवल उम्र छोटी है, बाकी सब तो किसी जनम जनम के साथ की प्रेम कहानी जैसा लगता है. धारावाहिक में बीच में लम्बाई प्राप्त करने के लिए स्टंट प्रसंग भी आए जैसे कि दादी सा के देवर महावीर सिंह को पता चलना कि दादी सा का बड़ा बेटा वसंत दरअसल उस का बेटा है आदि. कुल मिला कर यह सारा धारावाहिक आनंदी पर इतना ज़्यादा केंद्रित हो गया है कि किसी भी प्रकार से यह लगता ही नहीं कि यह बाल विवाह के विरुद्ध प्रचार करता है. इसे देख देख कर तो माँ बाप अपने बच्चों को आनंदी जैसी बहादुर लड़की बनने की प्रेरणा देंगे जिसने मुसीबतों पर मुसीबतें देखी पर अपनी जगह अडिग रही और अपना पूरा जनम ऐसी मुसीबतों वाली ससुराल को दे दिया. ऐसी शिक्षा दे कर कोई आश्चर्य नहीं कि समाज में बाल-विवाह बढ़ने शुरू हो जाएँ. 
















 मार्कण्डेय
मार्कण्डेय