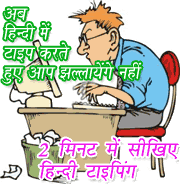~शंकर शरण
अंग्रेजी कहावत है, नाम में क्या रखा है! लेकिन दक्षिण अफ्रीका में यह कहने पर लोग आपकी ओर अजीब निगाहों से देखेंगे कि कैसा अहमक है! पिछले कुछ महीनों से वहां के कुछ बड़े शहरों, प्रांतों के नाम बदलने को लेकर देशव्यापी विवाद चल रहा है। प्रीटोरिया, पॉटचेफ्स्ट्रोम, पीटर्सबर्ग, पीट रेटिफ आदि शहरों, प्रांतों के नाम बदलने का प्रस्ताव है। तर्क है कि जो नाम लोगों को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें बदला ही जाना चाहिए।
यह विषय वहां इतना गंभीर है कि साउथ अफ्रीका ज्योग्राफीकल नेम काउंसिल (एसएजीएनसी) नामक एक सरकारी आयोग इस पर सार्वजनिक सुनवाई कर रहा है। प्रीटोरिया का नाम बदलने की घोषणा हो चुकी थी। किसी कारण उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। प्रीटोरिया पहले त्सवाने कहलाता था जिसे गोरे अफ्रीकियों ने बदल कर प्रीटोरिया किया था। त्सवाने वहां के किसी पुराने प्रतिष्ठित राजा के नाम से बना था जिसके वंशज अभी तक वहां हैं।
इस प्रकार नामों को बदलने का अभियान और विवाद वहां लंबे समय से चल रहा है। पिछले दस वर्ष में वहां 916 स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं। इनमें केवल शहर नहीं; नदियों, पहाड़ों, बांधों और हवाई अड्डों तक के नाम हैं। सैकड़ों सड़कों के बदले गए नाम अतिरिक्त हैं। वहां की एफपीपी पार्टी के नेता पीटर मुलडर ने संसद में कहा कि ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने के सवाल पर अगले बीस वर्ष तक वहां झगड़ा चलता रहेगा। उनकी पार्टी और कुछ अन्य संगठन प्रीटोरिया नाम बनाए रखना चाहते हैं।
इसलिए नाम में बहुत कुछ है। यह केवल दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं। पूरी दुनिया में स्थानों के नाम रखना या पूर्ववत करना सदैव गंभीर राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्त्व रखता है। जैसे किसी को जबरन महान बनाने या अपदस्थ करने की चाह। इन सबका महत्त्व है जिसे हल्के से नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कम्युनिज्म के पतन के बाद रूस, यूक्रेन, मध्य एशिया और पूरे पूर्वी यूरोप में असंख्य शहरों, भवनों, सड़कों के नाम बदले गए। रूस में लेनिनग्राद को पुन: सेंट पीटर्सबर्ग, स्तालिनग्राद को वोल्गोग्राद आदि किया गया। कई बार यह सब भारी आवेग और भावनात्मक ज्वार के साथ हुआ। हमारे पड़ोस में भी सीलोन ने अपना नाम श्रीलंका और बर्मा ने म्यांमा कर लिया। खुद ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी आधिकारिक संज्ञा बदल कर यूनाइटेड किंगडम की। इन सबके पीछे गहरी सांस्कृतिक, राजनीतिक भावनाएं होती हैं।
हमारे देश में भी शब्द और नाम गंभीर माने रखते हैं। अंग्रेजों ने यहां अपने शासकों, जनरलों के नाम पर असंख्य स्थानों के नाम रखे, कवियों-कलाकारों के नाम पर नहीं। फिर, जब 1940 में मुसलिम लीग ने मुसलमानों के अलग देश की मांग की और आखिरकार उसे लिया तो उसका नाम पाकिस्तान रखा। जैसा जर्मनी, कोरिया आदि के विभाजनों में हुआ था- पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया- वे भी नए देश का नाम ‘पश्चिमी भारत’ या ‘पश्चिमी हिंदुस्तान’ रख सकते थे। पर उन्होंने अलग मजहबी नाम रखा। इसके पीछे एक पहचान छोड़ने और दूसरी अपनाने की चाहत थी। यहां तक कि अपने को मुगलों का उत्तराधिकारी मानते हुए भी मुसलिम नेताओं ने मुगलिया शब्द ‘हिंदुस्तान’ भी नहीं अपनाया। क्यों?
इसलिए कि शब्द कोई उपयोगिता के निर्जीव उपकरण नहीं होते। वे किसी भाषा और संस्कृति की थाती होते हैं। कई शब्द तो अपने आप में संग्रहालय होते हैं, जिनमें किसी समाज की सहस्रों वर्ष पुरानी परंपरा, स्मृति, रीति और ज्ञान संघनित रहता है। इसीलिए जब कोई किसी भाषा या शब्द को छोड़ता है तो जाने-अनजाने उसके पीछे की पूरी अच्छी या बुरी परंपरा भी छोड़ता है। इसीलिए श्रीलंका ने ‘सीलोन’ को त्याग कर औपनिवेशिक दासता के अवशेष से मुक्ति पाने का प्रयास किया। हमने वह आज तक नहीं किया है।
सन 1947 में हमसे जो सबसे बड़ी भूलें हुईं उनमें से एक यह थी कि स्वतंत्र होने के बाद भी देश का नाम ‘इंडिया’ रहने दिया। लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वान संपादक गिरिलाल जैन ने लिखा था कि स्वतंत्र भारत में इंडिया नामक इस ‘एक शब्द ने भारी तबाही की’। यह बात उन्होंने इस्लामी समस्या के संदर्भ में लिखी थी। अगर देश का नाम भारत होता, तो भारतीयता से जुड़ने के लिए यहां किसी से अनुरोध नहीं करना पड़ता! गिरिलाल जी के अनुसार, इंडिया ने पहले इंडियन और हिंदू को अलग कर दिया। उससे भी बुरा यह कि उसने ‘इंडियन’ को हिंदू से बड़ा बना दिया। अगर यह न हुआ होता तो आज सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी, ह्यूमन राइट्स और मल्टी-कल्टी का शब्द-जाल और फंदा रचने वालों का काम इतना सरल न रहा होता। अगर देश का नाम भारत या हिंदुस्तान भी रहता तो इस देश के मुसलमान स्वयं को भारतीय मुसलमान कहते। इन्हें अरब में अब भी ‘हिंदवी’ या ‘हिंदू मुसलमान’ ही कहा जाता है। सदियों से विदेशी लोग भारतवासियों को ‘हिंदू’ ही कहते रहे और आज भी कहते हैं।
यह पूरी दुनिया में हमारी पहचान है, जिससे मुसलमान भी जुड़े थे। क्योंकि वे सब हिंदुओं से धर्मांतरित हुए भारतीय ही हैं (यह महात्मा गांधी ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं)। अगर देश का सही नाम पुनर्स्थापित कर लिया जाता, तो आज भी मुसलमान स्वयं को हिंदू या हिंदवी ही कहते जो एक ही बात है। यह विचित्र है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे अनेक प्रांतों और शहरों के नाम बदले, लेकिन देश का नाम यथावत छोड़ा हुआ है। जिन लोगों ने मद्रास को तमिलनाडु, बोंबे को मुंबई, कैलकटा को कोलकाता या बैंगलोर को बंगलुरु, उड़ीसा को ओडीशा आदि पुनर्नामांकित करना जरूरी समझा- उन्हें सबसे पहले इंडिया शब्द को विस्थापित करना चाहिए था। क्योंकि यह वह शब्द है जो हमें पददलित करने और दास बनाने वालों ने हम पर थोपा था।
विदेशियों द्वारा जबरन दिए गए नामों को त्यागना अच्छा ही नहीं, आवश्यक भी है। इसमें अपनी पहचान के महत्त्व और उसमें गौरव की भावना है। इसीलिए अब तक जब भी भारत में औपनिवेशिक नामों को बदल स्वदेशी नाम अपनाए गए, हमारे देश के अंग्रेजी-प्रेमी और पश्चिमोन्मुखी वर्ग ने विरोध नहीं किया है। पर यह उन्हें पसंद भी नहीं आया। क्योंकि वे जानते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ऐसे में एक दिन अंग्रेजी को भी राज-सिंहासन से उतरना पड़ेगा। इसीलिए, जब देश का नाम पुनर्स्थापित करने की बात उठेगी, वे विरोध करेंगे। चाहे इंडिया को बदलकर भारतवर्ष करने में किसी भाषा, क्षेत्र, जाति या संप्रदाय को आपत्ति न हो। वैसे भी भारतवर्ष ऐसा शब्द है जो भारत की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होता रहा है। बल्कि जिस कारण मद्रास, बोम्बे, कैलकटा, त्रिवेंद्रम आदि को बदला गया, वह कारण देश का नाम बदलने के लिए और भी उपयुक्त है। इंडिया शब्द भारत पर ब्रिटिश शासन का सीधा ध्यान दिलाता है। आधिकारिक नाम में इंडिया का पहला प्रयोग ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ में किया गया था जिसने हमें गुलाम बना कर दुर्गति की। पर जब वह इस देश में व्यापार करने आई थी तो यह देश स्वयं को भारतवर्ष या हिंदुस्तान कहता था। क्या हम अपना नाम भी अपना नहीं रखा सकते?
अगर देश का नाम पुन: भारतवर्ष कर लिया जाए तो यह हम सब को स्वत: इस भूमि की गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति से जोड़ता रहेगा जो पूरे विश्व में अनूठी है। अन्यथा आज हमें अपनी ही थाती के बचाव के लिए उन मूढ़ रेडिकलों,वामपंथियों, मिशनरी एजेंटों, ग्लोबल सिटिजनों से बहस करनी पड़ती है जो हर विदेशी नारे को हम पर थोपने और हमें किसी न किसी बाहरी सूत्रधार का अनुचर बनाने के लिए लगे रहते हैं।
इसीलिए जब देश का नाम भारतवर्ष या हिंदुस्तान करने का प्रयास होगा- इसका सबसे कड़ा विरोध यही सेक्युलर-वामपंथी बौद्धिक करेंगे। उन्हें ‘भारतीयता’ और ‘हिंदू’ शब्द और इनके भाव से घोर शत्रुता है। यही उनकी मूल सैद्धांतिक टेक है। इसीलिए चाहे वे कैलकटा, बांबे आदि पर विरोध न कर सकें, पर इंडिया को बदलने के प्रस्ताव पर वे चुप नहीं बैठेंगे। यह इसका एक और प्रमाण होगा कि नामों के पीछे कितनी बड़ी सांस्कृतिक, राजनीतिक मनोभावनाएं रहती हैं। वस्तुत: समस्या यही है कि जिस प्रकार कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के लिए स्थानीय जनता की सशक्त भावना थी, उस प्रकार भारतवर्ष के लिए नहीं दिखती। इसलिए नहीं कि इसकी चाह रखने वाले देश में कम हैं। बल्कि ठीक इसीलिए कि भारतवर्ष की भावना कोई स्थानीयता की नहीं, राष्ट्रीयता की भावना है। लिहाजा, देशभक्ति और राष्ट्रवाद से किसी न किसी कारण दूर रहने वाले, या किसी न किसी प्रकार के ‘अंतरराष्ट्रीयतावाद’ से अधिक जुड़ाव रखने वाले उग्र होकर इसका विरोध करेंगे।
यानी चूंकि इंडिया शब्द को बदल कर भारतवर्ष करना राष्ट्रीय प्रश्न है, इसीलिए राष्ट्रीय भाव को कमतर मानने वाली विचारधाराएं, हर तरह के गुट और गिरोह एकजुट होकर इसका प्रतिकार करेंगे। वे हर तरह की ‘अल्पसंख्यक’ भावना उभारेंगे और आधुनिकता के तर्क लाएंगे।
वैसे भी, उत्तर भारत की सांस्कृतिक-राजनीतिक चेतना और स्वाभिमान मंद है। यहां वैचारिक दासता, आपसी कलह, विश्वास, भेद और क्षुद्र स्वार्थ अधिक है। इन्हीं पर विदेशी, हानिकारक विचारों का भी अधिक प्रभाव है। वे बाहरी हमलावरों, पराए आक्रामक विचारों आदि के सामने झुक जाने, उनके दीन अनुकरण को ही ‘समन्वय’, ‘संगम’, ‘अनेकता में एकता’ आदि बताते रहे हैं। यह दासता भरी आत्मप्रवंचना है।
डॉ राममनोहर लोहिया ने आजीवन इसी आत्मप्रवंचना की सर्वाधिक आलोचना की थी जो विदेशियों से हार जाने के बाद ‘आत्मसमर्पण को सामंजस्य’ बताती रही है। अत: इस कथित हिंदी क्षेत्र से किसी पहलकदमी की आशा नहीं। इनमें अपने वास्तविक अवलंब को पहचानने और टिकने के बदले हर तरह के विदेशी विचारों, नकलों, दुराशाओं, शत्रु शक्तियों की सदाशयता पर आस लगाने की प्रवृत्ति है। इसीलिए उनमें भारतवर्ष नाम की पुनर्स्थापना की कोई ललक या चाह भी आज तक नहीं जगी है। अच्छा हो कि देश का नाम पुनर्स्थापित करने का अभियान किसी तमिल, मराठी या कन्नड़ हस्ती की ओर से आरंभ हो। यहां काम दक्षिण अफ्रीका की तुलना में आसान है, पर हमारा आत्मबल क्षीण है।
(जनसत्ता से साभार)


 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नया कारनामा. अब स्कूल में बच्चों को गीता पढना ज़रूरी है. क्या बात है, ये फैसला करके उन्होंने भगवान् कृष्ण से अपने लिए बहुत कुछ डिमांड कर डाला होगा, आखिर हमारे यहाँ धर्म का मतलब आम तौर पर मन्नत मांगना ही तो होता है और हमारे मुख्यमंत्री तो 'सिर्फ धार्मिक' ही हैं. ये अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम वापस अपने प्रिय मुख्यमंत्रीजी पर वापस आते हैं. गीता तो आपने थोप दी लेकिन क्या आपको खबर है कि जो पढाई ज़रूरी है एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए वो भी हो रही है या नहीं? स्वाभाविकतः नहीं, वरना मध्यप्रदेश को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में एक नहीं गिना जाता. ये तथ्य है कि मध्यप्रदेश के बच्चों को बाहर जाकर प्रतियोगिता करना भारी पड़ता है. लेकिन मुख्यमंत्रीजी को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि उन्होंने इतना सोचा भी होगा मुझे नहीं लगता. उनके अब तक के कार्यकाल में उन्होंने जो भी काम किये हैं वे उनकी बेहद सतही सोच को ही दर्शाते हैं. वो एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि किसी मोहल्ले की गणेश मंडली के अध्यक्ष की तरह सोचते हैं और राज्य को गणेश मंडल की तरह चला रहे हैं. स्कूलों में गीता पढ़वाएंगे लेकिन शिक्षक की जो फटीचर हालत है वो नहीं देखेंगे. प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम मेहनताना मिलता है उसमे वो क्या शिक्षा देगा बच्चों को. सच्चाई तो ये है कि जो आदमी किसी भी काम के योग्य नहीं होता (शिक्षक बनने के भी ) वो शिक्षक बन जाता है. सभी हारे हुए और अयोग्य लोग शिक्षा देने के धंधे में लगे हुए हैं तो कोई आश्चर्य नहीं कि पूरे राज्य की तस्वीर भी ऐसी ही है. मुख्यमंत्री भी ऐसे ही शिक्षकों का परिणाम लगते हैं जिन्होंने शिक्षा में विचार को कभी जगह ही नहीं दी. वैसे तो मुख्यमंत्रीजी बहुत ही लचीले हैं जिन्होंने कभी कोई मजबूत फैसला नहीं लिया लेकिन अब तक जिन बातों पर वे कड़क हुए हैं वे उनकी सोच के दीवालियेपन को ही दिखाती हैं. बानगी देखिये - जब राज्य में १ महीने तक बारिश नहीं होती तो वे महांकाल के मंदिर में जाकर ५०००० पंडों के साथ भोजन करते हैं और भगवन को बारिश की अर्जी देते हैं. अब एक आम आदमी को इस तरह की हरकत के लिए मूर्ख होने का तमगा देकर माफ़ किया जा सकता है लेकिन एक राज्य के मुखिया को नहीं. लेकिन इस एक काम के सिवा मुख्यमंत्रीजी ने पानी के मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया, उन्हें अब भी पानी का मेनेजमेंट पूरी तरह भगवन के हाथ में ही लगता है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमें ही कुछ नियम बनाने होंगे, कुछ कदम उठाने होंगे ताकि सही समय पर बारिश हो और पर्याप्त हो. मालवा में भूमिगत जलस्तर भयावह स्थिति में है लेकिन वे बेखबर हैं उन्हें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवन विष्णु अपने नाग पर नीचे बैठे हैं जो पानी कम नहीं होने देंगे. राज्य में पेडों की कटाई कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि ये किसी काम के हैं. दूसरी ज़ोरदार आवाज़ उन्होंने उठाई थी एक मसाज सेंटर के बोर्ड के खिलाफ....?????....क्या कर रहे हैं ये आप? आपको राज्य की बागडोर इन ओछे कामों के लिए नहीं सौंपी गई है. आपका राज्य बहुत बहुत पिछड़ा हुआ है, कभी अपने कुए से बाहर निकल कर देखिये कि दुनिया बहुत बड़ी है. अपने आप को ऊपर उठाइये, अपने कुए को और गहरा मत खोदिये. लाडली लक्ष्मी योजना को क़ानून बनाने के लिए वे बहुत आक्रामक नज़र आये लेकिन राज्य में जो गुंडों का साम्राज्य फ़ैल गया है (जिसके आका उन्ही कि पार्टी और सरकार के लोग हैं) उस पर गौर करना उन्हें ज़रूरी नहीं लगता. जहाँ भी कोई सोच-समझ से सम्बंधित मुद्दा सामने आता है वे केंद्र सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल कर सो जाते हैं. ८ साल हो गए हैं उनके शासन को लेकिन प्रदेश में बिजली की समस्या में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया है बल्कि हालात और भी बदतर हुए हैं. पहले सर्दियों में तो बिजली मिल जाती थी अब तो पूरे साल बिजली मेहमान कि तरह आती है. लेकिन ये समस्या केंद्र सरकार कि है, हम तो बस मंदिर जायेंगे और धर्म बचायेंगे तो भाई पुजारी बन जाओ मुख्यमंत्री बन कर इतने लोगों की ज़िन्दगी क्यों खराब करते हो? कहने को तो उन्होंने अपनी एक वेब साईट भी बनाई है और उस पर नागरिक अपनी समस्याएँ बता सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता की कोई कभी उसे देखने की ज़हमत भी उठाता होगा क्योंकि उनके आस-पास के लोग भी तो उभी की तरह के होंगे न जो भगवन भरोसे काम कर रहे हैं. मैंने कई बार उस पर पत्र लिखे लेकिन मुझे आज तक कोई जवाब नहीं आया.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नया कारनामा. अब स्कूल में बच्चों को गीता पढना ज़रूरी है. क्या बात है, ये फैसला करके उन्होंने भगवान् कृष्ण से अपने लिए बहुत कुछ डिमांड कर डाला होगा, आखिर हमारे यहाँ धर्म का मतलब आम तौर पर मन्नत मांगना ही तो होता है और हमारे मुख्यमंत्री तो 'सिर्फ धार्मिक' ही हैं. ये अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम वापस अपने प्रिय मुख्यमंत्रीजी पर वापस आते हैं. गीता तो आपने थोप दी लेकिन क्या आपको खबर है कि जो पढाई ज़रूरी है एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए वो भी हो रही है या नहीं? स्वाभाविकतः नहीं, वरना मध्यप्रदेश को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में एक नहीं गिना जाता. ये तथ्य है कि मध्यप्रदेश के बच्चों को बाहर जाकर प्रतियोगिता करना भारी पड़ता है. लेकिन मुख्यमंत्रीजी को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि उन्होंने इतना सोचा भी होगा मुझे नहीं लगता. उनके अब तक के कार्यकाल में उन्होंने जो भी काम किये हैं वे उनकी बेहद सतही सोच को ही दर्शाते हैं. वो एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि किसी मोहल्ले की गणेश मंडली के अध्यक्ष की तरह सोचते हैं और राज्य को गणेश मंडल की तरह चला रहे हैं. स्कूलों में गीता पढ़वाएंगे लेकिन शिक्षक की जो फटीचर हालत है वो नहीं देखेंगे. प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम मेहनताना मिलता है उसमे वो क्या शिक्षा देगा बच्चों को. सच्चाई तो ये है कि जो आदमी किसी भी काम के योग्य नहीं होता (शिक्षक बनने के भी ) वो शिक्षक बन जाता है. सभी हारे हुए और अयोग्य लोग शिक्षा देने के धंधे में लगे हुए हैं तो कोई आश्चर्य नहीं कि पूरे राज्य की तस्वीर भी ऐसी ही है. मुख्यमंत्री भी ऐसे ही शिक्षकों का परिणाम लगते हैं जिन्होंने शिक्षा में विचार को कभी जगह ही नहीं दी. वैसे तो मुख्यमंत्रीजी बहुत ही लचीले हैं जिन्होंने कभी कोई मजबूत फैसला नहीं लिया लेकिन अब तक जिन बातों पर वे कड़क हुए हैं वे उनकी सोच के दीवालियेपन को ही दिखाती हैं. बानगी देखिये - जब राज्य में १ महीने तक बारिश नहीं होती तो वे महांकाल के मंदिर में जाकर ५०००० पंडों के साथ भोजन करते हैं और भगवन को बारिश की अर्जी देते हैं. अब एक आम आदमी को इस तरह की हरकत के लिए मूर्ख होने का तमगा देकर माफ़ किया जा सकता है लेकिन एक राज्य के मुखिया को नहीं. लेकिन इस एक काम के सिवा मुख्यमंत्रीजी ने पानी के मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया, उन्हें अब भी पानी का मेनेजमेंट पूरी तरह भगवन के हाथ में ही लगता है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमें ही कुछ नियम बनाने होंगे, कुछ कदम उठाने होंगे ताकि सही समय पर बारिश हो और पर्याप्त हो. मालवा में भूमिगत जलस्तर भयावह स्थिति में है लेकिन वे बेखबर हैं उन्हें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवन विष्णु अपने नाग पर नीचे बैठे हैं जो पानी कम नहीं होने देंगे. राज्य में पेडों की कटाई कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि ये किसी काम के हैं. दूसरी ज़ोरदार आवाज़ उन्होंने उठाई थी एक मसाज सेंटर के बोर्ड के खिलाफ....?????....क्या कर रहे हैं ये आप? आपको राज्य की बागडोर इन ओछे कामों के लिए नहीं सौंपी गई है. आपका राज्य बहुत बहुत पिछड़ा हुआ है, कभी अपने कुए से बाहर निकल कर देखिये कि दुनिया बहुत बड़ी है. अपने आप को ऊपर उठाइये, अपने कुए को और गहरा मत खोदिये. लाडली लक्ष्मी योजना को क़ानून बनाने के लिए वे बहुत आक्रामक नज़र आये लेकिन राज्य में जो गुंडों का साम्राज्य फ़ैल गया है (जिसके आका उन्ही कि पार्टी और सरकार के लोग हैं) उस पर गौर करना उन्हें ज़रूरी नहीं लगता. जहाँ भी कोई सोच-समझ से सम्बंधित मुद्दा सामने आता है वे केंद्र सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल कर सो जाते हैं. ८ साल हो गए हैं उनके शासन को लेकिन प्रदेश में बिजली की समस्या में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया है बल्कि हालात और भी बदतर हुए हैं. पहले सर्दियों में तो बिजली मिल जाती थी अब तो पूरे साल बिजली मेहमान कि तरह आती है. लेकिन ये समस्या केंद्र सरकार कि है, हम तो बस मंदिर जायेंगे और धर्म बचायेंगे तो भाई पुजारी बन जाओ मुख्यमंत्री बन कर इतने लोगों की ज़िन्दगी क्यों खराब करते हो? कहने को तो उन्होंने अपनी एक वेब साईट भी बनाई है और उस पर नागरिक अपनी समस्याएँ बता सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता की कोई कभी उसे देखने की ज़हमत भी उठाता होगा क्योंकि उनके आस-पास के लोग भी तो उभी की तरह के होंगे न जो भगवन भरोसे काम कर रहे हैं. मैंने कई बार उस पर पत्र लिखे लेकिन मुझे आज तक कोई जवाब नहीं आया.  हिंदी शायद संसार की इकलौती ऐसी भाषा है जिसके परजीवी मलाई-रबड़ी पर पलते हैं और श्रमजीवी आर्थिक तंगी, अभाव, वंचना और अपमान का शिकार होते हैं। यह कड़वा सच है कि हिन्दी को जिन मनीषियों ने आधुनिक दृष्टि दी, नये मुहावरों, वाक्य-विन्यासों से लैस किया, अपने कृतित्व के जरिए जिन्होंने हिंदी को जनता की जुबान बना दी, उन्हें अपमानित, प्रताडि़त और विक्षिप्त होना पड़ा। उनमें से ज्यादातर मनीषियों को ताउम्र दो वक्त की रोटी की जद्दोजहज के बीच एक कठिन जिद के बूते अपनी रचनात्मक प्रतिभा को बचाए रखना पड़ा। एक ऐसी भाषा जिसमें साँस लेते हुए रघुवीर सहाय अपमानित हुए, मुक्तिबोध अभाव, वंचना और लंबी बीमारी से ग्रस्त होकर मरे, महाकवि निराला अर्द्ध-विक्षिप्त हुए और भुवनेश्वर ने मानसिक संतुलन खोकर भीख मांगते हुए दम तोड़ा। इसके उलट जो परजीवी हुए, प्रबंधन कुशल रहे वे हिन्दी की मलाई-रबड़ी खा-खाकर अघाते रहे।
हिंदी शायद संसार की इकलौती ऐसी भाषा है जिसके परजीवी मलाई-रबड़ी पर पलते हैं और श्रमजीवी आर्थिक तंगी, अभाव, वंचना और अपमान का शिकार होते हैं। यह कड़वा सच है कि हिन्दी को जिन मनीषियों ने आधुनिक दृष्टि दी, नये मुहावरों, वाक्य-विन्यासों से लैस किया, अपने कृतित्व के जरिए जिन्होंने हिंदी को जनता की जुबान बना दी, उन्हें अपमानित, प्रताडि़त और विक्षिप्त होना पड़ा। उनमें से ज्यादातर मनीषियों को ताउम्र दो वक्त की रोटी की जद्दोजहज के बीच एक कठिन जिद के बूते अपनी रचनात्मक प्रतिभा को बचाए रखना पड़ा। एक ऐसी भाषा जिसमें साँस लेते हुए रघुवीर सहाय अपमानित हुए, मुक्तिबोध अभाव, वंचना और लंबी बीमारी से ग्रस्त होकर मरे, महाकवि निराला अर्द्ध-विक्षिप्त हुए और भुवनेश्वर ने मानसिक संतुलन खोकर भीख मांगते हुए दम तोड़ा। इसके उलट जो परजीवी हुए, प्रबंधन कुशल रहे वे हिन्दी की मलाई-रबड़ी खा-खाकर अघाते रहे। लव, सेक्स और धोखा....नाम बेहद अजीब है...उस दौर में जब हर हिंदी फिल्म के साथ अंग्रेजी टैग का रिवाज़ हो....हालांकि, फिल्म देखने के बाद साफ़ हो गया कि लव सेक्स और धोखा आजकल के फ़टाफ़ट संबंधों का कच्चा चिटठा है....फ़टाफ़ट संबंधों में पहले फ़टाफ़ट लव होता है, फिर सेक्स होता है और फिर एक तयशुदा धोखा....(जैसा कर्म करोगे, वैसा फल मिलेगा टाइप)....लव आजकल और कमीने से एक कदम आगे की फिल्म....अब सीधे-सीधे फिल्म की कहानी कहने का दौर रहा नहीं.....कि कैमरा ऑन किया, एक्शन बोला और एक लम्बा सा सीन चालू
लव, सेक्स और धोखा....नाम बेहद अजीब है...उस दौर में जब हर हिंदी फिल्म के साथ अंग्रेजी टैग का रिवाज़ हो....हालांकि, फिल्म देखने के बाद साफ़ हो गया कि लव सेक्स और धोखा आजकल के फ़टाफ़ट संबंधों का कच्चा चिटठा है....फ़टाफ़ट संबंधों में पहले फ़टाफ़ट लव होता है, फिर सेक्स होता है और फिर एक तयशुदा धोखा....(जैसा कर्म करोगे, वैसा फल मिलेगा टाइप)....लव आजकल और कमीने से एक कदम आगे की फिल्म....अब सीधे-सीधे फिल्म की कहानी कहने का दौर रहा नहीं.....कि कैमरा ऑन किया, एक्शन बोला और एक लम्बा सा सीन चालू शास्त्रों को एक तरफ कर दें, तो भी इस पुरुष-प्रधान समाज में नारी-वेदना का एक लंबा इतिहास रहा है। केवल उदहारण के तौर पर सही, कोई सन् 1891 में ब्रिटिश द्वारा पारित ‘Age of Consent Bill’ को ही एक नज़र देख ले. यह बिल मुख्यतः पूना व बंगाल के समाज सुधारकों द्वारा दो दशक से भी अधिक तक चलाए गए अथक अभियान के बाद पारित हुआ. तत्कालीन ‘हिंदू विवाह अधिनियम’ (1860) के अनुसार किसी भी विवाहित लड़की का पति तब तक उस का शारीरिक संभोग नहीं कर सकता, जब तक कि वह 10 वर्ष की आयु की न हो जाए. सुधारकों ने इस बात के कड़े प्रयत्न शुरू कर दिये कि यह आयु कुछ वर्ष बढ़ाई जाए. बंबई में एक दस वर्ष व कुछ महीनों की लड़की के पति ने उस का संभोग किया तो वह इस प्रक्रिया को न सहन कर के मर गई. पुलिस ने उस के पति को गिरफ्तार कर के बलात्कार व हत्या का मुकदमा चलाया. लेकिन अदालत ने उसे इसीलिये बरी कर दिया कि कानूनन, वह लड़की क्योंकि दस वर्ष से बड़ी थी, इसलिए यह मृत्यु मात्र एक दुर्भाग्य है और पति किसी प्रकार के दंड का भोगी नहीं हो सकता. अंततः सुधारकों के गहरे प्रयासों के बाद ब्रिटिश ने विधेयक पारित कर के यह आयु दस से बढ़ा कर बारह कर दी. दुर्भाग्य कि देश के शास्त्रांध लोगों के गले यह विधेयक उतर नहीं पा रहा था. उन सब को पृथ्वी बुरी तरह कांपती महसूस हुई और लगा जैसे देवता सहसा खून के आंसू बहाने लगे हैं. नतीजतन इस विधेयक के विरुद्ध रैलियों का एक तांता लग गया. इस विधेयक के कड़े से कड़े विरोधियों में सब से अग्रणी थे लोकमान्य तिलक, जिन्होंने विधेयक की तथा उन तमाम लोगों की कड़ी भर्त्सना की जो कह रहे थे कि विधेयक किसी भी प्रकार से शास्त्रों की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाता. तिलक- अनुयायियों के कोप का भाजन बने प्रसिद्ध सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, जिन का एक पुतला बना कर पुतले के एक हाथ में उबला हुआ अंडा और दूसरे में व्हिस्की की बोतल पकड़ा दी गई, ताकि वे ब्रिटिश की पश्चिमी संस्कृति के पिट्ठू से नज़र आएं ! पुतले को पूरे शहर में घुमाया गया और उस का अन्तिम संस्कार कर दिया गया। सुधारकों को तिलक यह कह कर लताड़ने लगे कि ‘अगर आप शास्त्रों के बारे में पता ही नहीं तो बेहतर कि आप सब अपनी ज़बान न खोलें’. कलकत्ता में दो लाख लोगों की एक महारैली होनी लगी और खूब त्राहि त्राहि मच गई. सुधारकों पर ढेरों ज़हर उगलने के बाद अनेक तो ऐसे भी थे जो एक शिष्ट-मंडल लंदन भेजना चाहते थे कि वहां जा कर महारानी विक्टोरिया के आगे साष्टांग प्रणाम किया जाए और उन्हें नमन कर के प्रार्थना की जाए कि कृपया हमारी ‘हिंदू सभ्यता’ को बचा लें! तिलक एक महान देशभक्त थे, लेकिन एक बार जब पूना में महिला-शिक्षा के विषय पर वाद-विवाद के उद्देश्य से एक जनसभा का आयोजन किया गया, तब तिलक समर्थक हर उस वक्ता की हूटिंग करने लगे, जो महिला-शिक्षा के पक्ष में बोल रहा था. यहाँ तक कि जब सभा में उपस्थित दो महिला विचारक भी बारी बारी बोलने आई तो सुधार-विरोधियों ने उन की भी हूटिंग कर दी. तिलक ने इसीलिये महिला-शिक्षा समर्थकों का इतना कोप अर्जित कर लिया कि वे जब स्वयं बोलने आए तो मंच पर टमाटरों, चप्पलों और अण्डों की धुआंधार वर्षा होने लगी. एक पोलिस- इंस्पेक्टर को मंच पर फुर्ती से छलांग लगानी पडी और तिलक को बांहों के घेरे में में घेर कर किसी प्रकार मंच से कहीं सुरक्षित जगह ले जाना पड़ा.
शास्त्रों को एक तरफ कर दें, तो भी इस पुरुष-प्रधान समाज में नारी-वेदना का एक लंबा इतिहास रहा है। केवल उदहारण के तौर पर सही, कोई सन् 1891 में ब्रिटिश द्वारा पारित ‘Age of Consent Bill’ को ही एक नज़र देख ले. यह बिल मुख्यतः पूना व बंगाल के समाज सुधारकों द्वारा दो दशक से भी अधिक तक चलाए गए अथक अभियान के बाद पारित हुआ. तत्कालीन ‘हिंदू विवाह अधिनियम’ (1860) के अनुसार किसी भी विवाहित लड़की का पति तब तक उस का शारीरिक संभोग नहीं कर सकता, जब तक कि वह 10 वर्ष की आयु की न हो जाए. सुधारकों ने इस बात के कड़े प्रयत्न शुरू कर दिये कि यह आयु कुछ वर्ष बढ़ाई जाए. बंबई में एक दस वर्ष व कुछ महीनों की लड़की के पति ने उस का संभोग किया तो वह इस प्रक्रिया को न सहन कर के मर गई. पुलिस ने उस के पति को गिरफ्तार कर के बलात्कार व हत्या का मुकदमा चलाया. लेकिन अदालत ने उसे इसीलिये बरी कर दिया कि कानूनन, वह लड़की क्योंकि दस वर्ष से बड़ी थी, इसलिए यह मृत्यु मात्र एक दुर्भाग्य है और पति किसी प्रकार के दंड का भोगी नहीं हो सकता. अंततः सुधारकों के गहरे प्रयासों के बाद ब्रिटिश ने विधेयक पारित कर के यह आयु दस से बढ़ा कर बारह कर दी. दुर्भाग्य कि देश के शास्त्रांध लोगों के गले यह विधेयक उतर नहीं पा रहा था. उन सब को पृथ्वी बुरी तरह कांपती महसूस हुई और लगा जैसे देवता सहसा खून के आंसू बहाने लगे हैं. नतीजतन इस विधेयक के विरुद्ध रैलियों का एक तांता लग गया. इस विधेयक के कड़े से कड़े विरोधियों में सब से अग्रणी थे लोकमान्य तिलक, जिन्होंने विधेयक की तथा उन तमाम लोगों की कड़ी भर्त्सना की जो कह रहे थे कि विधेयक किसी भी प्रकार से शास्त्रों की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाता. तिलक- अनुयायियों के कोप का भाजन बने प्रसिद्ध सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, जिन का एक पुतला बना कर पुतले के एक हाथ में उबला हुआ अंडा और दूसरे में व्हिस्की की बोतल पकड़ा दी गई, ताकि वे ब्रिटिश की पश्चिमी संस्कृति के पिट्ठू से नज़र आएं ! पुतले को पूरे शहर में घुमाया गया और उस का अन्तिम संस्कार कर दिया गया। सुधारकों को तिलक यह कह कर लताड़ने लगे कि ‘अगर आप शास्त्रों के बारे में पता ही नहीं तो बेहतर कि आप सब अपनी ज़बान न खोलें’. कलकत्ता में दो लाख लोगों की एक महारैली होनी लगी और खूब त्राहि त्राहि मच गई. सुधारकों पर ढेरों ज़हर उगलने के बाद अनेक तो ऐसे भी थे जो एक शिष्ट-मंडल लंदन भेजना चाहते थे कि वहां जा कर महारानी विक्टोरिया के आगे साष्टांग प्रणाम किया जाए और उन्हें नमन कर के प्रार्थना की जाए कि कृपया हमारी ‘हिंदू सभ्यता’ को बचा लें! तिलक एक महान देशभक्त थे, लेकिन एक बार जब पूना में महिला-शिक्षा के विषय पर वाद-विवाद के उद्देश्य से एक जनसभा का आयोजन किया गया, तब तिलक समर्थक हर उस वक्ता की हूटिंग करने लगे, जो महिला-शिक्षा के पक्ष में बोल रहा था. यहाँ तक कि जब सभा में उपस्थित दो महिला विचारक भी बारी बारी बोलने आई तो सुधार-विरोधियों ने उन की भी हूटिंग कर दी. तिलक ने इसीलिये महिला-शिक्षा समर्थकों का इतना कोप अर्जित कर लिया कि वे जब स्वयं बोलने आए तो मंच पर टमाटरों, चप्पलों और अण्डों की धुआंधार वर्षा होने लगी. एक पोलिस- इंस्पेक्टर को मंच पर फुर्ती से छलांग लगानी पडी और तिलक को बांहों के घेरे में में घेर कर किसी प्रकार मंच से कहीं सुरक्षित जगह ले जाना पड़ा. 

 पिछले 6 दशकों से रचनाकर्म में सक्रिय राजेन्द्र यादव साहित्य में महानायक की हैसियत रखते हैं। साल 2006 में वरिष्ठ आलोचक आनंद प्रकाश और युवा कवि-लेखक रामजी यादव की टीम (पीपुल्स विजन प्रोडक्शन कम्पनी) ने राजेन्द्र यादव का लम्बा इंटरव्यू लिया। पीपुल्स विजन यादव जी के समग्र व्यक्तित्व और कृतित्व पर फिल्म बना रहा है। यदि आप भी इस प्रोजेक्ट से किसी भी तरह से जुड़ना चाहें तो रामजी यादव से (yadav.ramji2@gmail.com या 9015634902 पर) संपर्क करें। इस साक्षात्कार में राजेन्द्र यादव ने कविता की विलुप्ति, कहानी-नई कहानी, दलित और महिला लेखन, मार्क्सवाद की भारत में असफलता, साहित्य और राजनीति के पारस्परिक संबंधों इत्यादि पर खुलकर बोला। हमें यह साक्षात्कार संग्रहणीय लगा और यह भी लगा कि शायद हिन्द-युग्म के बहुत-से पाठक भी इसे सुनकर ऐसा महसूस करेंगे कि बहुत कुछ जानने और समझने को मिला।
पिछले 6 दशकों से रचनाकर्म में सक्रिय राजेन्द्र यादव साहित्य में महानायक की हैसियत रखते हैं। साल 2006 में वरिष्ठ आलोचक आनंद प्रकाश और युवा कवि-लेखक रामजी यादव की टीम (पीपुल्स विजन प्रोडक्शन कम्पनी) ने राजेन्द्र यादव का लम्बा इंटरव्यू लिया। पीपुल्स विजन यादव जी के समग्र व्यक्तित्व और कृतित्व पर फिल्म बना रहा है। यदि आप भी इस प्रोजेक्ट से किसी भी तरह से जुड़ना चाहें तो रामजी यादव से (yadav.ramji2@gmail.com या 9015634902 पर) संपर्क करें। इस साक्षात्कार में राजेन्द्र यादव ने कविता की विलुप्ति, कहानी-नई कहानी, दलित और महिला लेखन, मार्क्सवाद की भारत में असफलता, साहित्य और राजनीति के पारस्परिक संबंधों इत्यादि पर खुलकर बोला। हमें यह साक्षात्कार संग्रहणीय लगा और यह भी लगा कि शायद हिन्द-युग्म के बहुत-से पाठक भी इसे सुनकर ऐसा महसूस करेंगे कि बहुत कुछ जानने और समझने को मिला। 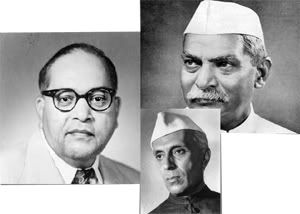 मंगलवार 9 मार्च 2010, ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ से एक दिन बाद का दिन भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब विश्व के सब से बड़े लोकतंत्र के उच्च-सदन ने बाबा साहब के संविधान में रेखांकित ‘समानता’ शब्द की प्रगति के लिए एक बड़ी छलांग लगाई है. राज्य सभा ने संविधान का 108 वां संशोधन बिल पारित कर दिया है, जिसके अनुसार देश की लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई. यह एक लंबे सफर के लिए उठाया गया मात्र पहला कदम होते हुए भी एक बड़ी छलांग माना जा रहा है क्योंकि निम्न-सदन लोकसभा की तरह उच्च-सदन को भी इसे दो तिहाई बहुमत से पारित करना था और ऐसा करना टेढ़ी खीर ही माना जा रहा था. यू.पी.ए सरकार के विलंबित तिकड़मों, शरद यादव की जनता दल (यू) में दो फाड़ा जिसके अंतर्गत नितीश कुमार ने पार्टी के फैसले के विरुद्ध बगावत का झंडा गाड़ दिया तथा अन्य कारणों से बिल को 186:1 मतों से पारित होने में सफलता मिल गई.
मंगलवार 9 मार्च 2010, ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ से एक दिन बाद का दिन भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब विश्व के सब से बड़े लोकतंत्र के उच्च-सदन ने बाबा साहब के संविधान में रेखांकित ‘समानता’ शब्द की प्रगति के लिए एक बड़ी छलांग लगाई है. राज्य सभा ने संविधान का 108 वां संशोधन बिल पारित कर दिया है, जिसके अनुसार देश की लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई. यह एक लंबे सफर के लिए उठाया गया मात्र पहला कदम होते हुए भी एक बड़ी छलांग माना जा रहा है क्योंकि निम्न-सदन लोकसभा की तरह उच्च-सदन को भी इसे दो तिहाई बहुमत से पारित करना था और ऐसा करना टेढ़ी खीर ही माना जा रहा था. यू.पी.ए सरकार के विलंबित तिकड़मों, शरद यादव की जनता दल (यू) में दो फाड़ा जिसके अंतर्गत नितीश कुमार ने पार्टी के फैसले के विरुद्ध बगावत का झंडा गाड़ दिया तथा अन्य कारणों से बिल को 186:1 मतों से पारित होने में सफलता मिल गई. श्वेता अग्रवाल फिल्म ‘शापित’ से पहले टर्की की एक फिल्म ‘मिरार’ में और ओलिवर पॉलिस की स्विस जर्मन फिल्म ‘तंदूरी लव’ में भी अभिनय कर चुकी हैं। ‘स्टार प्लस’ पर प्रसारित धारावाहिक ‘देखो मगर प्यार से’ में मोटी-सी लडकी के किरदार में नज़र आ चुकीं श्वेता अग्रवाल इन दिनों फिल्म सर्जक विक्रम भट्ट की खोज के रूप में उनकी आगामी फिल्म ‘शॉपित’ में अभिनय करके चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस फिल्म में उनके हीरो है मे मशहूर संगीतकार उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण हैं। देखा जाए तो यह फिल्म श्वेता के लिए डेब्यू होगी व अपनी बॉलीवुड की पहली ही फिल्म विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'शापित’ से कर रही है।
श्वेता अग्रवाल फिल्म ‘शापित’ से पहले टर्की की एक फिल्म ‘मिरार’ में और ओलिवर पॉलिस की स्विस जर्मन फिल्म ‘तंदूरी लव’ में भी अभिनय कर चुकी हैं। ‘स्टार प्लस’ पर प्रसारित धारावाहिक ‘देखो मगर प्यार से’ में मोटी-सी लडकी के किरदार में नज़र आ चुकीं श्वेता अग्रवाल इन दिनों फिल्म सर्जक विक्रम भट्ट की खोज के रूप में उनकी आगामी फिल्म ‘शॉपित’ में अभिनय करके चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस फिल्म में उनके हीरो है मे मशहूर संगीतकार उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण हैं। देखा जाए तो यह फिल्म श्वेता के लिए डेब्यू होगी व अपनी बॉलीवुड की पहली ही फिल्म विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'शापित’ से कर रही है। 
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने देश की आजादी में सराहनीय योगदान किया। स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनके नेताओं की भूमिका को राष्ट्र नकार नहीं सकता। आज कांग्रेस पार्टी अपना 125 वॉ जन्म वर्ष मना रही है। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसके संस्थापक ए0ओ0 ह्यूम जो एक रिटायर्ड अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे तथा प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डब्लू0सी0 बनर्जी हुए। ए0ओ0 ह्यूम, डब्लू सी0 बनर्जी से लेकर सोनियां गॉधी तक कांग्रेस पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। 1885 से लेकर 1905 तक लगातार 20 वर्षों तक कांग्रेस में उदारवादी गुट का प्रभाव रहा, जिसके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविन्द राना डे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय थे। 1905 से 1919 के मध्य नव राष्ट्रवाद तथा गरम पंथियों का उदय हुआ जिसके प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत राय (लाल-बाल-पाल) तथा अरविन्द घोष प्रमुख थे। लाल-बाल-पाल तथा अरविन्द्र घोष के प्रयासों के कारण प्रथम बार 1905 में कांग्रेस के बनारस राष्ट्रीय अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेश तथा 1906 के कलकत्ता राष्ट्रीय अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज की मांग रखी गयी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने देश की आजादी में सराहनीय योगदान किया। स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनके नेताओं की भूमिका को राष्ट्र नकार नहीं सकता। आज कांग्रेस पार्टी अपना 125 वॉ जन्म वर्ष मना रही है। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसके संस्थापक ए0ओ0 ह्यूम जो एक रिटायर्ड अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे तथा प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डब्लू0सी0 बनर्जी हुए। ए0ओ0 ह्यूम, डब्लू सी0 बनर्जी से लेकर सोनियां गॉधी तक कांग्रेस पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। 1885 से लेकर 1905 तक लगातार 20 वर्षों तक कांग्रेस में उदारवादी गुट का प्रभाव रहा, जिसके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविन्द राना डे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय थे। 1905 से 1919 के मध्य नव राष्ट्रवाद तथा गरम पंथियों का उदय हुआ जिसके प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत राय (लाल-बाल-पाल) तथा अरविन्द घोष प्रमुख थे। लाल-बाल-पाल तथा अरविन्द्र घोष के प्रयासों के कारण प्रथम बार 1905 में कांग्रेस के बनारस राष्ट्रीय अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेश तथा 1906 के कलकत्ता राष्ट्रीय अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज की मांग रखी गयी।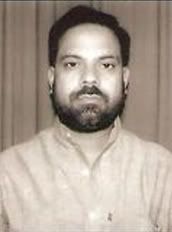 राघवेन्द्र सिंह
राघवेन्द्र सिंह मार्कण्डेय
मार्कण्डेय