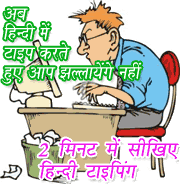~अभिषेक कश्यप*
भाग-5 से आगे॰॰॰॰
हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर लिखी समीक्षाओं-आलोचनाओं में ‘क्लैसिक’ शब्द पर बहुत जोर दिया जाता है। अखबारों के लिए समीक्षा लिखनेवाले कई नवसिखुए तो किसी ऐरे-गैरे के उपन्यास या कविता-संग्रह को क्लैसिक बताने में तनिक संकोच नहीं करते। यही नहीं, सरकारी पैसे पर शोध करने वाले विद्यार्थी और विश्वविद्यालयों में हिंदी की प्रोफेसरी करते हुए मोटी तनख्वाह, सामाजिक सुरक्षा-प्रतिष्ठा का भरपूर उपभोग करने वाले हमारे आलोचकगण भी अपनी परंपरागत विद्वता के बूते इस-उस किताब को क्लैसिक बताते रहते हैं। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि क्लैसिक का मतलब आखिर क्या है? दूसरे शब्दों में कहें तो किसी किताब या कृति को क्लैसिक कहने के मानदंड क्या हों?
इस मसले को लेकर पर्याप्त बहस और विवाद की गुंजाइश है। मगर कई साल पहले उर्दू के एक मशहूर लेखक ने किसी किताब के हवाले से क्लैसिक के बारे में जो बात कही, उसका मैं मुरीद हो गया। उन्होंने बताया-‘क्लैसिक वह कृति है, जो लोगों की जिन्दगी में इस कदर घुल-मिल जाए कि लोग उसमें अपने-अपने अर्थ निकालने लगें।’ मतलब ऐसी कृति जिसकी कहानी लोग अपने-अपने ढंग से कहने-सुनने लगें। किताब से बाहर लोगों की जिन्दगी पर जिसका ऐसा सर्वव्यापी असर हो कि हर शख्स के पास उसके परिवेश, घटनाओं और पात्रों की अपनी व्याख्याएं हों। ऐसी कृति जो जनमानस की सामूहिक स्मृतियों का निर्माण करे।
इस विचार की रोशनी में मैं आधुनिक हिंदी साहित्य की क्लैसिक मान ली गई कृतियों पर नजर डालता हूँ। सबसे पहले उपन्यासों की तरफ देखता हूँ- ‘गोदान’ (प्रेमचंद), ‘त्यागपत्र’ (जैनेंद्र कुमार), ‘मैला आंचल’ (फणीश्वर नाथ रेणु), ‘शेखर एक जीवनी’ (अज्ञेय), ‘सारा आकाश’ (राजेन्द्र यादव), ‘राग दरबारी’ (श्रीलाल शुक्ल), ‘कितने पाकिस्तान’ (कमलेश्वर), ‘नौकर की कमीज’ (विनोद कुमार शुक्ल) आदि......................फिर कहानियों की तरफ जाता हूँ- ‘उसने कहा था’ (चंद्रधर शर्मा गुलेरी), ‘पूस की रात’, ‘कफन’(प्रेमचंद), ‘भेडिय़े’ (भुवनेश्वर), ‘परिंदे’ (निर्मल वर्मा), ‘हत्यारे’ (अमरकान्त), ‘राजा निरबंसिया’ (कमलेश्वर),‘जहां लक्ष्मी कैद है’ (राजेन्द्र यादव), ‘टेपचू’, ‘तिरिछ’, ‘और अंत में प्रार्थना’ (उदय प्रकाश) आदि। कविताओं में तत्काल निराला की ‘सरोज स्मृति’, ‘राम की शक्ति पूजा’ और मुक्तिबोध की ‘अंधेरे में’ याद आती है।
मैं खुद से सवाल करता हूँ- ‘ऊपर मैंने आधुनिक हिंदी साहित्य की जिन निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण कृतियों के नाम दिए ... और भी अनेक कृतियां, स्थानाभाव की वजह से जिनके नाम यहां दे पाना संभव नहीं, में से कोई ऐसी कृति है, जनमानस पर जिसका असर तुलसीदास के ‘रामचरितमानस’, मीरा के पद या कबीर के दोहे जैसा हो?’
बिना किसी दुविधा के तत्काल इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है- ‘नहीं।’
यह कड़वी सच्चाई है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की कोई ऐसी कृति नहीं जो ‘रामचरितमानस’ की तरह जनता की स्मृतियों में रची-बसी हो, नि:संदेह ‘रामचरितमानस’ क्लैसिक है। कोई यह कह सकता है कि तुलसी, सुर, मीरा या कबीर ने लोक जीवन में रच-बस जाने के लिए वक्त की एक लंबी दूरी तय की है। जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की उम्र महज सौ-डेढ़ सौ बरस की है। हिंदी साहित्य के कई सुरमा आज गर्व से यह कहते नजर आते हैं कि दो सौ या पांच सौ साल बाद जिस लेखक की कृतियां बची रह जाएं वही ‘सच्चा लेखक’ होगा। अफसोस कि उनकी आंखें बंद हैं, इसलिए 200-500 साल के बाद की कौन कहे आज ही उनकी किताबें ढाई सौ-पाँच सौ प्रतियाँ छपती हैं और सरकारी पुस्तकालयों के कब्रगाह में कैद हो जाती हैं। अगर हम जानना चाहें तो भारतीय भाषाओं में ही कालजयी लेखकों और क्लैसिक कृतियों के कई उदाहरण मिल सकते हैं।
रवीन्द्रनाथ टैगोर और उनकी कृतियाँ बंगाली जनमानस में किस कदर रची-बसी हैं यह बताने की जरूरत नहीं। यही नहीं, हिंदी के लेखकों, शोध छात्रों और साहित्यिक पाठकों से इतर मैंने हिंदी भाषी प्रदेशों के आम लोगों के बीच जिस कहानी की सबसे ज्यादा चर्चा सुनी है वह हिंदी कथा साहित्य के प्रतीक-पुरुष प्रेमचंद की नहीं, बांग्ला उपन्यासकार शरतचंद्र की है- देवदास। मुझे ऐसे कई लोग मिले हैं जो शरतचंद्र को नहीं जानते, न ही यह जानते हैं कि ‘देवदास’ एक उपन्यास है। देवदास और पारो की प्रेमकथा को वे किसी उपन्यासकार की कल्पना नहीं बल्कि सच्ची कहानी मानते हैं, जो वास्तव में कभी घटी थी।
मैं समझता हूँ जो कृति ऐसा असर पैदा करे, वही क्लैसिक कही जा सकती है। दुनिया भर में ऐसे कई लेखक हैं जिनकी कृतियाँ क्लैसिक के इस मानदंड पर खरी उतरती हैं। चेखव की कई कहानियों में हर तबके के लोगों के सर चढक़र बोलने वाला जादू मौजूद है। महान लातिनी-अमेरिकी उपन्यासकार गैब्रियल गार्सिया माक्र्वेज का उपन्यास ‘हन्ड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिटयूड’ ऐसा ही क्लैसिक है जिसकी जादुई सफलता हैरतअंगेज है। वर्ष 1982 में ‘नोबल पुरस्कार’ से नवाजे गए इस उपन्यास की अब तक विभिन्न भाषाओं में ढाई करोड़ से ज्यादा प्रतियाँ बिक चुकी है। माक्र्वेज अभी जीवित हैं और किंवदंती बन चुके हैं। जो कोलंबिया गए हैं वे जानते हैं कि माक्र्वेज एक लेखक का नहीं, जनता में समाहित एक विचार का नाम है और ‘हन्ड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिटयूड’ सहित माक्र्वेज की कई कृतियाँ समीक्षाओं-आलोचनाओं से परे सचमुच क्लैसिक हैं यानी जनता की स्मृतियों में रच-बस गई हैं।
बेशक हिंदी को ऐसे लेखकों और ऐसी क्लैसिक कृतियों की सख्त दरकार है। आने वाले समय के लिए हिंदी साहित्य के लिए इससे अच्छी शुभकामना और क्या हो सकती है।


 इधर मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित कई बेस्टसेलर पढ़े। इनमें से ज्यादातर सेल्फ-हेल्प पुस्तकें थीं, जिन्हें भोपाल के मंजूल पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया है। पहली बार साल २००३ में मैंने नेपोलियन हिल की ‘थिंक एंड ग्रो रिच’ (हिंदी अनुवाद: सोचिए और अमीर बनिए) पढ़ी और तभी से मुझे ऐसी किताबों का चस्का लग गया। कुछ वैचारिक असहमतियों के बावजूद इनमें से ज्यादातर किताबों ने आइडिया, सहज भाषा-शैली और पाठकों को मुरीद बनाने के अपने कौशल की वजह से मुझे बार-बार अपनी ओर आकर्र्षित किया। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में अपने विलक्षण योगदान के लिए जाने जानेवाले अरविंद कुमार ने भी कुछ साल पहले अपना प्रकाशन शुरू किया है-‘अरविंद कुमार पब्लिशर्स।’ इस प्रकाशन के जरिए वे नए-नए विषयों की बेहद सुंदर, उपयोगी और पठनीय पुस्तकें किफायती दाम पर पाठकों को उपलब्ध करा रहे हैं। मगर अफसोस कि मंजूल, अरविंद कुमार पब्लिशर्स और ऐसे ऊंगलियों पर गिने जा सकने वाले चंद प्रकाशक पेशेगत विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए हिंदी में लीक से हटकर जो किताबें छाप रहे हैं, वह सब अंग्रेजी भाषा की बेस्टसेलर हैं। हिंदी में आकर्षक साज-सज्जा के साथ प्रकाशित इन किताबों के आवरण पर खासतौर से यह सूचना दर्ज होती है कि दुनिया भर में इस खास पुस्तक की कई लाख प्रतियां बिक चुकी हैं और यूरोप व अमेरिका के अखबारों ने इसकी प्रशंसा में ये शब्द कहे हैं। कवर पर दी गई ऐसी सूचनाएं किताब के प्रति पाठकों में उत्सूकता जगाती हैं और किताब की बिक्री का सकारात्मक माहौल तैयार करती हैं।
इधर मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित कई बेस्टसेलर पढ़े। इनमें से ज्यादातर सेल्फ-हेल्प पुस्तकें थीं, जिन्हें भोपाल के मंजूल पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया है। पहली बार साल २००३ में मैंने नेपोलियन हिल की ‘थिंक एंड ग्रो रिच’ (हिंदी अनुवाद: सोचिए और अमीर बनिए) पढ़ी और तभी से मुझे ऐसी किताबों का चस्का लग गया। कुछ वैचारिक असहमतियों के बावजूद इनमें से ज्यादातर किताबों ने आइडिया, सहज भाषा-शैली और पाठकों को मुरीद बनाने के अपने कौशल की वजह से मुझे बार-बार अपनी ओर आकर्र्षित किया। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में अपने विलक्षण योगदान के लिए जाने जानेवाले अरविंद कुमार ने भी कुछ साल पहले अपना प्रकाशन शुरू किया है-‘अरविंद कुमार पब्लिशर्स।’ इस प्रकाशन के जरिए वे नए-नए विषयों की बेहद सुंदर, उपयोगी और पठनीय पुस्तकें किफायती दाम पर पाठकों को उपलब्ध करा रहे हैं। मगर अफसोस कि मंजूल, अरविंद कुमार पब्लिशर्स और ऐसे ऊंगलियों पर गिने जा सकने वाले चंद प्रकाशक पेशेगत विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए हिंदी में लीक से हटकर जो किताबें छाप रहे हैं, वह सब अंग्रेजी भाषा की बेस्टसेलर हैं। हिंदी में आकर्षक साज-सज्जा के साथ प्रकाशित इन किताबों के आवरण पर खासतौर से यह सूचना दर्ज होती है कि दुनिया भर में इस खास पुस्तक की कई लाख प्रतियां बिक चुकी हैं और यूरोप व अमेरिका के अखबारों ने इसकी प्रशंसा में ये शब्द कहे हैं। कवर पर दी गई ऐसी सूचनाएं किताब के प्रति पाठकों में उत्सूकता जगाती हैं और किताब की बिक्री का सकारात्मक माहौल तैयार करती हैं। राज्यसभा में केवल ‘समाजवादी पार्टी’ (सपा) व ‘राष्ट्रीय जनता दल’ (आर.जे.डी) के कुछ सदस्यों की शर्मनाक व गैर-संसदीय गतिविधियों यथा राज्यसभा अध्यक्ष व देश के उप-राष्ट्रपति डॉ. हामिद अंसारी की सीट तक लपकने तथा उन से बिल छीन कर फाड़ देने के कारण यह बिल ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ पर पारित न हो सका. यदि उस दिन हो जाता तो यह ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ पर देश की महिलाओं के लिए एक उपहार होता. उप-राष्ट्रपति के पास बार बार सदन को स्थगित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प था ही नहीं. यह बिल जो कि देश के चौथे प्रधानमंत्री राजीव गाँधी का स्वप्न था, संसद में सन् 1996 में ही जा कर प्रस्तुत किया जा सका, जब एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे. उस समय भी यह विषय क्यों कि जीवंत था, जनता खुशखबरी सुनने के लिए दूरदर्शन से चिपकी रही, लेकिन सपा नेता मुलायम सिंह यादव व कुछ अन्य नेताओं के आकस्मिक हस्तक्षेप के कारण सपना चूर सा हो गया था. ‘अन्य पिछड़े वर्ग’ यानी OBC पल्टन को ‘आरक्षण के भीतर आरक्षण’ चाहिए था तथा बिल को रोकना पड़ा और यह बिल उस के बाद 14-15 वर्ष तक दिन का प्रकाश नहीं देख सका. सन् ’96 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली ‘राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबन्ध’ (NDA) सरकार द्वारा कुल पांच बार - सन् 98, 99,2002 व 2003 (दो बार) में - प्रस्तुत किया गया पर बार बार इसे पटरी से उतारा गया और तब तक यह एक टेढ़ी खीर सा लगने लगा. डॉ. मनमोहन सिंह की ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन’ (UPA) सरकार सन् 2004 में सत्ता में आई तो उस ने इसे ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ (Common Minimum Programme) का हिस्सा बनाया और सन् 2008 में संसद में प्रस्तुत किया. OBC नेताओं ने हमेशा आरक्षण को ले कर अधिकाधिक टुच्चे किस्म के राजनीतिक खेल खेले. पहले सन् ’90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह व चौधरी देवीलाल ने एक दूसरे को धूल चटवानी चाही. उप-प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने दिल्ली के ‘बोट क्लब’ की अपनी आगामी जन्म-दिवस रैली में ‘मंडल आयोग’ की सफरिशें लागू करने की मांग रख कर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सांसत में डाल देने की योजना बनाई. पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी चित्त कर देने का कच्ची गोलियाँ नहीं खाई थी. इस से पहले कि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन आए, उस ने ‘मंडल आरक्षण’ की सफरिशें लागू करने का निर्णय ले कर देवीलाल को चारों खाने चित्त सा कर दिया. न अन्य राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा और न कोई ज़रूरी बहस! . देश अचानक हक्का-बक्का सा हो कर नौजवानों के आत्म-दाह व विश्वनाथ प्रताप सिंह के पुतले जलाए जाने की खबरें सुनने लगा. एक नवयुवक राजीव गोस्वामी, (जो अब मर चुके हैं) जो आत्म-दाह के बाद बुरी तरह जली हुई स्थिति में सफ़दरजंग हस्पताल में दाखिल थे, को देखने जब मदनलाल खुराना व लालकृष्ण अडवानी गए तो ज्यों ही वे हस्पताल से बाहर आए, कई बौखलाए हुए नौजवान उन दोनों पर झपटे और दौड़ कर मदनलाल खुराना की तो कमीज़ ही फाड़ दी. अडवानी चुस्ती से खिसक कर कार में घुस गए. देश के कई पिछड़े वर्गों को आरक्षण का इंतज़ार था पर यहाँ बेहद घटिया स्तर की राजनीति शुरू हो चुकी थी. आखिर सरकारी नौकरियों में ‘मंडल आरक्षण’ नरसिम्हा राव के कार्यकाल (’91 -’96) में एक अदालती फैसले के बाद ही लागू हो सके. परन्तु उस के बाद भी लालू प्रसाद जैसे निकृष्ट नेताओं का टुच्चापन चलता रहां जो या तो Creamy Layer’ पर या अन्य मसलों पर चद्दर को अपनी ओर खींचते रहे. परन्तु आश्चर्य कि जब लालू प्रसाद सन् 2004 में डॉ. मनमोहन सिंह की UPA सरकार में रेलमंत्री बने व उन के ही OBC समर्थक राजनीतिक शत्रु नितीश कुमार ने सन् 2005 में बिहार के मुख्यामंत्री पद की शपथ ली तब उन्होंने OBC के सवाल पर केवल हल्की मौखिक बयानबाजी करते रहना काफी समझा. लालू प्रसाद को तो देसी घी की स्वादिष्ट कचौड़ियाँ तभी से पसंद थी जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे सो अब केंद्रीय सत्ता की उस से भी बड़ी व स्वादिष्ट कचौड़ी मुंह में रखे रहना उन्हें अच्छा लगता होगा. नतीजतन सन् 2006 में जब संसद ने OBC को शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण देने का विधेयक पारित किया, तब इन दोनों नेताओं ने अधिक कुछ कहा ही नहीं, जबकि उच्च-जातियों के विद्यार्थी विरोध के गुस्से में देश को सिर पर उठाए थे. मीडिया उन्हें पूरी ‘कवरेज’ दे रहा था पर OBC की तरफ से कोई आवाज़ थी ही नहीं. इन प्रदर्शनों के लिए भा.जा.पा व कांग्रेस पर अंगुलियां उठ रही थी कि OBC को खुश करने के बाद वे अपनी गिरगिटिया शैली में उच्च-जातीय वोट बचाने के लिए इन प्रदर्शनों को भीतर ही भीतर से हवा दे रहे हैं. ‘महिला आरक्षण बिल’ पर भी लालू व मुलायम जैसे नेताओं की नज़र बिहार व उत्तर प्रदेश में क्रमशः 2010 व 2012 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर रही. सौभाग्य से तीन पार्टियां जिन का हमेशा आपस में झगड़ते रहने का ही रिकॉर्ड रहा, यानी भा.ज.पा कांग्रेस व वाम-मोर्चा, एकजुट हो कर ‘महिला आरक्षण बिल’ के समर्थन में आ खड़ी हुई थी**. दूरदर्शन चैनलों पर तीन महिलाओं - सोनिया गाँधी, सुषमा स्वराज व बृंदा करात को बार बार देखा गया जो इस बिल को पारित कराने के लिए अधिकाधिक उत्तेजित लग रही थी. इन के साथ जयंती नटराजन व नजमा हेप्तुल्ला जैसी उत्साही महिलाएं भी थी. मीडिया ने खुश हो कर सोनिया-सुषमा- बृंदा की तिकड़ी में से सोनिया को ‘बिल की ड्राईवर’ की उपाधि दे दी.
राज्यसभा में केवल ‘समाजवादी पार्टी’ (सपा) व ‘राष्ट्रीय जनता दल’ (आर.जे.डी) के कुछ सदस्यों की शर्मनाक व गैर-संसदीय गतिविधियों यथा राज्यसभा अध्यक्ष व देश के उप-राष्ट्रपति डॉ. हामिद अंसारी की सीट तक लपकने तथा उन से बिल छीन कर फाड़ देने के कारण यह बिल ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ पर पारित न हो सका. यदि उस दिन हो जाता तो यह ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ पर देश की महिलाओं के लिए एक उपहार होता. उप-राष्ट्रपति के पास बार बार सदन को स्थगित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प था ही नहीं. यह बिल जो कि देश के चौथे प्रधानमंत्री राजीव गाँधी का स्वप्न था, संसद में सन् 1996 में ही जा कर प्रस्तुत किया जा सका, जब एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे. उस समय भी यह विषय क्यों कि जीवंत था, जनता खुशखबरी सुनने के लिए दूरदर्शन से चिपकी रही, लेकिन सपा नेता मुलायम सिंह यादव व कुछ अन्य नेताओं के आकस्मिक हस्तक्षेप के कारण सपना चूर सा हो गया था. ‘अन्य पिछड़े वर्ग’ यानी OBC पल्टन को ‘आरक्षण के भीतर आरक्षण’ चाहिए था तथा बिल को रोकना पड़ा और यह बिल उस के बाद 14-15 वर्ष तक दिन का प्रकाश नहीं देख सका. सन् ’96 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली ‘राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबन्ध’ (NDA) सरकार द्वारा कुल पांच बार - सन् 98, 99,2002 व 2003 (दो बार) में - प्रस्तुत किया गया पर बार बार इसे पटरी से उतारा गया और तब तक यह एक टेढ़ी खीर सा लगने लगा. डॉ. मनमोहन सिंह की ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन’ (UPA) सरकार सन् 2004 में सत्ता में आई तो उस ने इसे ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ (Common Minimum Programme) का हिस्सा बनाया और सन् 2008 में संसद में प्रस्तुत किया. OBC नेताओं ने हमेशा आरक्षण को ले कर अधिकाधिक टुच्चे किस्म के राजनीतिक खेल खेले. पहले सन् ’90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह व चौधरी देवीलाल ने एक दूसरे को धूल चटवानी चाही. उप-प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने दिल्ली के ‘बोट क्लब’ की अपनी आगामी जन्म-दिवस रैली में ‘मंडल आयोग’ की सफरिशें लागू करने की मांग रख कर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सांसत में डाल देने की योजना बनाई. पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी चित्त कर देने का कच्ची गोलियाँ नहीं खाई थी. इस से पहले कि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन आए, उस ने ‘मंडल आरक्षण’ की सफरिशें लागू करने का निर्णय ले कर देवीलाल को चारों खाने चित्त सा कर दिया. न अन्य राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा और न कोई ज़रूरी बहस! . देश अचानक हक्का-बक्का सा हो कर नौजवानों के आत्म-दाह व विश्वनाथ प्रताप सिंह के पुतले जलाए जाने की खबरें सुनने लगा. एक नवयुवक राजीव गोस्वामी, (जो अब मर चुके हैं) जो आत्म-दाह के बाद बुरी तरह जली हुई स्थिति में सफ़दरजंग हस्पताल में दाखिल थे, को देखने जब मदनलाल खुराना व लालकृष्ण अडवानी गए तो ज्यों ही वे हस्पताल से बाहर आए, कई बौखलाए हुए नौजवान उन दोनों पर झपटे और दौड़ कर मदनलाल खुराना की तो कमीज़ ही फाड़ दी. अडवानी चुस्ती से खिसक कर कार में घुस गए. देश के कई पिछड़े वर्गों को आरक्षण का इंतज़ार था पर यहाँ बेहद घटिया स्तर की राजनीति शुरू हो चुकी थी. आखिर सरकारी नौकरियों में ‘मंडल आरक्षण’ नरसिम्हा राव के कार्यकाल (’91 -’96) में एक अदालती फैसले के बाद ही लागू हो सके. परन्तु उस के बाद भी लालू प्रसाद जैसे निकृष्ट नेताओं का टुच्चापन चलता रहां जो या तो Creamy Layer’ पर या अन्य मसलों पर चद्दर को अपनी ओर खींचते रहे. परन्तु आश्चर्य कि जब लालू प्रसाद सन् 2004 में डॉ. मनमोहन सिंह की UPA सरकार में रेलमंत्री बने व उन के ही OBC समर्थक राजनीतिक शत्रु नितीश कुमार ने सन् 2005 में बिहार के मुख्यामंत्री पद की शपथ ली तब उन्होंने OBC के सवाल पर केवल हल्की मौखिक बयानबाजी करते रहना काफी समझा. लालू प्रसाद को तो देसी घी की स्वादिष्ट कचौड़ियाँ तभी से पसंद थी जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे सो अब केंद्रीय सत्ता की उस से भी बड़ी व स्वादिष्ट कचौड़ी मुंह में रखे रहना उन्हें अच्छा लगता होगा. नतीजतन सन् 2006 में जब संसद ने OBC को शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण देने का विधेयक पारित किया, तब इन दोनों नेताओं ने अधिक कुछ कहा ही नहीं, जबकि उच्च-जातियों के विद्यार्थी विरोध के गुस्से में देश को सिर पर उठाए थे. मीडिया उन्हें पूरी ‘कवरेज’ दे रहा था पर OBC की तरफ से कोई आवाज़ थी ही नहीं. इन प्रदर्शनों के लिए भा.जा.पा व कांग्रेस पर अंगुलियां उठ रही थी कि OBC को खुश करने के बाद वे अपनी गिरगिटिया शैली में उच्च-जातीय वोट बचाने के लिए इन प्रदर्शनों को भीतर ही भीतर से हवा दे रहे हैं. ‘महिला आरक्षण बिल’ पर भी लालू व मुलायम जैसे नेताओं की नज़र बिहार व उत्तर प्रदेश में क्रमशः 2010 व 2012 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर रही. सौभाग्य से तीन पार्टियां जिन का हमेशा आपस में झगड़ते रहने का ही रिकॉर्ड रहा, यानी भा.ज.पा कांग्रेस व वाम-मोर्चा, एकजुट हो कर ‘महिला आरक्षण बिल’ के समर्थन में आ खड़ी हुई थी**. दूरदर्शन चैनलों पर तीन महिलाओं - सोनिया गाँधी, सुषमा स्वराज व बृंदा करात को बार बार देखा गया जो इस बिल को पारित कराने के लिए अधिकाधिक उत्तेजित लग रही थी. इन के साथ जयंती नटराजन व नजमा हेप्तुल्ला जैसी उत्साही महिलाएं भी थी. मीडिया ने खुश हो कर सोनिया-सुषमा- बृंदा की तिकड़ी में से सोनिया को ‘बिल की ड्राईवर’ की उपाधि दे दी. मार्कण्डेय
मार्कण्डेय