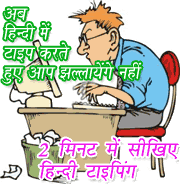दरभंगा से चल कर मुजफ्फरपुर, बनारस, इलाहाबाद और अलीगढ़ होते हुए नई दिल्ली जानेवाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में एस 3 डिब्बे (कोच नंबर 90309) का बर्थ नंबर 12 (टिकट नंबर 97361975) मेरे लिए आरक्षित था। इस रेलगाड़ी में मैं मुजफ्फरपुर से चढ़ा था। मुजफ्फरपुर में विख्यात समाजवादी चिंतक तथा श्रमिक नेता सच्चिदानंद सिन्हा के अस्सी वर्ष का हो जाने पर एक दिन का घरेलू आयोजन था। आयोजन में सिर्फ सच्चिदानंद सिन्हा की जीवन यात्रा, रचनावली और वैचारिक दृष्टि की ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि आधुनिक सभ्यता के संकट के विभिन्न पहलुओं पर सुनने लायक व्याख्यान भी हुए। बाहर से आनेवाले लोगों के स्वागत तथा आवभगत का बहुत उत्तम प्रबंध मनोरमा सिन्हा और प्रभाकर सिन्हा ने किया था। हम सभी अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में अपने-अपने घर लौट रहे थे। मानो किसी तपोवन से लौट रहे हों। इस समय देश में सैकड़ों विद्वान और चिंतक हैं। लेकिन उनमें से कौन ऐसे तपोवन में रहता है, जिसका मासिक खर्च मुश्किल से हजार रुपए होगा?
वापसी की इस कृतज्ञ और प्रसन्न यात्रा के स्वाद को खट्टा कर दिया एक ऐसे टीटी ने, जिसे कायदे से जेल में होना चाहिए था। उससे मेरी मुठभेड़ हुई 29-30 मार्च की रात बारह बज कर पंद्रह मिनट पर। गाजीपुर और बनारस के बीच। इस युवा टीटी के दर्शन होने के पहले मेरी यात्रा बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। कई यात्रियों का सहयोग भाव देख कर मैं चकित हो गया। उनके मधुर व्यवहार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि अभी भी भारत के सबसे भले लोग गांवों में रहते हैं। कुछ सहयोग मैंने भी किया था। मेरा बर्थ सबसे नीचे था। वह मैंने एक सज्जन को दे दिया, जो शायद किडनी के मरीज थे। उनके नाम आठ नंबर का बर्थ था। उस पर जा कर मैं लेट गया। एक टीटी लगभग आठ बजे उस डिब्बे के टिकटों की जांच करके जा चुका था।
आधी रात को इस दूसरे टीटी ने हमारे डिब्बे में प्रवेश किया। सबसे पहले उसने एक व्यक्ति से 300 रुपए गैरकानूनी ढंग से वसूल किए। कुछ और लोगों का शोषण किया। फिर वह सात नंबर बर्थ किसके नाम पर है, यह खोजने लगा। वह बर्थ मेरे बर्थ के नीचे था। उस पर एक युवा दंपति लेटा हुआ था। उसका टिकट देख कर टीटी ने उनके अपने बर्थ पर भेज दिया। इससे सात नंबर बर्थ खाली हो गया। इस बर्थ को उसने एक व्यक्ति को बेच दिया। कितने में, यह मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों की बातचीत मैं सुन नहीं पाया था।
अब वह मेरे पास आया। उसने मेरा टिकट देखने की मांग की। अगर वह पूरे डिब्बे के यात्रियों के टिकट चेक कर रहा होता, तो अपना टिकट दिखाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। पर मैं लक्ष्य कर चुका था कि वह उन्हीं बर्थों के पास जा कर टिकट देख रहा था, जहां से उसे कुछ नकद मिलने की उम्मीद की। इस कारण से उस पर मेरे मन में कुछ गुस्सा भी था। उसके साथ मेरा जो संवाद हुआ, उसका एक हिस्सा इस प्रकार है :
वह -- टिकट दिखाइए।
मैं - अपना टिकट दिखाने के पहले मैं आपका आई कार्ड देखना चाहूंगा।
वह - मेरा कोट नहीं दिखाई नहीं दे रहा है?
मैं - ऐसे कोट बाजार में बहुत मिल जाएंगे।
वह - यह चार्ट भी आप नहीं देख पा रहे हैं?
मैं -- यह तो कंप्यूटर का खेल है। आप मेरे घर चलें, मैं ऐसे कई चार्ट बना कर उनका प्रिंट आपको दे दूंगा।
वह -- बकवास छोड़िए। आप अपना टिकट दिखाइए।
मैं -- मैं अपना टिकट तभी दिखाऊंगा जब आप अपना आई कार्ड दिखा देंगे। मुझे यह यकीन कैसे हो कि आप ही टीटी हैं? वह -- सरकार हमें आई कार्ड नहीं देती।
मैं -- ऐसा नहीं हो सकता। सरकार अपने हर सार्वजनिक अधिकारी को आई कार्ड जारी करती है।
वह - टिकट देखना मेरा काम है। आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं।
मैं -- जी नहीं, आपका काम बर्थ बेचना, रिश्वत लेना और यात्रियों का शोषण करना है। यह मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं।
वह -- तो ठीक है, जो उखा..ते बने, उखा..ड़ लेना। पहले हिन्दुस्तान को सुधार लो, फिर मुझसे बात करना।
मैं -- सर, आप भी इसी हिन्दुस्तान के पार्ट हैं। मान लीजिए, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं।
बातचीत जारी रही।
वह -- बाबूजी, आप टिकट दिखाइए।
मैं -- सर, मैं आपको टिकट नहीं दिखाऊंगा।
वह - आप बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं सीधे से कह रहा हूं कि आप अपना टिकट दिखाइए।
मैं -- मैं बच्चा होता, तब भी यही करता।
वह -- आप टिकट दिखाइए।
मैं -- मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। आपने अभी-अभी सात नंबर बर्थ बेचा है।
वह - यह मेरा बर्थ है। इसे मैं बेच सकता हूं।
मैं -- जी नहीं, आप नहीं बेच सकते। आप इसे अलॉट कर सकते हैं। लेकिन रसीद काटने के बाद। आपने अलॉट नहीं किया है, बेचा है।
वह -- तो आपकी क्यों ..ट रही है? आप अपना टिकट दिखाइए।
मैं -- यह टिकट देखने का समय नहीं है। सवा बारह बज रहे हैं। आप मेरी नींद में खलल डाल रहे हैं।
वह -- आप दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगे।
मैं -- मुझे इसकी परवाह नहीं है। आपका आई कार्ड देखे बिना मैं आपको टिकट नहीं दिखा सकता।
वह -- मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। आप टिकट दिखा दीजिए।
मैं -- आप मुझे खिड़की से फेंक देंगे. तब भी मैं आपको टिकट नहीं दिखाऊंगा। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। क्या पता आप मेरा टिकट फाड़ कर फेंक दें और बाद में मुझे बेटिकट साबित कर मुझे अगले स्टेशन पर उतार दें। फिर मेरा बर्थ किसी और को बेच दें।
अब उसे यकीन हो गया कि वह मुझे सिर्फ धमकी दे कर बाध्य नहीं कर सकता। उसने एक फोन निकाला और किसी से अनुरोध किया -- एक आदमी सरकारी काम में दखल दे रहा है। दो पुलिसवाले तुरंत भेजिए। मैंने कहा -- हां, मैं पुलिस को टिकट दिखा सकता हूं। कुछेक मिनट बाद दो पुलिसवाले प्रगट हुए। टीटी ने उन्हें मेरा केस बताया। मैंने कहा -- ये सज्जन अपना आई कार्ड नहीं दिखा रहे हैं। जब तक इनका परिचय इस्टैब्लिश नहीं हो जाता, मैं इन्हें किस आधार पर टिकट दिखाऊं? एक पुलिसवाले ने मुलायम आवाज में कहा -- आप कैसी बात कर रहे हैं? टीटी ही हैं। मैं -- तो आप पहले इनकी तलाशी लीजिए। इन्होंने मेरे सामने कई आदमियों से रिश्वत ली है। पुलिसवाला -- क्यों बात बढ़ा रहे हैं? आप टिकट दिखा दीजिए, सारा मामला खतम हो जाएगा। मैंने उसकी ओर टिकट बढ़ा दिया। उसने टिकट हाथ में ले कर जोर से पढ़ा -- एस तीन, बर्थ नंबर बारह। चलिए, आप अपने बर्थ पर चलिए। मैंने अपना सामान उतारा और अपने बर्थ की ओर जाने लगा। पुलिसवाला मेरे पीछे-पीछे। बारह नंबर पर वही मरीज था। उसने बताया -- मैं पेशेट हूं। पुलिसवाले ने उस पर दया की। मुझे अपना पहलेवाला बर्थ मिल गया। टीटी और पुलिसवाले चले गए। उनके जाते ही, एक मुसाफिर ने सात नंबर सीट पर लगी हुई एक पट्टी दिखाई, जिस पर लिखा हुआ था -- विकलांग के लिए सुरक्षित।
कुछ देर बाद बनारस स्टेशन आ गया। मैंने सोचा, ट्रेन में जगह-जगह अंकित सुझावों के अनुसार गार्ड के पास जा कर शिकायत लिखवाऊं। पर उसका डिब्बा बहुत दूर था। वहां तक जाना संभव नहीं था। स्टेशन मास्टर के पास जाता, तब तक रेल छूट जाती। इलाहाबाद आया, तब भी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दिया, जिससे मैं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकूं। उधर टीटी से विवाद के दौरान दस-पंद्रह आदमी जमा हो गए थे, पर कोई कुछ नहीं बोला। अगले दिन सबेरे, वही व्यक्ति जिसने विकलांग वाला बर्थ दिखाया था, मुझे शाबाशी देने लगा। उसका नाम-पता और टिकट नंबर ( 42517369) मैंने नोट कर लिया। मैंने सोचा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच कर अपनी शिकायत दर्ज करवा दूंगा। स्टेशन आने पर मैं अजमेरी गेट साइड की ओर चला। सीढ़ी पर रेलवे का इश्तहार देखा, जिसमें 'शिकायत' के सामने दोनों ओर तीर का निशान था। नीचे आने पर लगभग पंद्रह मिनट तक वह जगह खोजता रहा, जहां शिकायत दर्ज कराई जा सके। सफलता नहीं मिली।
घर की ओर जाते हुए मैं यही सोच रहा था कि रेल मंत्रालय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए लालू प्रसाद को बहुत बधाई मिली है, पर लगता है कि वे रेल के आंतरिक भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाए हैं। नहीं तो वह सब कैसे हो पाता जो मेरे डिब्बे में हुआ? वह और उस जैसे सैकड़ों टीटी आज जेल में होते।
फिर याद आया -- हमारे डिब्बे के दोनों शौचालयों में न पानी था, न बिजली थी। मन में यह सवाल उठा -- अगर मैं उस टीटी को पानी और बिजली की कमी दूर कराने के लिए अनुरोध करता, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया क्या होती? डिब्बे के शौचालयों में पानी और रोशनी हो तथा टीटी बेईमान और बदतमीज न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए मैं या मेरे सहयात्री क्या कर सकते थे? शायद रेल मंत्री अपने चुनाव भाषणों में इस पर प्रकाश डालें।
राजकिशोर
skip to main |
skip to sidebar

अभी हाल ही में उड़ीसा के नंदन कानन अभयारण्य में गया। यह एक चिड़ियाघर भी है। यहाँ जैसे ही हम लोग अंदर घुसने को हुए तो हमारी तलाशी ली गई और हमसे पूछा गया कि प्लास्टिक की कोई बोतल, पॉलीथीन की थैली आदि तो नहीं है? और फिर अंदर पहुँचते ही जगह जगह मुझे यह बोर्ड दिखाई दिया। यह सब देखते ही यकायक दिल्ली का ख्याल आ गया। अभी कुछ सप्ताह पहले ही तो दिल्ली से पॉलीथीन की थैलियाँ गायब करने की घोषणा की थी राज्य सरकार ने। पर हुआ क्या अभी तक? कुछ दिनों तक दुकानों पर एक पोस्टर चिपका हुआ दिखाई दिया-"असुविधा के लिये खेद है"। कुछ दिनों तक पॉलीथीन की थैलियाँ नहीं मिली। लेकिन जो थैलियाँ दुकानदार खरीद चुके थे, वो तो इस्तेमाल होनी ही थी। और फिर सब्जी वाले क्या इस्तेमाल करेंगे? जो ग्राहक घर से कोई थैली लाना भूल गये वो कैसे सामान लेंगे? इन सभी सवालों के चलते पॉलीथीन की थैलियाँ भी चलती रहीं और आज भी बेधड़क चल रही हैं।
अब तो असुविधा वाला कागज़ भी फट चुका है। थैलियाँ अभी भी प्रयोग में हैं।
आखिर इन थैलियों से नुकसान क्या है? हममें से अधिकतर सभी जानते हैं। बात है केवल जागरूकता फैलाने की। लोगों को समझाने की। आइये एक बार फिर जानें कि क्या कुछ कर सकती हैं ये थैलियाँ-
१)धरती को खोखला कर रही हैं ये थैलियाँ: ये थैलियाँ हमारे घरों, ऑफिसों, सब्जी की रेहड़ियों, दुकानों से होती हुई पार्कों, सड़क के किनारे की पगडंडियों और कूड़े के ढेरों में पहुँच जाती हैं। और गंदा कर देती हैं मिट्टी को, दिक्कत देती हैं पेड़-पौधों की सिंचाई में। यही थैलियाँ नालियों से होती हुई नदियों में जा पहुँचाती हैं। इनके जलने से जहरीली गैस भी निकलती है।
२)क्या आप जानते हैं इन थैलियों से हर साल लाखों जानवर मारे जाते हैं। इनमें डालफिन, मछलियाँ व अन्य जलचर शामिल हैं। इन्हीं थैलियों में खाने को डालते हैं और यही सब खाकर गाय-भैंस बीमार पड़ती हैं। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि उस जानवर के मारे जाने के बाद भी वो प्लास्टिक उसके शरीर में ज्यों का त्यों रहता है और जो भी अन्य पशु उस मृत पशु को खाता है उसके शरीर में भी प्लास्टिक प्रवेश कर जायेगा।
३)प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म होने में हज़ार वर्ष लग जाते हैं। यानि पर्यावरण में हजार साल तक प्लास्टिक रहेगा।
४)एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि प्लास्टिक पैट्रोलियम पदार्थों से बनता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम के इस्तेमाल से ही पॉलीथीन बनाया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ पहले से ही हमारे जीवन की जरुरत बन चुके हैं। वाहन का ईंधन, घर में रसोई गैस, फैक्ट्री, बिजली घर इत्यादि यानि कि हर पल पेट्रोलियम की जरुरत हमें रहती है। अब यदि पॉलीथीन को इस तरह हम बर्बाद करेंगे तो इसका आशय यह है कि हम अधिकाधिक पेट्रोल को बर्बाद कर रहे हैं।
आखिर हम कर क्या सकते हैं?
प्लास्टिक के बैग की जगह कपड़े व जूट आदि के बने हुए बैग का प्रयोग करें। दूसरा आसान तरीका यह है कि एक ही थैली को बार-बार प्रयोग में लायें। इससे पॉलीथीन का उत्पादन और बर्बादी दोनों कम होगी।
सरकार तो कानून बनाती रहेगी लेकिन पर्यावरण को बचाने और उसकी देखभाल का जिम्मा तो हमारे ऊपर भी है। इस तरह के छोटे-छोटे कदम से हम प्रकृति को खत्म होने से बचा सकते हैं। कहते हैं कि जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है। यदि हम प्रकृति को नुकसान पहुँचायेंगे तो अंत हमारा भी होगा। पर्यावरण को दूषित होने से बचायें। आइये यह संकल्प लें।
तपन शर्मा
 सरकार महंगाई दर कम होने पर अपनी पीठ ठोक रही है कि 14 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान यह घट कर 0.27 प्रतिशत पर आ गई है। यह महंगाई की दर में वृद्वि का पिछले 30 वर्षों का सबसे नीचा स्तर है। सरकार के लिए संतोष की बात है भी क्योंकि गत वर्ष इसी अवधि में यह 8.02 प्रतिशत थी। यही नहीं गत वर्ष अगस्त में यह दर 13 प्रतिशत का आकंड़ा छू गई थी। उस समय पूरा मीडिया महंगाई को लेकर सरकार के पीछे पड़ गया था। इसे देखते हुए सरकार के लिए यह राहत की बात है। यही नहीं आगामी आम चुनाव को देखते हुए भी सरकार प्रसन्न है कि चलो महंगाई की दर पर काबू तो पाया।
सरकार महंगाई दर कम होने पर अपनी पीठ ठोक रही है कि 14 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान यह घट कर 0.27 प्रतिशत पर आ गई है। यह महंगाई की दर में वृद्वि का पिछले 30 वर्षों का सबसे नीचा स्तर है। सरकार के लिए संतोष की बात है भी क्योंकि गत वर्ष इसी अवधि में यह 8.02 प्रतिशत थी। यही नहीं गत वर्ष अगस्त में यह दर 13 प्रतिशत का आकंड़ा छू गई थी। उस समय पूरा मीडिया महंगाई को लेकर सरकार के पीछे पड़ गया था। इसे देखते हुए सरकार के लिए यह राहत की बात है। यही नहीं आगामी आम चुनाव को देखते हुए भी सरकार प्रसन्न है कि चलो महंगाई की दर पर काबू तो पाया।
महंगाई की गिरती दर को देखते हुए अनेक अर्थशास्त्री देश में मुद्रा स्फीति की बजाए अपस्फीति की आशंका जताने लगे हैं।
विरोधाभास
वास्तव में सरकार के बयानों में ही विरोधाभास है। थोक मूल्य सूचकांक उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि देश में महंगाई की दर कम हो रही है और आगामी सप्ताहों में यह शून्य पर आ जाएगी या निगेटिव हो जाएगी।
लेकिन वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार स्वयं यह मान रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई है। उनका कहना है कि महंगाई की दर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निकाली जाती है। यह ठीक है कि थोक मूल्य सूचकांक में लगातार कमी आ रही है लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्वि दर तो अब भी 10 प्रतिशत के आसपास घूम रही है।
उपभोक्ता हैरान
बरहहाल, इन सब से आम उपभोक्ता हतप्रभ है। वह महंगाई की दर 13 प्रतिशत के आसपास पहुंचने के बाद परेशान तो था लेकिन अब गिर कर 0.27 प्रतिशत आ जाने पर प्रसन्न नहीं लेकिन हैरान अवश्य है कि यह क्या हो रहा है? उसका बजट तो वहीं का वहीं है या बढ़ रहा है, फिर महंगाई कैसे कम हो रही है।
क्या है सूचकांक
थोक मूल्य सूचकांक में लगभग एक हजार विभिन्न वस्तुओं का समावेश है। दिलचस्प बात यह है कि सूचकांक की लगभग 78 प्रतिशत वस्तुएं वे हैं जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी को आवश्यकता ही नहीं होती है। इनमें विभिन्न रसायन, धातुएं, विभिन्न प्रकार के ईंधन, ग्रीस, रंग-रोगन, सीमेंट, स्टील, मशीनरी व मशीन टूल, पुस्तकों व समाचार पत्रों की प्रिन्टिग, पल्प, कागज आदि अनेक वस्तुएं इस सूची में शामिल हैं। शेष 22 प्रतिशत में वे वस्तुएं हैं जिनकी रोज आवश्यकता होती है।
आंकड़ों की सच्चाई
आम उपभोग की अनेक वस्तुओं के भाव दिल्ली बाजार में गत वर्ष की तुलना में ऊंचे चल रहे हैं। गत वर्ष दिल्ली बाजार में चीनी के एक्स मिल भाव 1600 रुपए के आसपास चल रहे थे जो अब लगभग 2200 रुपए (थोक में 25 रुपए किलो) चल रहे हैं। गुड़ के भाव तो इससे भी आगे हैं। गेहूं दड़ा क्वालिटी के थोक भाव 1125/1130 रुपए से बढ़ कर 1160/1165 रुपए हो गए हैं। मूंग के भाव गत वर्ष 2200/2650 रुपए थे जो अब 3500/4000 रुपए हो गए हैं। रंगून की अरहर गत वर्ष 2575/2600 रुपए थी जो अब 3500 रुपए पार कर गई है। रंगून की उड़द भी 2375/2400 रुपए से बढ़ कर 2800 रुपए के आसपास हो गई है। चने के भाव गत वर्ष की तुलना में अवश्य कम हैं। मसालों के भाव भी गत वर्ष की तुलना में काफी तेज हैं लेकिन खाद्य तेलों के भाव नीचे चल रहे हैं।
सरकारी आंकड़े
यदि सरकारी आंकड़ों को देखें तो भी यह स्पष्ट है कि खाद्य वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक बढ़ा है। इस वर्ष 14 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान दलहनों का थोक मूल्य सूचकांक 269.1 था जो गत वर्ष 15 मार्च को 244.7 था। अनाजों का सूचकांक आलोच्य अवधि में 219.4 से बढ़ कर 241.6 पर पहुंच गया है। सब्जियों व फलों का सूचकांक 234.8 से बढ़ कर 247.6 हो गया है। दूध का सूचकांक 220.3 से बढ़ कर 233.7 हो गया है। इसी प्रकार मसालों, खांडसार, गुड़ व चीनी तथा अन्य खाद्य उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक बढ़ा है लेकिन अन्य व गैर खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में कमी के कारण महंगाई की दर में बढ़ोतरी कम हो गई है।
यहां यह जानना भी आवश्यक है कि महंगाई की दर में बढ़ोतरी की गति कम हुई लेकिन वह घट नहीं रही है।
--राजेश शर्मा
Thursday, April 02, 2009
Wednesday, April 01, 2009
आइए पॉलीथीन के खिलाफ संकल्प लें....

अभी हाल ही में उड़ीसा के नंदन कानन अभयारण्य में गया। यह एक चिड़ियाघर भी है। यहाँ जैसे ही हम लोग अंदर घुसने को हुए तो हमारी तलाशी ली गई और हमसे पूछा गया कि प्लास्टिक की कोई बोतल, पॉलीथीन की थैली आदि तो नहीं है? और फिर अंदर पहुँचते ही जगह जगह मुझे यह बोर्ड दिखाई दिया। यह सब देखते ही यकायक दिल्ली का ख्याल आ गया। अभी कुछ सप्ताह पहले ही तो दिल्ली से पॉलीथीन की थैलियाँ गायब करने की घोषणा की थी राज्य सरकार ने। पर हुआ क्या अभी तक? कुछ दिनों तक दुकानों पर एक पोस्टर चिपका हुआ दिखाई दिया-"असुविधा के लिये खेद है"। कुछ दिनों तक पॉलीथीन की थैलियाँ नहीं मिली। लेकिन जो थैलियाँ दुकानदार खरीद चुके थे, वो तो इस्तेमाल होनी ही थी। और फिर सब्जी वाले क्या इस्तेमाल करेंगे? जो ग्राहक घर से कोई थैली लाना भूल गये वो कैसे सामान लेंगे? इन सभी सवालों के चलते पॉलीथीन की थैलियाँ भी चलती रहीं और आज भी बेधड़क चल रही हैं।
अब तो असुविधा वाला कागज़ भी फट चुका है। थैलियाँ अभी भी प्रयोग में हैं।
आखिर इन थैलियों से नुकसान क्या है? हममें से अधिकतर सभी जानते हैं। बात है केवल जागरूकता फैलाने की। लोगों को समझाने की। आइये एक बार फिर जानें कि क्या कुछ कर सकती हैं ये थैलियाँ-
१)धरती को खोखला कर रही हैं ये थैलियाँ: ये थैलियाँ हमारे घरों, ऑफिसों, सब्जी की रेहड़ियों, दुकानों से होती हुई पार्कों, सड़क के किनारे की पगडंडियों और कूड़े के ढेरों में पहुँच जाती हैं। और गंदा कर देती हैं मिट्टी को, दिक्कत देती हैं पेड़-पौधों की सिंचाई में। यही थैलियाँ नालियों से होती हुई नदियों में जा पहुँचाती हैं। इनके जलने से जहरीली गैस भी निकलती है।
२)क्या आप जानते हैं इन थैलियों से हर साल लाखों जानवर मारे जाते हैं। इनमें डालफिन, मछलियाँ व अन्य जलचर शामिल हैं। इन्हीं थैलियों में खाने को डालते हैं और यही सब खाकर गाय-भैंस बीमार पड़ती हैं। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि उस जानवर के मारे जाने के बाद भी वो प्लास्टिक उसके शरीर में ज्यों का त्यों रहता है और जो भी अन्य पशु उस मृत पशु को खाता है उसके शरीर में भी प्लास्टिक प्रवेश कर जायेगा।
३)प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म होने में हज़ार वर्ष लग जाते हैं। यानि पर्यावरण में हजार साल तक प्लास्टिक रहेगा।
४)एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि प्लास्टिक पैट्रोलियम पदार्थों से बनता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम के इस्तेमाल से ही पॉलीथीन बनाया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ पहले से ही हमारे जीवन की जरुरत बन चुके हैं। वाहन का ईंधन, घर में रसोई गैस, फैक्ट्री, बिजली घर इत्यादि यानि कि हर पल पेट्रोलियम की जरुरत हमें रहती है। अब यदि पॉलीथीन को इस तरह हम बर्बाद करेंगे तो इसका आशय यह है कि हम अधिकाधिक पेट्रोल को बर्बाद कर रहे हैं।
आखिर हम कर क्या सकते हैं?
प्लास्टिक के बैग की जगह कपड़े व जूट आदि के बने हुए बैग का प्रयोग करें। दूसरा आसान तरीका यह है कि एक ही थैली को बार-बार प्रयोग में लायें। इससे पॉलीथीन का उत्पादन और बर्बादी दोनों कम होगी।
सरकार तो कानून बनाती रहेगी लेकिन पर्यावरण को बचाने और उसकी देखभाल का जिम्मा तो हमारे ऊपर भी है। इस तरह के छोटे-छोटे कदम से हम प्रकृति को खत्म होने से बचा सकते हैं। कहते हैं कि जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है। यदि हम प्रकृति को नुकसान पहुँचायेंगे तो अंत हमारा भी होगा। पर्यावरण को दूषित होने से बचायें। आइये यह संकल्प लें।
तपन शर्मा
Monday, March 30, 2009
....सबको ये फिक्र है कि सरदार कौन हो ??
कहा जाता है कि वह राजनेता उतना ही बड़ा होता है जो जितना बड़ा ख्वाब देखता है। जवाहरलाल नेहरू से ले कर राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण तक की पीढ़ी ख्वाब देखते-देखते गुजर गई। पता नहीं इनमें कौन कितना बड़ा राजनेता था। जब कोई नेता अपने जीवन काल में अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाता, तो उसका कर्तव्य होता है कि वह उस ख्वाब को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर दे। इनमें सबसे ज्यादा सफल नेहरू ही हुए। लोहिया और जयप्रकाश के उत्तराधिकारी लुंपेन बन गए। कुछ का कहना है कि वे शुरू से ही ऐसे थे, पर अपने को साबित करने का पूरा मौका उन्हें बाद में मिला। पर नेहरू का ख्वाब आज भी देश पर राज कर रहा है। नेहरू ने आधुनिक भारत का निर्माण किया था। हम आधुनिकतम भारत का निर्माण कर रहे हैं। सुनते हैं, इस बार के चुनाव का प्रमुख मुद्दा है, विकास। नेहरू का मुद्दा भी यही था। इसी मुद्दे पर चलते-चलते कांग्रेस के घुटने टूट गए। अब फिर वह दौड़ लगाने को तैयार है।
इस देश के सबसे बड़े और संगठित ख्वाब देखनेवाले कम्युनिस्ट थे। उनका ख्वाब एक अंतरराष्ट्रीय ख्वाब से जुड़ा हुआ था। इसलिए वह वास्तव में जितना बड़ा था, देखने में उससे काफी बड़ा लगता था। यह ख्वाब कई देशों में यथार्थ बन चुका था, इसलिए इसकी काफी इज्जत थी। लेकिन जब तेलंगाना में असली आजादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ, तो नेहरू के ख्वाब ने उसे कुचल दिया। तब का दर्द आज तक कम्युनिस्ट ख्वाब को दबोचे हुए है। किताब में कुछ लिख रखा है, पर मुंह से निकलता कुछ और है। कम्युनिस्टों के दो बड़े नेता -- एक प. बंगाल में और दूसरा केरल में -- एक नया ख्वाब देख रहे हैं। समानता के ख्वाब को परे हटा कर वे संपन्नता का ख्वाब देखने में लगे हुए हैं। ईश्वर उनकी सहायता करे, क्योंकि जनता का सहयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
बाबा साहब अंबेडकर ने भी एक ख्वाब देखा था। यह ख्वाब अभी भी फैशन में है। पर सिर्फ बुद्धिजीवियों में। राजनीति में इस ख्वाब ने एक ऐसी जिद्दी महिला को जन्म दिया है जिसका अपना ख्वाब कुछ और है। वे अंबेडकर की मूर्तियां लगवाती हैं, गांवों के साथ उनका नाम जोड़ देती हैं, उनके नाम पर तरह-तरह के आयोजन करती रहती हैं। पर उन्होंने कसम खाई हुई है कि आंबेडकर वास्तव में क्या चाहते थे, यह पता लगाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। इसके लिए अंबेडकर साहित्य पढ़ना होगा और आजकल किस नेता के पास साहित्य पढ़ने का समय है? फिर इस जिद्दी महिला का ख्वाब क्या है? इस बारे में क्या लिखना! बच्चों से ले कर बड़ों तक सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा वे जानते हैं जो तीसरा मोर्चा नाम का चिड़ियाघर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
हिन्दू राष्ट्र के दावेदारों ने भी एक ख्वाब देखा था। उनका ख्वाब काफी पुराना है। जब बाकी लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब वे एक छोटा-सा घर बना कर अपने ख्वाब के भ्रूण का पालन-पोषण कर रहे थे। उनकी रुचि स्वतंत्र भारत में नहीं, हिन्दू भारत में थी। वैसे ही जैसे लीगियों की दिलचस्पी आजाद हिन्दुस्तान में नहीं, मुस्लिम पाकिस्तान में थी। लीगियों को कटा-फटा ही सही, अपना पाकिस्तान मिल गया, पर संघियों को इतिहास ने ठेंगा दिखा दिया। तब से वे स्वतंत्र भारत के संविधान को ठेंगा दिखाने में लगे हुए हैं। लीगियों ने आजादी के पहले खून बहाया था, संघियों ने आजादी के बाद खून बहाया। शुरू में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। वे सिर्फ अपना विचार फैला सके। बाद में जब भारतवाद कमजोर पड़ने लगा, तब हिन्दूवाद के खूनी पंजे भगवा दस्तानों से निकल आए। कोई-कोई अब भी दस्तानों का इस्तेमाल करते हैं,पर उनके भीतर छिपे हाथों का रंग दूर से ही दिखाई देता है।
अब कोई बड़ा ख्वाब देखने का समय नहीं रहा। कुछ विद्वानों का कहना है कि महास्वप्नों का युग विदा हुआ, यह लघु आख्यानों का समय है। भारत में इस समय लघु आख्यान का एक ही मतलब है, प्रधानमंत्री का पद। मंत्री तो गधे भी बन जाते हैं, घोड़े प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ लगाते हैं। अभी तक हम इस पद के लिए दो ही गंभीर उम्मीदवारों को जानते थे। अब महाराष्ट्र से, बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से -- जिधर देखो, उधर से उम्मीदवार उचक-उचक कर सामने आने लगे हैं। यह देख कर मुझे लालकृष्ण आडवाणी से बहुत सहानुभूति होने लगी है। बेचारे कब से नई धोती और नया कुरता ड्राइंग रूम में सजा कर बैठे हुए हैं। इस बार तो उनके इस्तेमाल का मौका नजदीक आते दिखाई नहीं देता। बल्कि रोज एकाध किलोमीटर दूर चला जाता है। चूंकि मैं सभी का और इस नाते उनका भी शुभचिंतक हूं, इसलिए आडवाणी को प्रधानमंत्री बनने का आसान नुस्खा बता देना चाहता हूं। इसके लिए सिर्फ दो शब्द काफी हैं -- पीछे मुड़ (अबाउट टर्न)। सर, संप्रदायवाद, हिन्दू राष्ट्र वगैरह खोटे सिक्कों को सबसे नजदीक के नाले में फेंक दीजिए। आम जनता की भलाई की राजनीति कीजिए। अगली बार आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकेगा।
राजकिशोर
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं...)
इस देश के सबसे बड़े और संगठित ख्वाब देखनेवाले कम्युनिस्ट थे। उनका ख्वाब एक अंतरराष्ट्रीय ख्वाब से जुड़ा हुआ था। इसलिए वह वास्तव में जितना बड़ा था, देखने में उससे काफी बड़ा लगता था। यह ख्वाब कई देशों में यथार्थ बन चुका था, इसलिए इसकी काफी इज्जत थी। लेकिन जब तेलंगाना में असली आजादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ, तो नेहरू के ख्वाब ने उसे कुचल दिया। तब का दर्द आज तक कम्युनिस्ट ख्वाब को दबोचे हुए है। किताब में कुछ लिख रखा है, पर मुंह से निकलता कुछ और है। कम्युनिस्टों के दो बड़े नेता -- एक प. बंगाल में और दूसरा केरल में -- एक नया ख्वाब देख रहे हैं। समानता के ख्वाब को परे हटा कर वे संपन्नता का ख्वाब देखने में लगे हुए हैं। ईश्वर उनकी सहायता करे, क्योंकि जनता का सहयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
बाबा साहब अंबेडकर ने भी एक ख्वाब देखा था। यह ख्वाब अभी भी फैशन में है। पर सिर्फ बुद्धिजीवियों में। राजनीति में इस ख्वाब ने एक ऐसी जिद्दी महिला को जन्म दिया है जिसका अपना ख्वाब कुछ और है। वे अंबेडकर की मूर्तियां लगवाती हैं, गांवों के साथ उनका नाम जोड़ देती हैं, उनके नाम पर तरह-तरह के आयोजन करती रहती हैं। पर उन्होंने कसम खाई हुई है कि आंबेडकर वास्तव में क्या चाहते थे, यह पता लगाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। इसके लिए अंबेडकर साहित्य पढ़ना होगा और आजकल किस नेता के पास साहित्य पढ़ने का समय है? फिर इस जिद्दी महिला का ख्वाब क्या है? इस बारे में क्या लिखना! बच्चों से ले कर बड़ों तक सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा वे जानते हैं जो तीसरा मोर्चा नाम का चिड़ियाघर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
हिन्दू राष्ट्र के दावेदारों ने भी एक ख्वाब देखा था। उनका ख्वाब काफी पुराना है। जब बाकी लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब वे एक छोटा-सा घर बना कर अपने ख्वाब के भ्रूण का पालन-पोषण कर रहे थे। उनकी रुचि स्वतंत्र भारत में नहीं, हिन्दू भारत में थी। वैसे ही जैसे लीगियों की दिलचस्पी आजाद हिन्दुस्तान में नहीं, मुस्लिम पाकिस्तान में थी। लीगियों को कटा-फटा ही सही, अपना पाकिस्तान मिल गया, पर संघियों को इतिहास ने ठेंगा दिखा दिया। तब से वे स्वतंत्र भारत के संविधान को ठेंगा दिखाने में लगे हुए हैं। लीगियों ने आजादी के पहले खून बहाया था, संघियों ने आजादी के बाद खून बहाया। शुरू में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। वे सिर्फ अपना विचार फैला सके। बाद में जब भारतवाद कमजोर पड़ने लगा, तब हिन्दूवाद के खूनी पंजे भगवा दस्तानों से निकल आए। कोई-कोई अब भी दस्तानों का इस्तेमाल करते हैं,पर उनके भीतर छिपे हाथों का रंग दूर से ही दिखाई देता है।
अब कोई बड़ा ख्वाब देखने का समय नहीं रहा। कुछ विद्वानों का कहना है कि महास्वप्नों का युग विदा हुआ, यह लघु आख्यानों का समय है। भारत में इस समय लघु आख्यान का एक ही मतलब है, प्रधानमंत्री का पद। मंत्री तो गधे भी बन जाते हैं, घोड़े प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ लगाते हैं। अभी तक हम इस पद के लिए दो ही गंभीर उम्मीदवारों को जानते थे। अब महाराष्ट्र से, बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से -- जिधर देखो, उधर से उम्मीदवार उचक-उचक कर सामने आने लगे हैं। यह देख कर मुझे लालकृष्ण आडवाणी से बहुत सहानुभूति होने लगी है। बेचारे कब से नई धोती और नया कुरता ड्राइंग रूम में सजा कर बैठे हुए हैं। इस बार तो उनके इस्तेमाल का मौका नजदीक आते दिखाई नहीं देता। बल्कि रोज एकाध किलोमीटर दूर चला जाता है। चूंकि मैं सभी का और इस नाते उनका भी शुभचिंतक हूं, इसलिए आडवाणी को प्रधानमंत्री बनने का आसान नुस्खा बता देना चाहता हूं। इसके लिए सिर्फ दो शब्द काफी हैं -- पीछे मुड़ (अबाउट टर्न)। सर, संप्रदायवाद, हिन्दू राष्ट्र वगैरह खोटे सिक्कों को सबसे नजदीक के नाले में फेंक दीजिए। आम जनता की भलाई की राजनीति कीजिए। अगली बार आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकेगा।
राजकिशोर
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं...)
Sunday, March 29, 2009
महंगाई दर घटी लेकिन तेज़ी वहीं की वहीं
 सरकार महंगाई दर कम होने पर अपनी पीठ ठोक रही है कि 14 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान यह घट कर 0.27 प्रतिशत पर आ गई है। यह महंगाई की दर में वृद्वि का पिछले 30 वर्षों का सबसे नीचा स्तर है। सरकार के लिए संतोष की बात है भी क्योंकि गत वर्ष इसी अवधि में यह 8.02 प्रतिशत थी। यही नहीं गत वर्ष अगस्त में यह दर 13 प्रतिशत का आकंड़ा छू गई थी। उस समय पूरा मीडिया महंगाई को लेकर सरकार के पीछे पड़ गया था। इसे देखते हुए सरकार के लिए यह राहत की बात है। यही नहीं आगामी आम चुनाव को देखते हुए भी सरकार प्रसन्न है कि चलो महंगाई की दर पर काबू तो पाया।
सरकार महंगाई दर कम होने पर अपनी पीठ ठोक रही है कि 14 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान यह घट कर 0.27 प्रतिशत पर आ गई है। यह महंगाई की दर में वृद्वि का पिछले 30 वर्षों का सबसे नीचा स्तर है। सरकार के लिए संतोष की बात है भी क्योंकि गत वर्ष इसी अवधि में यह 8.02 प्रतिशत थी। यही नहीं गत वर्ष अगस्त में यह दर 13 प्रतिशत का आकंड़ा छू गई थी। उस समय पूरा मीडिया महंगाई को लेकर सरकार के पीछे पड़ गया था। इसे देखते हुए सरकार के लिए यह राहत की बात है। यही नहीं आगामी आम चुनाव को देखते हुए भी सरकार प्रसन्न है कि चलो महंगाई की दर पर काबू तो पाया।महंगाई की गिरती दर को देखते हुए अनेक अर्थशास्त्री देश में मुद्रा स्फीति की बजाए अपस्फीति की आशंका जताने लगे हैं।
विरोधाभास
वास्तव में सरकार के बयानों में ही विरोधाभास है। थोक मूल्य सूचकांक उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि देश में महंगाई की दर कम हो रही है और आगामी सप्ताहों में यह शून्य पर आ जाएगी या निगेटिव हो जाएगी।
लेकिन वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार स्वयं यह मान रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई है। उनका कहना है कि महंगाई की दर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निकाली जाती है। यह ठीक है कि थोक मूल्य सूचकांक में लगातार कमी आ रही है लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्वि दर तो अब भी 10 प्रतिशत के आसपास घूम रही है।
उपभोक्ता हैरान
बरहहाल, इन सब से आम उपभोक्ता हतप्रभ है। वह महंगाई की दर 13 प्रतिशत के आसपास पहुंचने के बाद परेशान तो था लेकिन अब गिर कर 0.27 प्रतिशत आ जाने पर प्रसन्न नहीं लेकिन हैरान अवश्य है कि यह क्या हो रहा है? उसका बजट तो वहीं का वहीं है या बढ़ रहा है, फिर महंगाई कैसे कम हो रही है।
क्या है सूचकांक
थोक मूल्य सूचकांक में लगभग एक हजार विभिन्न वस्तुओं का समावेश है। दिलचस्प बात यह है कि सूचकांक की लगभग 78 प्रतिशत वस्तुएं वे हैं जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी को आवश्यकता ही नहीं होती है। इनमें विभिन्न रसायन, धातुएं, विभिन्न प्रकार के ईंधन, ग्रीस, रंग-रोगन, सीमेंट, स्टील, मशीनरी व मशीन टूल, पुस्तकों व समाचार पत्रों की प्रिन्टिग, पल्प, कागज आदि अनेक वस्तुएं इस सूची में शामिल हैं। शेष 22 प्रतिशत में वे वस्तुएं हैं जिनकी रोज आवश्यकता होती है।
आंकड़ों की सच्चाई
आम उपभोग की अनेक वस्तुओं के भाव दिल्ली बाजार में गत वर्ष की तुलना में ऊंचे चल रहे हैं। गत वर्ष दिल्ली बाजार में चीनी के एक्स मिल भाव 1600 रुपए के आसपास चल रहे थे जो अब लगभग 2200 रुपए (थोक में 25 रुपए किलो) चल रहे हैं। गुड़ के भाव तो इससे भी आगे हैं। गेहूं दड़ा क्वालिटी के थोक भाव 1125/1130 रुपए से बढ़ कर 1160/1165 रुपए हो गए हैं। मूंग के भाव गत वर्ष 2200/2650 रुपए थे जो अब 3500/4000 रुपए हो गए हैं। रंगून की अरहर गत वर्ष 2575/2600 रुपए थी जो अब 3500 रुपए पार कर गई है। रंगून की उड़द भी 2375/2400 रुपए से बढ़ कर 2800 रुपए के आसपास हो गई है। चने के भाव गत वर्ष की तुलना में अवश्य कम हैं। मसालों के भाव भी गत वर्ष की तुलना में काफी तेज हैं लेकिन खाद्य तेलों के भाव नीचे चल रहे हैं।
सरकारी आंकड़े
यदि सरकारी आंकड़ों को देखें तो भी यह स्पष्ट है कि खाद्य वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक बढ़ा है। इस वर्ष 14 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान दलहनों का थोक मूल्य सूचकांक 269.1 था जो गत वर्ष 15 मार्च को 244.7 था। अनाजों का सूचकांक आलोच्य अवधि में 219.4 से बढ़ कर 241.6 पर पहुंच गया है। सब्जियों व फलों का सूचकांक 234.8 से बढ़ कर 247.6 हो गया है। दूध का सूचकांक 220.3 से बढ़ कर 233.7 हो गया है। इसी प्रकार मसालों, खांडसार, गुड़ व चीनी तथा अन्य खाद्य उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक बढ़ा है लेकिन अन्य व गैर खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में कमी के कारण महंगाई की दर में बढ़ोतरी कम हो गई है।
यहां यह जानना भी आवश्यक है कि महंगाई की दर में बढ़ोतरी की गति कम हुई लेकिन वह घट नहीं रही है।
--राजेश शर्मा
Saturday, March 28, 2009
सोने का पिंजर (10)
दसवां अध्याय
अमेरिका के कुत्ते बच्चों से ज़्यादा प्यार पाते हैं....
अमेरिका में रेस्ट्राज की भरमार आपको मिलेगी, सभी तरह के खाने आपको मिल जाएँगे। एक लाइन से रेस्ट्रा है, थाई, मलेशियायी, चीनी, इण्डियन, वियतनामी आदि आदि। लेकिन भारतीय स्वाद का जवाब नहीं। किसी भी भारतीय रेस्ट्रा में चले जाइए आपको ढेर सारे अमेरिकी मिल जाएँगे। समोसा और नान सबसे अधिक पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता, लेकिन स्वाद और साइज़ में बहुत अंतर। भारतीयों के लिए सबसे मुश्किल है रोटी। बाजार में बनी-बनाई भी खूब मिलती है लेकिन अपने यहाँ की मालपुए-सी रोटी वहाँ नसीब नहीं होती। आप ठीक सोच रहे हैं कि घर पर क्यों नहीं बना लेते? घर पर सभी बनाते हैं रोटी, लेकिन आटे में स्वाद हो तब तो बने अपने जैसी रोटी। एक घटना याद आ गई, उदयपुर के बहुत बड़े उद्योगपति का समाचार था कि वे जब भी यूरोप जाते हैं, अपने साथ आटा लेकर जाते हैं। एक बार कस्टम वालों ने पकड़ लिया और काफी कठिनाई का उन्हें सामना करना पड़ा। तब मन में प्रश्न आया था कि आटा जैसी चीज वे क्यों ले जाते हैं? फिर सोचा था कि शायद वहाँ भी बाजार में मैदे का आटा ही मिलता होगा। एक बात और मन में आयी कि भई बड़े लोग हैं, तो उनके चोंचले भी बड़े ही होंगे। ये पता नहीं था कि वहाँ अपने जैसा आटा नहीं मिलता। पहले दिन घर में रोटी खायी, स्वाद ही नहीं आया। तो बेटे से कहा कि आटा कुछ अजीब है, उसने उसे बदल दिया और बाजार से दूसरा ले आया। अब भी वही स्थिति। फिर हमने जुबान पर ताला लगा लिया। एक-दो जगह गए और धीरे से आटे के बारे में पूछ लिया तो मालूम पड़ा कि यह तो सभी की परेशानी का सबब है। फिर लगा कि उन उद्योगपति का चोंचला सही था। कृषि क्षेत्र में बहुत प्रयोग किए हैं अमेरिका ने। शायद ऐसा ही कोई प्रयोग गैंहू में किया हो, क्योंकि उन्हें रोटी का स्वाद पता नहीं, वे तो ब्रेड खाते हैं। अतः जो ब्रेड में अच्छा स्वाद दे, वैसा ही गैंहू बना दो, शायद।
सेब और आडू को मिलाकर कई फल तैयार हो गए, ऐसे ही अनेक संकर फल आपको वहाँ मिल जाएंगे। किसी में स्वाद है और किसी में नहीं। अब जब संकर प्रजातियों की बात ही आ गयी है तो एक और मजे़दार मानसिकता वहाँ दिखायी दी। कुत्तों को लेकर वे बहुत प्रयोगवादी हैं। कॉलोनी में अक्सर प्रत्येक व्यक्ति सुबह-शाम कुत्ते घुमाता हुआ दिखायी दे जाएगा। एक-एक व्यक्ति के पास तीन-तीन कुत्ते। मजेदार बात यह है कि सारे ही कुत्ते एक दूसरे से अलग। स्ट्रीट डॉग वहाँ नहीं हैं, लेकिन घरों में कुत्तों और बिल्लियों की भरमार है। बाज़ार में उनके लिए बड़े-बड़े मॉल है, जहाँ उनका खाना से लेकर बिस्तर तक उपलब्ध हैं। उनके सेलून भी हैं और अस्पताल भी।
कुछ घरों में तो केवल कुत्ते-बिल्ली ही हैं, बच्चे नहीं। वहाँ व्यक्ति पहले कुत्ता पालता है और उसके बाद उसके पास आर्थिक सामर्थ्य होता है तब बच्चे पैदा करता है। शायद सुरक्षित सुख इसी में है। जिम्मेदारी रहित सुख। किसी को दो दिन के लिए बाहर जाना है तो पड़ौस में कुत्ते को बाँध गए या फिर अपने परिचित से कह दिया कि ध्यान रख लेना। बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते न? कुत्ता दूसरे पर भौंकता है जबकि बच्चा अपनों पर। भौंकने की बात पर ध्यान आया कि हमारे यहाँ जब भाग्य से कभी-कभार रात को कुछ शोरगुल थमता है तब कुत्तों के भौंकने की आवाजे आप बड़े मनोयोग पूर्वक सुन सकते हैं। ये आवाज़ें जरूरी नहीं कि गली के कुत्तों की हो, वे पालतू कुत्तों की भी होती है। वैसे अमेरिका में लोग इतने प्यार से कुत्ते पालते हैं कि मुझे यहाँ उनके लिए कुत्ते शब्द का प्रयोग खल रहा है। तो वहाँ कुत्ते भी भौंकते नहीं है और दूसरे को देखकर झपटते नहीं हैं। यहाँ तो गोद मे चढ़ा पिल्ला भी दूसरे को देखकर गुर्रा लेता है और फिर मालिक उसे प्यार से थपथपाता है और चुप कराता है तब वह शान से अपनी अदा बिखेरता हुआ कूं-कूं कर देता है। मालिक की गर्दन भी गर्व से तन जाती है, कि देखो मेरा पिल्ला भी कैसा जागरूक है? लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, लोग चुपचाप अपने कुत्तों को घुमाते रहते हैं, आप पास से निकल जाएं कुत्ता कोई हरकत नहीं करता। जहाँ के कुत्ते तक इतने शान्त हो, वहाँ के व्यक्ति का क्या कहना? तभी तो वे एशियन्स को देखते ही घबरा जाते हैं, आ गए आतंकवादी। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बहुत अन्तर नहीं है वहाँ, उनके लिए सब ही लड़ाका हैं।
एक मजे़दार किस्सा है, किस्सा क्या है सत्य घटना है। पोता अभी पाँच महिने का ही था, घुटनों के बल चलता था। बेटे का एक अमेरिकन दोस्त है-मार्टिन, उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन बेटा मार्टिन से मिलने गया, साथ में अपने नन्हें से बेटे को भी ले गया। मन में डर भी था कि कहीं बिल्ली से बच्चा डर नहीं जाए। घर पहुँचकर पोता खेलने लगा और दोनों दोस्त बातों में रम गए। कुछ देर बाद रोने की आवाज सुनाई दी, तब बेटे को होश आया। अरे कहीं चुन्नू को तो बिल्ली ने नहीं मारा है? लेकिन यह क्या बिल्ली एक कोने में दुबकी हुई चुन्नू को देखकर रो रही थी। हमारे यहाँ बिल्ली घाट-घाट का पानी पीती है, घर-घर जाकर दूध साफ करती है। लेकिन वहाँ घर में बंद रहती है। सुबह-शाम मालिक घुमाने ले जाता है, तब कोई भी सड़क पर घुटने चलता बच्चा नजर नहीं आता। बेचारी बिल्ली ने कभी बच्चों को घुटने चलते देखा ही नहीं तो उसने समझा कि कौन सा जानवर आ गया है, इतना बड़ा?
भारत की भूमि पर घर-घर में कृष्ण के बाल रूप के दर्शन हो जाते हैं। सुबह उन्हें नहलाया जाता है, भोग लगता है, झाँकी होती है और सारा दिन कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वहाँ सारा दिन कुत्तों और बिल्लियों के साथ कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वहाँ कुत्तों-बिल्लियों तक ही लोग सीमित नहीं है, छिपकली तक पाल लेते हैं। शहरों में कहीं भी पशु-पक्षियों के दर्शन नहीं होते तो वीकेंड पर कैंप लगाकर जंगलों की खाक छानते रहते हैं, जानवरों को देखने के लिए। एक ऐसे ही जंगल में हम भी गए। घूमते-घूमते मालूम पड़ा कि यहाँ भालू है। बस फिर क्या था, हम भी घुस पड़े जंगल में। वहाँ देखा पहले से ही दसेक लोग भालू को निहारने के लिए खड़े हैं। भालू मजे से पेड़ पर चढ़कर सेव खा रहा था। हम और अंदर चले गए, हमें दो और भालू दिख गए। दो-तीन लोग तो ज्यादा ही अंदर चले गए। लेकिन हम समय पर बाहर आ गए, हमारे बाहर आते ही रेंजर काफिले सहित आ गया और सभी को ऐसा नहीं करने की हिदायत देने लगा। हम तो सबकुछ देखकर चुपचाप खिसक आए।
जंगलों में भी वहाँ जानवर दिखायी नहीं देते। वहाँ होटल परिसर में मोटी-ताजी गिलहरी घूम रही थी बस वे ही सब के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई थीं। जंगल भी जानवरों से रिक्त कैसे हैं, यह हमें समझ नहीं आया। शहर तो सारे ही कीड़े-मकोड़ों से रिक्त हैं ही। वहाँ लगा कि वास्तव में आदमी ने दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा लिया है। अभी भारत इस बात में पिछड़ा हुआ है। यहाँ सारे ही जीव-जन्तु भी साथ-साथ पलते हैं। इस धरती पर मनुष्य ही स्वेच्छा से विचरण करे शायद इसे ही विकास कहते हैं। हमारे जंगलों में, शहरों में कितने जीव मिलते हैं? सुबह पेड़ों पर तोते अमरूद खाते मिल जाएंगे, बंदर छलांग लगाते, हूप-हूप बोलते हुए दिख जाएंगे। कौवा तो जैसे पाहुने का संदेशा लाने के लिए ही मुंडेर पर आकर बैठता है। कोयल सावन का संदेशा ले आती है। चिड़िया, कबूतर तो घर में घोंसला बनाने को तैयार ही रहते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में चले जाइए, मोर नाचते आपको मिल जाएंगे।
हम मानते हैं कि देश का विकास दो प्रकार का होता है, एक सभ्यता का विकास और दूसरा संस्कृति का विकास। अमेरिकी भौतिक स्वरूप का विकास अर्थात सभ्यता का विकास पूर्ण रूप में है और भारत इस मायने में विकासशील देश कहलाता है। अमेरिका पूँजीवादी देश है और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ कर ली है कि वे सारी दुनिया को पैसा उधार देते हैं और ब्याज के बदले में सारी जीवनोपयोगी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। सारा बाजार एशिया की वस्तुओं से भरा हुआ है। 25 प्रतिशत एशियायी उनके भौतिक स्वरूप के विकास में भागीदार हैं। वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति टैक्स देता है, जबकि हमारे यहाँ टैक्स देने वालों का प्रतिशत क्या है? एक सज्जन ने बताया कि यहाँ टैक्स की आमदनी ही इतनी है कि इन्हें समझ नहीं आता कि इस पैसे को कहाँ खर्च करें? परिणाम सारी दुनिया को खैरात बाँटना और फिर उनकी प्रकृति-प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करना। अमेरिका के पास भी प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता है लेकिन वह इनका उपयोग नहीं करता। जब दुनिया के संसाधन समाप्त हो जाएँगे तब हम उनका उपभोग करेंगे, यह है उनकी मानसिकता। इसलिए ही खाड़ी के देशों से तैल की लड़ाई लड़ी जा रही है। उनकी सभ्यता के विकास के पीछे है उनका अर्थप्रधान सोच है। दुनिया के सारे संसाधन, बौद्धिक प्रतिभा सब कुछ एकत्र करो और अमेरिका के लिए प्रयोग करो। ऐसा कौन करने में समर्थ होता है, निःसंदेह ताकतवर इंसान। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वे विज्ञान के इस सिद्धान्त को वरीयता देते हैं कि जो भी ताकतवर हैं वे ही जीवित रहेगा। अतः उनकी जीवनपद्धति का मूल मंत्र ताकत एकत्र करना है।
प्रकृति सारे ही जीव-जन्तुओं के सहारे सुरक्षित रहती है, लेकिन अमेरिका में सभी के स्थान निश्चित हैं, जहाँ मनुष्य रहेंगे, वहाँ ये नहीं रहेंगे। अर्थात सारी प्रकृति को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति। भोग-विलास के लिए एकत्रीकरण की प्रवृत्ति। त्याग और समर्पण के लिए कहीं स्थान नहीं। टेक्स के रूप में देने का अर्थ भी क्लब जैसी मानसिकता के रूप में परिलक्षित होता है। देश का मेनेजमेंट सरकार के रूप में तुम देखते हो तो टेक्स लो और हमें सुविधाएं दो। उसमें त्याग की भावना नहीं है। भारत में त्याग ही त्याग है। हम टेक्स के रूप में कुछ नहीं देना चाहते लेकिन दान के रूप में सबकुछ दे देते हैं। इसलिए हमारा सांस्कृतिक विकास पूर्ण हैं। भारत की जनसंख्या सौ करोड़ से भी अधिक है, यदि भारत में भी लोग अमेरिका की तरह टैक्स देने लग जाएं तो शायद सर्वाधिक टेक्स हमारे देश में आएगा। फिर विकास की कैसी गंगा बहेगी, इसकी शायद हमें कल्पना नहीं है? हम केवल दान देकर स्वयं को भगवान बनाने में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ भौतिक विकास का कभी चिंतन हुआ ही नहीं, बस आध्यात्मिक विकास के लिए ही हम हमेशा चिंतित रहते हैं। हम केवल अपने लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए, चर-अचर जगत के लिए चिंतन करते हैं। शायद हमारा यही सांस्कृतिक सोच कभी विश्व को बचाने में समर्थ बनेगा। आज नवीन पीढ़ी को यह दकियानूसी लगता है लेकिन कल यही सिद्धान्त सभी को आकर्षित करेगा।
डॉ अजित गुप्ता
अमेरिका के कुत्ते बच्चों से ज़्यादा प्यार पाते हैं....
अमेरिका में रेस्ट्राज की भरमार आपको मिलेगी, सभी तरह के खाने आपको मिल जाएँगे। एक लाइन से रेस्ट्रा है, थाई, मलेशियायी, चीनी, इण्डियन, वियतनामी आदि आदि। लेकिन भारतीय स्वाद का जवाब नहीं। किसी भी भारतीय रेस्ट्रा में चले जाइए आपको ढेर सारे अमेरिकी मिल जाएँगे। समोसा और नान सबसे अधिक पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता, लेकिन स्वाद और साइज़ में बहुत अंतर। भारतीयों के लिए सबसे मुश्किल है रोटी। बाजार में बनी-बनाई भी खूब मिलती है लेकिन अपने यहाँ की मालपुए-सी रोटी वहाँ नसीब नहीं होती। आप ठीक सोच रहे हैं कि घर पर क्यों नहीं बना लेते? घर पर सभी बनाते हैं रोटी, लेकिन आटे में स्वाद हो तब तो बने अपने जैसी रोटी। एक घटना याद आ गई, उदयपुर के बहुत बड़े उद्योगपति का समाचार था कि वे जब भी यूरोप जाते हैं, अपने साथ आटा लेकर जाते हैं। एक बार कस्टम वालों ने पकड़ लिया और काफी कठिनाई का उन्हें सामना करना पड़ा। तब मन में प्रश्न आया था कि आटा जैसी चीज वे क्यों ले जाते हैं? फिर सोचा था कि शायद वहाँ भी बाजार में मैदे का आटा ही मिलता होगा। एक बात और मन में आयी कि भई बड़े लोग हैं, तो उनके चोंचले भी बड़े ही होंगे। ये पता नहीं था कि वहाँ अपने जैसा आटा नहीं मिलता। पहले दिन घर में रोटी खायी, स्वाद ही नहीं आया। तो बेटे से कहा कि आटा कुछ अजीब है, उसने उसे बदल दिया और बाजार से दूसरा ले आया। अब भी वही स्थिति। फिर हमने जुबान पर ताला लगा लिया। एक-दो जगह गए और धीरे से आटे के बारे में पूछ लिया तो मालूम पड़ा कि यह तो सभी की परेशानी का सबब है। फिर लगा कि उन उद्योगपति का चोंचला सही था। कृषि क्षेत्र में बहुत प्रयोग किए हैं अमेरिका ने। शायद ऐसा ही कोई प्रयोग गैंहू में किया हो, क्योंकि उन्हें रोटी का स्वाद पता नहीं, वे तो ब्रेड खाते हैं। अतः जो ब्रेड में अच्छा स्वाद दे, वैसा ही गैंहू बना दो, शायद।
सेब और आडू को मिलाकर कई फल तैयार हो गए, ऐसे ही अनेक संकर फल आपको वहाँ मिल जाएंगे। किसी में स्वाद है और किसी में नहीं। अब जब संकर प्रजातियों की बात ही आ गयी है तो एक और मजे़दार मानसिकता वहाँ दिखायी दी। कुत्तों को लेकर वे बहुत प्रयोगवादी हैं। कॉलोनी में अक्सर प्रत्येक व्यक्ति सुबह-शाम कुत्ते घुमाता हुआ दिखायी दे जाएगा। एक-एक व्यक्ति के पास तीन-तीन कुत्ते। मजेदार बात यह है कि सारे ही कुत्ते एक दूसरे से अलग। स्ट्रीट डॉग वहाँ नहीं हैं, लेकिन घरों में कुत्तों और बिल्लियों की भरमार है। बाज़ार में उनके लिए बड़े-बड़े मॉल है, जहाँ उनका खाना से लेकर बिस्तर तक उपलब्ध हैं। उनके सेलून भी हैं और अस्पताल भी।
कुछ घरों में तो केवल कुत्ते-बिल्ली ही हैं, बच्चे नहीं। वहाँ व्यक्ति पहले कुत्ता पालता है और उसके बाद उसके पास आर्थिक सामर्थ्य होता है तब बच्चे पैदा करता है। शायद सुरक्षित सुख इसी में है। जिम्मेदारी रहित सुख। किसी को दो दिन के लिए बाहर जाना है तो पड़ौस में कुत्ते को बाँध गए या फिर अपने परिचित से कह दिया कि ध्यान रख लेना। बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते न? कुत्ता दूसरे पर भौंकता है जबकि बच्चा अपनों पर। भौंकने की बात पर ध्यान आया कि हमारे यहाँ जब भाग्य से कभी-कभार रात को कुछ शोरगुल थमता है तब कुत्तों के भौंकने की आवाजे आप बड़े मनोयोग पूर्वक सुन सकते हैं। ये आवाज़ें जरूरी नहीं कि गली के कुत्तों की हो, वे पालतू कुत्तों की भी होती है। वैसे अमेरिका में लोग इतने प्यार से कुत्ते पालते हैं कि मुझे यहाँ उनके लिए कुत्ते शब्द का प्रयोग खल रहा है। तो वहाँ कुत्ते भी भौंकते नहीं है और दूसरे को देखकर झपटते नहीं हैं। यहाँ तो गोद मे चढ़ा पिल्ला भी दूसरे को देखकर गुर्रा लेता है और फिर मालिक उसे प्यार से थपथपाता है और चुप कराता है तब वह शान से अपनी अदा बिखेरता हुआ कूं-कूं कर देता है। मालिक की गर्दन भी गर्व से तन जाती है, कि देखो मेरा पिल्ला भी कैसा जागरूक है? लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, लोग चुपचाप अपने कुत्तों को घुमाते रहते हैं, आप पास से निकल जाएं कुत्ता कोई हरकत नहीं करता। जहाँ के कुत्ते तक इतने शान्त हो, वहाँ के व्यक्ति का क्या कहना? तभी तो वे एशियन्स को देखते ही घबरा जाते हैं, आ गए आतंकवादी। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बहुत अन्तर नहीं है वहाँ, उनके लिए सब ही लड़ाका हैं।
एक मजे़दार किस्सा है, किस्सा क्या है सत्य घटना है। पोता अभी पाँच महिने का ही था, घुटनों के बल चलता था। बेटे का एक अमेरिकन दोस्त है-मार्टिन, उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन बेटा मार्टिन से मिलने गया, साथ में अपने नन्हें से बेटे को भी ले गया। मन में डर भी था कि कहीं बिल्ली से बच्चा डर नहीं जाए। घर पहुँचकर पोता खेलने लगा और दोनों दोस्त बातों में रम गए। कुछ देर बाद रोने की आवाज सुनाई दी, तब बेटे को होश आया। अरे कहीं चुन्नू को तो बिल्ली ने नहीं मारा है? लेकिन यह क्या बिल्ली एक कोने में दुबकी हुई चुन्नू को देखकर रो रही थी। हमारे यहाँ बिल्ली घाट-घाट का पानी पीती है, घर-घर जाकर दूध साफ करती है। लेकिन वहाँ घर में बंद रहती है। सुबह-शाम मालिक घुमाने ले जाता है, तब कोई भी सड़क पर घुटने चलता बच्चा नजर नहीं आता। बेचारी बिल्ली ने कभी बच्चों को घुटने चलते देखा ही नहीं तो उसने समझा कि कौन सा जानवर आ गया है, इतना बड़ा?
भारत की भूमि पर घर-घर में कृष्ण के बाल रूप के दर्शन हो जाते हैं। सुबह उन्हें नहलाया जाता है, भोग लगता है, झाँकी होती है और सारा दिन कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वहाँ सारा दिन कुत्तों और बिल्लियों के साथ कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वहाँ कुत्तों-बिल्लियों तक ही लोग सीमित नहीं है, छिपकली तक पाल लेते हैं। शहरों में कहीं भी पशु-पक्षियों के दर्शन नहीं होते तो वीकेंड पर कैंप लगाकर जंगलों की खाक छानते रहते हैं, जानवरों को देखने के लिए। एक ऐसे ही जंगल में हम भी गए। घूमते-घूमते मालूम पड़ा कि यहाँ भालू है। बस फिर क्या था, हम भी घुस पड़े जंगल में। वहाँ देखा पहले से ही दसेक लोग भालू को निहारने के लिए खड़े हैं। भालू मजे से पेड़ पर चढ़कर सेव खा रहा था। हम और अंदर चले गए, हमें दो और भालू दिख गए। दो-तीन लोग तो ज्यादा ही अंदर चले गए। लेकिन हम समय पर बाहर आ गए, हमारे बाहर आते ही रेंजर काफिले सहित आ गया और सभी को ऐसा नहीं करने की हिदायत देने लगा। हम तो सबकुछ देखकर चुपचाप खिसक आए।
जंगलों में भी वहाँ जानवर दिखायी नहीं देते। वहाँ होटल परिसर में मोटी-ताजी गिलहरी घूम रही थी बस वे ही सब के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई थीं। जंगल भी जानवरों से रिक्त कैसे हैं, यह हमें समझ नहीं आया। शहर तो सारे ही कीड़े-मकोड़ों से रिक्त हैं ही। वहाँ लगा कि वास्तव में आदमी ने दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा लिया है। अभी भारत इस बात में पिछड़ा हुआ है। यहाँ सारे ही जीव-जन्तु भी साथ-साथ पलते हैं। इस धरती पर मनुष्य ही स्वेच्छा से विचरण करे शायद इसे ही विकास कहते हैं। हमारे जंगलों में, शहरों में कितने जीव मिलते हैं? सुबह पेड़ों पर तोते अमरूद खाते मिल जाएंगे, बंदर छलांग लगाते, हूप-हूप बोलते हुए दिख जाएंगे। कौवा तो जैसे पाहुने का संदेशा लाने के लिए ही मुंडेर पर आकर बैठता है। कोयल सावन का संदेशा ले आती है। चिड़िया, कबूतर तो घर में घोंसला बनाने को तैयार ही रहते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में चले जाइए, मोर नाचते आपको मिल जाएंगे।
हम मानते हैं कि देश का विकास दो प्रकार का होता है, एक सभ्यता का विकास और दूसरा संस्कृति का विकास। अमेरिकी भौतिक स्वरूप का विकास अर्थात सभ्यता का विकास पूर्ण रूप में है और भारत इस मायने में विकासशील देश कहलाता है। अमेरिका पूँजीवादी देश है और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ कर ली है कि वे सारी दुनिया को पैसा उधार देते हैं और ब्याज के बदले में सारी जीवनोपयोगी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। सारा बाजार एशिया की वस्तुओं से भरा हुआ है। 25 प्रतिशत एशियायी उनके भौतिक स्वरूप के विकास में भागीदार हैं। वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति टैक्स देता है, जबकि हमारे यहाँ टैक्स देने वालों का प्रतिशत क्या है? एक सज्जन ने बताया कि यहाँ टैक्स की आमदनी ही इतनी है कि इन्हें समझ नहीं आता कि इस पैसे को कहाँ खर्च करें? परिणाम सारी दुनिया को खैरात बाँटना और फिर उनकी प्रकृति-प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करना। अमेरिका के पास भी प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता है लेकिन वह इनका उपयोग नहीं करता। जब दुनिया के संसाधन समाप्त हो जाएँगे तब हम उनका उपभोग करेंगे, यह है उनकी मानसिकता। इसलिए ही खाड़ी के देशों से तैल की लड़ाई लड़ी जा रही है। उनकी सभ्यता के विकास के पीछे है उनका अर्थप्रधान सोच है। दुनिया के सारे संसाधन, बौद्धिक प्रतिभा सब कुछ एकत्र करो और अमेरिका के लिए प्रयोग करो। ऐसा कौन करने में समर्थ होता है, निःसंदेह ताकतवर इंसान। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वे विज्ञान के इस सिद्धान्त को वरीयता देते हैं कि जो भी ताकतवर हैं वे ही जीवित रहेगा। अतः उनकी जीवनपद्धति का मूल मंत्र ताकत एकत्र करना है।
प्रकृति सारे ही जीव-जन्तुओं के सहारे सुरक्षित रहती है, लेकिन अमेरिका में सभी के स्थान निश्चित हैं, जहाँ मनुष्य रहेंगे, वहाँ ये नहीं रहेंगे। अर्थात सारी प्रकृति को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति। भोग-विलास के लिए एकत्रीकरण की प्रवृत्ति। त्याग और समर्पण के लिए कहीं स्थान नहीं। टेक्स के रूप में देने का अर्थ भी क्लब जैसी मानसिकता के रूप में परिलक्षित होता है। देश का मेनेजमेंट सरकार के रूप में तुम देखते हो तो टेक्स लो और हमें सुविधाएं दो। उसमें त्याग की भावना नहीं है। भारत में त्याग ही त्याग है। हम टेक्स के रूप में कुछ नहीं देना चाहते लेकिन दान के रूप में सबकुछ दे देते हैं। इसलिए हमारा सांस्कृतिक विकास पूर्ण हैं। भारत की जनसंख्या सौ करोड़ से भी अधिक है, यदि भारत में भी लोग अमेरिका की तरह टैक्स देने लग जाएं तो शायद सर्वाधिक टेक्स हमारे देश में आएगा। फिर विकास की कैसी गंगा बहेगी, इसकी शायद हमें कल्पना नहीं है? हम केवल दान देकर स्वयं को भगवान बनाने में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ भौतिक विकास का कभी चिंतन हुआ ही नहीं, बस आध्यात्मिक विकास के लिए ही हम हमेशा चिंतित रहते हैं। हम केवल अपने लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए, चर-अचर जगत के लिए चिंतन करते हैं। शायद हमारा यही सांस्कृतिक सोच कभी विश्व को बचाने में समर्थ बनेगा। आज नवीन पीढ़ी को यह दकियानूसी लगता है लेकिन कल यही सिद्धान्त सभी को आकर्षित करेगा।
डॉ अजित गुप्ता
Subscribe to:
Posts (Atom)
बहस का हिस्सा बनिए॰॰॰
स्थाई पाठक बनिए
बैठकबाज और उनकी बैठकें
अनिरूद्ध शर्मा
अबयज़ खान
अभिषेक पाटनी
डॉ॰ अजित गुप्ता
तपन शर्मा
नाज़िम नक़वी
निखिल आनंद गिरि
नीलम मिश्रा
प्रेमचंद सहजवाला
भूपेन्द्र राघव
मनु बे-तखल्लुस
राजकिशोर
राजेश शर्मा
शैलेश भारतवासी
हार्दिक मेहता
सुनील डोगरा ज़ालिम
- ऐ शहीदे मुल्को-मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार
- आशिकों का आज जमघट कूच-ए-कातिल में है
- क्या तमन्ना-ऐ- शहादत भी किसी के दिल में है (1)
- क्या तमन्ना-ऐ- शहादत भी किसी के दिल में है (2)
- देखना है ज़ोर कितना बाज़ू ए कातिल में है...
- सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है...
- हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है...
- रहबरे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में...
- लज्ज़ते सहरा-नवर्दी दूरिये - मंजिल में है
- अब न अहले-वलवले हैं और न अरमानों की भीड़
विशेष
लोकसभा चुनाव 2009
ब्लू फिल्म (गौरव सोलंकी
भगत सिंहः कुछ और पन्ने
- मुसलमान बेआवाज़ क्यों
- भारत का आम आदमी कब महान होगा ?
- एक वेबसाइट ऐसी भी.....
- ....सबको ये फिक्र है कि सरदार कौन हो ??
- लोकतंत्र से ज़्यादा अहम आईपीएल ???
- इंटरनेट की पटरी पर आडवाणी की पीएम यात्रा...
- क्या आप सुन पाए संसद में सिसकी....
- चुनाव नाम की लूट है लुटा सके तो लुटा
- राहुल, मनमोहन या आडवाणी: युवा कौन?
- आज़ादी से पहले और बाद के जूता-काण्ड
- अजय माकन को अपनी तथा मनमोहन सिंह दोनों की छवियों का दोहरा लाभ
- जनता ने भर दी है हामी, एम एल ए होंगे गोस्वामी
- फिर भी कुंवारे रह गये अटलजी...
- 15वीं लोकसभा चुनाव को याद रखने के कई कारण
- चुनाव से पहले इम्तिहान देंगे नेता तब वोट करेगी जनता
- भाजपा प्रचार जानी पहचानी लीक पर
- यथा-राजा तथा-प्रजा
- गिरता मतदान- लोकतंत्र या अल्पतंत्र
- कार्टून- क्या करें मज़बूरी भी कोई चीज है
शहीद भगत सिंह की 102वीं जयंती पर उनके जीवन दर्शन, संघर्ष और गाँधी-दर्शन से मतांतर पर हमने आलेखों की एक शृंखला प्रकाशित की है॰॰॰
- 1. ऐ शहीदे मुल्को-मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार
- 2. आशिकों का आज जमघट कूच-ए-कातिल में है
- 3. क्या तमन्ना-ऐ- शहादत भी किसी के दिल में है (1)
- 4. क्या तमन्ना-ऐ- शहादत भी किसी के दिल में है (2)
- 5. देखना है ज़ोर कितना बाज़ू ए कातिल में है...
- 6. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है...
- 7. हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है...
- 8. रहबरे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में...
- 9. लज्ज़ते सहरा-नवर्दी दूरिये - मंजिल में है
- 10. अब न अहले-वलवले हैं और न अरमानों की भीड़
- 11. खींच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद ....
- 12. एक मर मिटने की हसरत ही दिले-बिस्मिल में है
- 13. अहिंसा परमो-धर्मः
यादें
सिनेमाघर जाने से पहले
सप्ताह की बड़ी रीलिज पर पढ़िए फिल्म-समीक्षक प्रशेन की राय--
नई पोस्ट
संग्रहालय
-
▼
2011
(8)
- June 2011 (2)
- May 2011 (1)
- April 2011 (2)
- February 2011 (2)
- January 2011 (1)
-
►
2010
(98)
- December 2010 (3)
- November 2010 (1)
- October 2010 (3)
- September 2010 (2)
- August 2010 (18)
- July 2010 (20)
- June 2010 (13)
- May 2010 (9)
- April 2010 (8)
- March 2010 (16)
- February 2010 (2)
- January 2010 (3)
-
►
2009
(259)
- December 2009 (8)
- November 2009 (16)
- October 2009 (13)
- September 2009 (22)
- August 2009 (30)
- July 2009 (30)
- June 2009 (23)
- May 2009 (21)
- April 2009 (22)
- March 2009 (29)
- February 2009 (21)
- January 2009 (24)
-
►
2008
(5)
- December 2008 (5)


 मार्कण्डेय
मार्कण्डेय