
जब भी गांव के विकास की बात आती है ...शहरों की खिंचाई शुरू हो जाती है..ये थोड़ा सा अन्याय है मुझे लगता है..शहर विकास का एक नैसर्गिक पड़ाव है..ऐसा नहीं होता तो विकास के चश्मे से शहरों का भी वर्गीकरण नहीं होता..मसलन छोटा शहर..बड़ा शहर..सिटी..मेट्रो सिटी..कॉस्मोपॉलिटन सिटी..वगैरह वगैरह..छोटे शहरों के लोगों का भी मेट्रोपॉलिटन के सामने कुछ ऐसा ही रोना है...पिछड़े रह जाने की ऐसी ही दुहाई है..सबकुछ नहीं मिल पाने की ऐसी ही कसक है..लेकिन उनको नहीं मालूम कि दिल्ली का दिल भी लंदन या न्यूयार्क को देख कर जल सकता है...या फिर ये कह सकता है कि वो आगे निकल गये..हम कहां रह गये...ये शिकायत व्यक्तिगत तौर पर मुझे थोड़ी 'रिस्पेक्टिव' या 'रेलेटिव' लगती है. बहरहाल, ये सवाल कि शहरों ने गांवों को क्या दिया है.. बताने की ज़रूरत नहीं है..शहर उन लोगों का आलंब बने जो बाढ़ या सूखे में अपना सबकुछ खो बैठे..जब गांव घर में पानी घुसा तो शहरों की तंग गलियों ने आसरा दिया..जब गांव के स्कूल बदहाल हो गये..तब शहरों ने हमें ये क़ाबलियत दी कि हम पुरज़ोर ढ़ंग से अपने गांवों के लिए आवाज़ उठा पाने की ताक़त रखते है..आज हमारे गांवों की बात हमारे मुंह से सुनी और समझी जा रही है तो बीच में कहीं न कहीं एक शहर ज़रूर खड़ा रहता है..कमज़ोरी नहीं बल्कि हौसला बनकर..अत्मविश्वास बनकर. गांवों की जो तस्वीर हम अपने आनेवाले दिनों के लिए बुनते हैं..जिसे दिमाग के काग़ज से ज़मीन की ठोस परत पर उतारना चाहते है...तो कल्पना की वो जमीन भी कहीं न कहीं इन शहरों ने मिल कर बनाई है....बीच की लाईन क्यों बना देते हैं हम..मान लीजिए कि दिल अगर गांव है..वैसे बापू ने भी माना था कि भारत की आत्मा गांवो में ही बसती है...तो इस शरीर का दिमाग शहर है..शहरों का आधार गांव रहे है..इसमें कोई दो राय नहीं...यहां के फाईवस्टार होटलों में परोसा जाने वाला खाना..और उसे परोसने वाला दोनों ज्यादातर गांवों के ही होते है...शहर के हाथ गांव से आते है...लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा..कि शहर इन हाथों को थाम भी लेते हैं..बीच की लाईन को मिटा कर बात करते हैं..ये मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि गांव पीछे छूट गये..कारणों की विवेचना नहीं करूंगा...लेकिन गांवों की बड़ी ज़रूरतें क्या हैं इस समय..उनके पास क्या कुछ है जिससे इन ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा...ये समझना ज्यादा ज़रूरी है..गांवों के पास कुछ चीज़े ऐसी हैं जो शहरों के पास नहीं हैं....गांवों-ज़रूरतों को तोड़ कर देखेंगे तो शहरों के मुक़ाबले छोटी लगेंगी लेकिन ग्रासरूट लेवल पर सब मिलजुल कर अभाव की बड़ी तस्वीर बना देते हैं....तो मेरे हिसाब से हल ग्रास लेवल से शुरू होना चाहिए..गांव की ताक़त क्या है?..गांवों की असल ताक़त उनका सस्ता संसाधन है..बात चाहे प्राकृतिक संसाधनों की हो, मानव संसाधन की हो ..हर मामले में उपलब्धता ज्यादा है...लेकिन इन संसाधनो के साथ सबसे बड़ी चुनौती इनकी क्वालिटी को लेकर...सबसे ज्यादा काम की ज़रूरत मानवसंसाधन के विकास और उसके इस्तेमाल पर करने की है..डीसेंट्रलाईज़ेशन ऑफ डेवलपमेंट..अगर इस संकल्पना पर काम किया जाये तो विकास के विकेंद्रीकरण का अंतिम बिंदु गांव का कोई वही आदमी होगा..जिसे हम शहरों की ओर पलायन करने से रोकना चाहते हैं..जब बिहार के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि राज्य की श्रम शक्ति का 50 फ़ीसदी से ज्यादा हिस्सा राज्य से बाहर है तो पलायन की गंभीरता समझी जा सकती है..तो जब हम विकास के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो यहीं से शहरों की गांवों के अंदर भूमिका शुरू हो जाती है...इस प्रक्रिया में वो सबकुछ आता है जो शहरों की तरफ़ गांवों के लोगों को खींच कर ले जाता है..कारण चाहे ज़रूरत हो या सपने...आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्यों नहीं सोच पाते....हर चीज़ को विकेंद्रीकृत कर दे- शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय सबकुछ. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अंग्रेजी बोलने-पढ़ने का माहौल हम गांवो और छोटे शहरों में पैदा कर दे..फिर वहां से विलेज कैंपस कर वहां के युवा को किसी बीपीओ में उसे नौकरी दे दे..और ये आउटसोर्सिंग गांवो से ही हो..ये सुविधा दिल्ली से नहीं हटेगी तो लोग भागेंगे...गया का पटुआ टोली गांव एक बेहतरीन उदाहरण है..जहां जुलाहों की बस्ती से हर साल आईआईटी में बच्चे दाखिला लेते है..पटना का सुपर थर्टी भी बेहतरीन मिसाल है....ये लोग महंगी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली नहीं जा सकते ...लेकिन अच्छी पढ़ाई अपने घर में ज़रूर कर लेते ...गांवों में और छोटे शहरों में जहां बिजली नहीं रहती वहां के लड़के-लड़कियां एजुकेशन क्लब बना कर तैयारियां करते है..और खुद को साबित करते हैं..अगर इन युवाओं को ये शहरी सुविधायें विकेंद्रित हो गांव में मिलें तो ..कौन जाये कमबख्त अपने गांव की गलियां छोड़कर....शहर की सड़कें जब हरियाणा, पंजाब, गोवा, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों के गांवों तक विकेंद्रीकृत होती हुई पहुंची..तो शहर की चीज़े भी वहां तक गई..बस यही प्रक्रिया हर मामले में हो..एक बार बीबीसी में ये पूछा गया कि एक दिन के लिए पीएम बनने पर आप क्या करेंगे? तो किसी का सुझाव था कि एक दिन के लिए कैबिनेट की बैठक किसी गांव में कराऊंगा..उस एक दिन के चक्कर में उस गांव की कई चीज़े सुधर जायेंगी..मुझे अच्छा लगा..क्या शहरों में,राजधानियों में होने वाली इस तरह की बैठकों ,सम्मेलनों, सभाओं, महोत्सवों को हम गांवों में नहीं कर सकते ...यक़ीन मानिये कोई मुश्किल काम नहीं है..अलबत्ता गांवों में रोज़गार के साथ-साथ कई चीज़ो का इज़ाफा होगा...इन सब पर तो गांव का भी हक है... यानि शहरों का विकेंद्रीकरण ऐसे भी हो सकता है.. इससे शहरों को भी एक बड़ा फ़ायदा होगा...एक तो उनपर दबाव घटेगा..दूसरे आयोजनों का खर्च घटेगा...शहरों में स्लम्स के लिए टूरिज़म नाम की चीज विकसित हो जाती है..इससे लाख बेहतर है कि विलेज टूरिज़म विकसित करें..दुनियां को गांवों के दर्शन करायें..सरकार अपने किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए गांवो को प्राथमिकता दे..खेलों के स्टेडियम गांवों में क्यों नहीं बने...जगह काफ़ी है वहां ..क्यों शहरों में भीड़ बढ़ाते हैं हम... बडी बात ये है कि गांव के लोग भी ये महसूस कर पायेंगे कि हम भी इन सब चीज़ो से जुड़े है..फिर शहर और गांव के बीच की जो लाईन है वो हल्की होती जायेगी...जब मै विकेंद्रीकरण की बात करता हूं तो यही सोचता हूं...सुविधाओं के गढ़ बन चुके बड़े शहर टूटें..और ये सविधायें छोटे शहरों और गांवों तक जायें...सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात पर तो पहल बहुत तेज़ी से हुई..लेकिन दिल्ली में जमा हुई सुविधाओं के बारे में ऐसा विचार क्यों नहीं आया..आख़िऱ में मै आपको एक सपने के साथ छोड़ जाता हूं....आंखें बंद कीजिए..और देखिये...मऊ का बीपीओ सेंटर..छपरा के किसी गांव का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम..गुंटूर के गांव में बना आईआईएम....उड़िसा के चिल्का गांव में कैबिनेट मीटिंग भवन...प्रगति मैदान का मोटर एक्सपो श्रीगंगानगर के किसी गांव में....नागालैड या सिक्किम के किसी पहाड़ी गांव में राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव....आंखे खोलिये ..आपको लगता है कि इस एक क़दम से उन जगहों की इससे तस्वीर बदेलगी?..नहीं लगता तो आप इसे मेरा यूटोपिया कह सकते हैं..मुझे बुरा नहीं लगेगा...
रवि मिश्रा


 मार्कण्डेय
मार्कण्डेय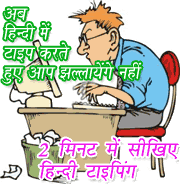
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
6 बैठकबाजों का कहना है :
रवि मिश्रा जी
अच्छा विषय उठाया है। हम यदि प्रारम्भ से ही समग्र विकास की बात करते तो शायद इतना विरोधाभाषी विकास नहीं हुआ होता। आप कहते हैं कि जब गाँव में विपत्ति आती है तब शहर ही पनाह देता है। यह उनकी मजबूरी है, कैसी पनाह मिलती है? झुग्गी झोपडी में, गन्दी बस्तियों में। पहले राजाओं के काल में भी शहर का विकास होता था। एक पानी की समस्या को ही लें। वे तालाब बनवाते थे और पानी नि:संदेह गाँवों से ही आता था लेकिन शहरों में भी बावडी, कुएं खुदवाते थे। लेकिन आजादी के बाद सारे ही जल के अन्य स्रोतों को बन्द कर दिया गया और केवल बडे बांधों का जमाना आ गया। इससे गाँव उजड गए। आज गाँवों में जागृति आयी है, वहाँ भी एनीकट बनने लगे हैं और शहर के तालाब सूखने लगे हैं। हम विकास कहीं का भी करे लेकिन एक दूसरे की कीमत पर नहीं। गाँव का व्यक्ति 50 वर्ष पूर्व मजदूरी करने शहर गया था, आज भी वह मजदूर ही है। कहाँ हुआ उनका विकास? शहरों ने उन्हें आबाद नहीं किया है बल्कि बर्बाद कर दिया है। मेरे पडोस में एक फाइव स्टार होटल बन रहा था, मैने देखा कि कारीगर और मजदूर कैसे नारकीय रूप में रहने को वहाँ मजबूर थे। यदि हमें फासले कम करने हैं तो गाँव ने हमें क्या दिया इसकी सूची बनानी होगी तब मालूम पडेगा कि रोटी, पानी, सडक, बिजली आदि सभी कुछ उनकी मेहरबानी से हमें मिला है। उनकी जमीनों पर, उनके लोगों द्वारा ही हम ठाट से रह रहे हैं। जिस दिन भारत में गाँवों में विकास की कल्पना साकार होगी उस दिन हम दुनिया में अग्रणी होंगे। आपका आलेख अच्छा है, आवश्यकता बस गाँव के जीवन को देखने की ही है। तभी हम समझ पाएंगे उनका दर्द। अच्छे आलेख के लिए बधाई।
आज भारत की राजधानी दिल्ली में कितने ही इलाकों में पानी ,बिजली नहीं है . गाँव का हाल तो जग जाहिर है .गाँधी जी ने कहा भारत गाँव में बसता हैं .इसलिए काम की पहल वहीं से की .उनका विकास किया .लेकिन तब से आज तक शहर -गाँव की खाई पाटी न जा सकी ..बिजली बनाने के लिए नदियों पर बाँध बनाये जा रहें हैं .जैसे उत्तराखंड में मनेरीभाली में गंगा नदी पर बाँध बना है . सारे आसपास के गाँव को यहाँ से हटना पडा .वहां
के ग्लेशियर ,मौसम गंगा की धारा में बदलाव आया .गंगा का पानी कम होता जा रहा है . प्रकृति से खिलवाड़ न करें .यह अन्याय ,समस्याएं गाँव -शहर पर भारी पडती हैं .जागरूक आलेख लगा बधाई .
रवि जी सबसे पहले इस बहतरीन आलेख के लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद.
आपने बिलकुल सही कहा की हमें गांव और शहर की बीच की खाई को पाटना चाहिए. देश की आज़ादी के बात विकास को लेकर शहरो और गांवो में होने वाले परिवर्तनों को लेकर गांधी जी ने भी यही कहा था की न केवल शहरों को बल्कि गांवो को भी विकसित किया जाना चाहियेत था. लेकिन बदनसीबी देखिये की गांवों को तो दूर छोटे शहरों को भी विकसित नहीं किया गया. आज किसी भी तरह के बड़े काम के लिए शहर जाना पड़ता है. चाहे वो नाकरी ढूढने की बात हो या इन्टरनेट इस्तेमाल करने की. आपने अंत में बिलकुल सही कहा है हर काम गांव में नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ काम तो किये जा सकते हैं जैसे टूरिस्म वगैरा वगैरा.
रवि जी आपने बहुत सटीक विषय पर अपनी बात कही है | गॉव और शहर के बीच की लकीर मिट जाए तो बेशक आपकी भाषा में अगर गॉव को दिल और शहर को दिमाग मान ले तो ,,भारत रूपी शारीर दोनों के तालमेल से ज्यादा स्वस्थ होगा................जिसे किसी भी प्रकार के विकासहीन फ्लू का कोई असर नहीं होगा |
आलेख और उस पर सभी की टिप्पणियाँ बहुत ही अच्छी लगीं मुझे.
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)