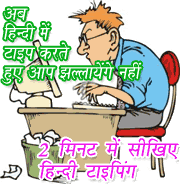इस शुक्रवार को जिन उन्नीस सांसदों ने केंद्र के मंत्री पद की शपथ ली है, वे बुरा न मानें, तो एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने, प्रधानमंत्री सहित, अपनी शुरुआत झूठ से की है। मैं यहां इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता कि जो लोग चुनाव जीत कर लोक सभा में आए हैं, उन्होंने अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव खर्च की सीमा का जरूर उल्लंघन किया होगा। यह एक ऐसा उल्लंघन है जिसके बिना संसद या विधान सभा का कोई भी चुनाव आज जीता ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि जन सामान्य के मन में यह धारणा घर कर गई है कि जब इतना खर्च करके चुनाव लड़ा जाता है, तो सांसद या मंत्री बनने के बाद इसकी भरपाई किए बिना किसी का काम कैसे चल सकता है? भरपाई ही नहीं, कुछ अतिरिक्त उपार्जन भी होना चाहिए। घर की पूंजी लुटाने के लिए तो कोई सांसद नहीं बनता! अगर यह घाटे का सौदा होता, तो किसी भी चुनाव क्षेत्र के लिए इतने उम्मीदवार कहां से आते! मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूं और बहुत भरे ह्मदय से, वह इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, एक तो उन्हें पता नहीं होगा कि वे किस बात की शपथ ले रहे हैं और जिन्हें पता होगा, वे जानते होंगे कि वे जो शपथ ले रहे हैं, उसका निर्वाह करने नहीं जा रहे हैं। पहले शपथ की शब्दावली पर ध्यान दिया जाए। संविधान में दी गई शपथ की भाषा इस प्रकार है : ‘मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।’
शपथ के केंद्र में संविधान और उसके प्रति निष्ठा ही मुख्य है, जिसके अनुसार मंत्री को राज-काज करना चाहिए। इस निष्ठा के दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि सभी नागरिकों के साथ न्याय किया जाएगा। किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। लेकिन यह तो प्रशासनिक फैसलों की बात है, सरकारी कार्य प्रणाली का मामला है। मूलभूत सवाल यह है कि राज्य का काम क्या है। भारत सरकार को करना क्या चाहिए? यह तय किए बिना प्रशासनिक फैसले किस आधार पर किए जाएंगे?
यहां दो चीजें प्रासंगिक हैं। राज्य का एक कर्तव्य यह है कि सभी नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की जाए। पर यह एक तरह से नकारात्मक कर्तव्य है। राज्य किसी के मूल अधिकारों की अवहेलना न करे। सबको संविधान के अनुसार स्वसंत्रतापूर्वक जीने का अवसर मिले। इससे यह पता चलता है कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख संविधान के भाग चार में किया गया है। इस भाग में राज्य की नीति के इक्यावन तत्व निश्चित किए गए हैं। यानी अपनी नीतियां बनाते समय और फैसले करते समय राज्य को इन निदेशक तत्वों को दिमान में रखना होगा। संविधान कहता है : ‘...इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।’ कहा जा सकता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों वाला यह भाग चार ही भारत सरकार का वेद, कुरआन और बाइबल है।
दुर्भाग्यवश भारत सरकार के संचालन में संविधान के जिस हिस्से की सर्वाधिक अवहेलना हुई है, वह यही भाग चार है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तब से अब तक कुछ महीने कम साठ साल हो चुके हैं। संविधान के भाग चार का अनुच्छेद 45 कहता है : ‘राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।’ हम जानना चाहते हैं कि अभी तक किस सरकार ने इस अनुच्छेद को लागू करने का प्रयास किया है? मनमोहन सिंह की पिछली सरकार ने इस बारे में एक कानून जरूर बनाया है, जो संविधान के इरादे से मेल नहीं खाता। इस कानून को भी अभी तक लागू नहीं किया गया है।
लेकिन भाग चार के उद्देश्यों की व्यापकता देखते हुए बालकों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा बहुत मामूली बात है। कुछ बड़े उद्देश्यों पर विचार कीजिए -- राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संचार किया जाएगा, आय की असमानताओं को कम करने की कोशिश की जाएगी, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाएगी जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी मिले तथा काम की दशाएं ऐसी हों जो शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करनेवाली हों। इसके अतिरिक्त लगभग एक दर्जन निदेश और हैं जो इसी प्रकृति के हैं।
सवाल यह है कि इस शुक्रवार को जिन सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है, क्या वे राज्य की नीति के इन निदेशक तत्वों का पालन करेंगे? भविष्य में जो सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या उनका ऐसा कोई इरादा होगा? क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल यह सामूहिक जिम्मेदारी महसूस करेगा कि सरकार संविधान के भाग चार के अनुसार चलाई जाए?
यह सच है कि संविधान स्वयं कहता है कि इन उपबंधों को लागू कराने के लिए कोई नागरिक अदालत में नहीं जा सकता। लेकिन इससे क्या होता है? संविधान के अनुसार सरकार का जो कर्तव्य है, वह कर्तव्य है। उस कर्तव्य का पालन करने की ईमानदार कोशिश किए बगैर ‘संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा’ रखने के संकल्प का अर्थ क्या है?
राजकिशोर


 मार्कण्डेय
मार्कण्डेय