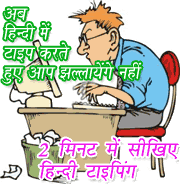अहमद फ़राज़ एक ऐसा नाम जिसके बिना उर्दू शायरी अधूरी है. आज अगर एशिया में इश्किया शायरी में फैज़ अहमद "फैज़" के बाद किसी शायर का नाम आता है तो वो हैं अहमद "फ़राज़". आज उनकी ग़ज़लें हिन्दुस्तान और पकिस्तान के अलावा कई और मुल्कों में भी मशहूर हैं. जहाँ भी इंसानी आबादी पाई जाती है. उनकी ग़ज़लें पढ़ी और सुनी जाती है.
अहमद फ़राज़ साहब की पैदाइश पकिस्तान के नौशेरा जिले में 14 जनवरी 1931 को को एक पठान परिवार में हुई. उन्होंने पेशावर युनिवर्सिटी से इल्म हासिल किया और वही पर कुछ वक़्त तक रीडर भी रहे. उनका विसाल (निधन) 25 अगस्त, 2008 को इस्लामाबाद के एक अस्पताल में हुआ. वो गुर्दे की बीमारी में मुब्तिला हो चुके थे. उन्हें पकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान हिलाल-ऐ-इम्तियाज़ भी हासिल था. इसी के साथ उन्हें कई और गैर मुल्की सम्मान भी मिले था.
फ़राज़ साहब की मकबूलियत और शोहरत का अंदाजा एक वाकये से लगाया जा सकता है. एक दफा अमेरिका में उनका मुशायरा था जिसके बाद एक लड़की उनके पास आटोग्राफ लेने आयी। नाम पूछने पर लड़की ने कहा "फराज़ा". फराज़ ने चौंककर कहा "यह क्या नाम हुआ?" तो बच्ची ने कहा "मेरे मम्मी पापा के आप पसंदीदा शायर हैं। उन्होंने सोचा था कि बेटा होने पर उसका नाम फराज़ रखेंगे। लेकिन बेटी पैदा हो गयी तो उन्होंने फराज़ा नाम रख दिया।"
इस बात पर एक शे'र कहा था.
"तुझे और कितनी मोहब्बतें चाहिए फराज़,
मांओ ने तेरे नाम से बच्चों का नाम रख दिया"
क्या कहते हैं दूसरे शायर
फ़राज़ की शायरी ग़में दौराँ और ग़में जानाँ का एक हसीन संगम है। उनकी ग़ज़लें उस तमाम पीड़ा की प्रतीक हैं जिससे एक हस्सास (सोचने वाला) और रोमांटिक शायर को जूझना पड़ता है। उनकी नज़्में ग़में दौराँ की भरपूर तर्जुमानी करती हैं और उनकी कही हुई बात, जो सुनता है उसी की दास्ताँ मालूम होती है।
कुंवर महेंद्र सिंह बेदी "सहर"
आज के दौर में भारत और पाकिस्तान की बंदिशों को नहीं मानने वाले लोगों की बेहद कमी है। पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरह की परेशानियों को उन्होंने झेला और उसके बाद भी इंसानी आजादी और मजहब के भेदभाव से ऊपर उठकर लिखा वह काबिले तारीफ है।
डॉ. अली जावेद
(नेशलन काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के निदेशक)
फराज़ उर्दू रोमांटिक शायरी का ऐसा नाम है जिसकी गज़लों और नज्मों से तीन पीढ़ियां वाकिफ है। इस वक्त उनके जितने शेर लोगों को याद है उतने शायद ही किसी अन्य शायर के हों
मशहूर शायर मुमताज राशिद
फ़राज़ अपने वतन के मज़लूमों के साथी हैं। उन्हीं की तरह तड़पते हैं, मगर रोते नहीं। बल्कि उन जंजीरों को तोड़ते और बिखेरते नजर आते हैं जो उनके माशरे (समाज) के जिस्म (शरीर) को जकड़े हुए हैं। उनका कलाम न केवल ऊँचे दर्जे का है बल्कि एक शोला है, जो दिल से ज़बान तक लपकता हुआ मालूम होता है।
मजरूह सुल्तानपुरी
इसी तरह से उनकी वतनपरस्ती की एक मिसाल मिलती है. पश्चिम एशिया के अरबी बोलने वाले मुल्कों में एक जश्ने-शायराँ (काव्योत्सव) बहुत मशहूर है—अल मरबिद पोयट्री फेस्टिवल. उसमें तमाम मुल्कों से अलग-अलग ज़बानों के मशहूर शायर हिस्सा लेने के लिए बुलाये जाते हैं. उसी में पाकिस्तान से उर्दू की नुमाइन्दगी करने आए थे जनाब अहमद फ़राज़. हिन्दुस्तान से उर्दू की नुमाइन्दगी करने के लिए भेजे गए थे जनाब रिफ़त सरोश. यह वह वक़्त था जब इराक़ की लड़ाई ईरान से चल रही थी और ख़ूब घमासान चल रहा था.फ़राज़ की शायरी ग़में दौराँ और ग़में जानाँ का एक हसीन संगम है। उनकी ग़ज़लें उस तमाम पीड़ा की प्रतीक हैं जिससे एक हस्सास (सोचने वाला) और रोमांटिक शायर को जूझना पड़ता है। उनकी नज़्में ग़में दौराँ की भरपूर तर्जुमानी करती हैं और उनकी कही हुई बात, जो सुनता है उसी की दास्ताँ मालूम होती है।
कुंवर महेंद्र सिंह बेदी "सहर"
आज के दौर में भारत और पाकिस्तान की बंदिशों को नहीं मानने वाले लोगों की बेहद कमी है। पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरह की परेशानियों को उन्होंने झेला और उसके बाद भी इंसानी आजादी और मजहब के भेदभाव से ऊपर उठकर लिखा वह काबिले तारीफ है।
डॉ. अली जावेद
(नेशलन काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के निदेशक)
फराज़ उर्दू रोमांटिक शायरी का ऐसा नाम है जिसकी गज़लों और नज्मों से तीन पीढ़ियां वाकिफ है। इस वक्त उनके जितने शेर लोगों को याद है उतने शायद ही किसी अन्य शायर के हों
मशहूर शायर मुमताज राशिद
फ़राज़ अपने वतन के मज़लूमों के साथी हैं। उन्हीं की तरह तड़पते हैं, मगर रोते नहीं। बल्कि उन जंजीरों को तोड़ते और बिखेरते नजर आते हैं जो उनके माशरे (समाज) के जिस्म (शरीर) को जकड़े हुए हैं। उनका कलाम न केवल ऊँचे दर्जे का है बल्कि एक शोला है, जो दिल से ज़बान तक लपकता हुआ मालूम होता है।
मजरूह सुल्तानपुरी
तमाम मुल्कों के शायर बग़दाद में मौजूद थे. इराक़ी हुकूमत को लगा कि यह बढ़िया मौक़ा है दुनिया भर के शायरों को ‘ईरान की ज़्यादतियों को दिखाने का'. इसलिए उन्होंने काव्योत्सव के एक दिन पहले जंग के मोर्चे पर ले जाने के लिए एक बस का इन्तज़ाम किया और सभी को एक-एक यूनिफॉर्म पकड़ाना शुरू कर दिया। सबब यह बताया गया कि जंग के मोर्चे पर जा रहे हैं तो जंग की पोशाक ही होनी चाहिए। हिफाज़त के मद्देनज़र यह ज़रूरी है. तमाम मुल्कों के शायर पोशाक की पुलिन्दा लेकर बस में जा बैठे। जब एक भारत से गए हिंदी कवि का नंबर आया तो वह अड़ गए कि मैं यह नहीं पहनूंगा. इंचार्ज इराक़ी कमाण्डर उसे समझाने आया तो उन्होंने उसे समझाना शुरू कर दिया और बताया कि मैं बसरा से एक बार उस इलाक़े को देखने एक पत्रकार के रूप में सादे लिबास में जा चुका हूँ। दुबारा अगर आप उस इलाक़े में ले ही जाना चाहते हैं तो मैं जैसा हूँ, भारतीय, वैसा ही चलूँगा. आपकी फौजी वर्दी पहनकर हर्गिज़ नहीं जाऊँगा। कभी अगर फौजी वर्दी पहनने का अवसर आया भी तो अपने देश के लिए पहनूँगा, इराक़ या ईरान के लिए नहीं। अफसर ज़रा तन्नाया लेकिन कर कुछ न पाया। उसने तुरुप चाल चली कि अगर मोर्चे पर आपको कुछ हो गया, गोली ही लग गई तो ?
"तो मैं, ज़ाहिर है कि मर जाऊँगा। लेकिन मरूँगा तो भारतीय. आपकी सैनिक वर्दी में अगर मरा तो मेरी पहचान भी सही न हो सकेगी," उन्होंने कहा।
उन हिंदी कवि के साथ साथ रिफ़त सरोश साहब भी अड़ गए. और लोग भी मेरी इस दलील में शामिल न हो जाएँ, इस डर से वर्दी न लेने वाले लोगों को साथ न ले जाना मुनासिब पाया गया और वह वापस रिफ़त साहब के साथ होटल लौट आये. लॉबी में देखा कि फ़राज़ साहब पहले से ही कुछ चाहने वालों के साथ बैठे हैं।
उन्होंने ही टोका : ‘तो आप लोग भी नहीं गए?’
‘जी नहीं ! हमें उनकी वर्दी पहनना गवारा नहीं था.’ हिंदी कवि ने कहा।
‘निहायत अहमक़ाना ज़िद थी। मैं भी इसी वजह वापस आ गया।’ फ़राज़ साहब ने कहा।
फिर हिंदी कवि ने मजाकिया लहजे में कहा कि इतने लम्बे-तगड़े पठानी बदन पर कोई इराक़ी वर्दी फिट भी तो नहीं आ सकती थी, फ़राज़ साहब। इतने ख़ूबसूरत बदन के सामने वर्दी को खुदकुशी करनी पड़ती और उन्होंने फ़राज़ साहब की ही ग़ज़ल का एक शेर उन्हें नजर किया :
जिसको देखो वही ज़ंजीर-ब-पा लगता है।
शहर का शहर हुआ दाखिले-ज़िन्दा जानाँ!
फ़राज़ साहब को जिन दो ग़मों ने ज़िन्दगी भर परेशान किया. वो हैं उन्हें देश निकला दे देना और पकिस्तान में जम्हूरियत कायम न हो पाना.
उन्होंने एक ग़ज़ल कही थी.
रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ
आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ
किस किस को बताएँगे जुदाई का सबब हम
तू मुझसे ख़फ़ा है तो जमाने के लिए आ
पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो
रस्मो-रहे-दुनिया ही निभाने के लिए आ
जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने
ऐसे ही किसी रोज़ न जाने के लिए आ
हमारी अन्य प्रस्तुतियाँ
कुछ लोगों का कहना है कि यह ग़ज़ल फ़राज़ साहब ने अपनी महबूबा के लिए कही थी तो कुछ लोगो का कहना है कि उन्होंने यह ग़ज़ल पुष्पा डोगरा के लिए कही थी जो कि भारतीय कत्थक डांसर थी. लेकिन अहमद फ़राज़ साहब का कहना था कि यह ग़ज़ल उन्होंने पकिस्तान की जम्हूरियत के लिए कही. फर्क सिर्फ इतना है कि उसे अपनी महबूबा मान लिया है.दूसरा गम उन्हें देश निकाला से मिला था. अपने इस गम को कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने अश'आर में कहा है.
कुछ इस तरह से गुज़ारी है ज़न्दगी जैसे
तमाम उम्र किसी दूसरे के घर में रहा।
किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंज़िल
कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा।
हिजरत यानी देश से दूर रहने का दर्द और अपने देश की यादें अपनी उनके यहाँ मिलती हैं। कुछ शेर देंखें :
वो पास नहीं अहसास तो है, इक याद तो है, इक आस तो है
दरिया-ए-जुदाई में देखो तिनके का सहारा कैसा है।
मुल्कों मुल्कों घूमे हैं बहुत, जागे हैं बहुत, रोए हैं बहुत
अब तुमको बताएँ क्या यारो दुनिया का नज़ारा कैसा है।
ऐ देश से आने वाले मगर तुमने तो न इतना भी पूछा
वो कवि कि जिसे बनवास मिला वो दर्द का मारा कैसा है।
फ़राज़ साहब हिन्दोस्तानी मुशायरों में उन्हें बख्शी गई इज़्जत का बयां करते नहीं थकते थे.
"हिन्दुस्तान में अक्सर मुशायरों में शिरकत से मुझे ज़ाती तौर पर अपने सुनने और पढ़ने वालों से तआरुफ़ का ऐज़ाज़ मिला और वहाँ के अवाम के साथ-साथ निहायत मोहतरम अहले-क़लम ने भी अपनी तहरीरों में मेरी शेअरी तख़लीक़ात को खुले दिल से सराहा। इन बड़ी हस्तियों में फ़िराक़, अली सरदार जाफ़री, मजरूह सुल्तानपुरी, डॉक्टर क़मर रईस, खुशवंत सिंह, प्रो. मोहम्मद हसन और डॉ. गोपीचन्द नारंग ख़ासतौर पर क़ाबिले-जिक्र हैं"
वैसे तो फ़राज़ एक ग़ज़ल कहने वाले शायर कि हैसियत से जाने जाते हैं. लेकिन उनकी नज्मों का भी कोई सानी नहीं है.
ये दुख आसाँ न थे जानाँ
पुरानी दास्तानों में तो होता था
कि कोई शाहज़ादी या कोई नीलम परी
देवों या आसेबों की क़ैदी
अपने आदम ज़ाद दीवाने की रह तकते
फ़राज़ साहब को गुज़रे एक साल हो गया मगर उनकी शाइरी आने वाली कई पीढ़ियों को रोशनी देगी....
अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख़्वाबों में मिलें
जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें
शामिख फ़राज़
(लेखक हिंदयुग्म के यूनिपाठक भी हैं...)


 मार्कण्डेय
मार्कण्डेय